पेशे से कॉरपोरेट मजदूर, अनुपमा शर्मा एक अलग पहचान की तलाश में हैं। इस तलाश के सफर में अपने विचारों को कविता रूप में ढाल कर उनकी अभिव्यक्ति करने की चेष्टा करती हैं। दिल्ली निवासी अनुपमा का यह कहीं भी उनकी कविताओं के छपने का पहला अवसर है। लेखन के अतिरिक्त वे अध्यात्म में रुचि रखती हैं।
तितलियाँ
देखो एक खुले बाग़ में
ओस पड़ी ठंडी घास पर
हाथ फैलाए एक परछाई खड़ी है
स्थिर जैसे किसी की प्रतीक्षा करती है
देखो एक एक करके ढेरों रंग बिरंगी तितलियाँ
उस खुले हाथ पर आ बैठी हैं
उड़ती नहीं, बस उसके आस-पास ही रहती हैं
कभी उसके कंधों पर बैठती हैं
कभी बालों से खेलती हैं
वो यूँ ही रह जाती हैं उसके पास
देखो वो हाथ उन तितलियों को पकड़ते नहीं
उन्हें अपनी मुट्ठी में क़ैद करते नहीं
वो परछाई तो बस उन्हें क़रीब से देखती है
उनके रंग आँखों में उतार लेती है
उनके छोटे-छोटे पंखों के साथ अपने मन को भी पंख दे देती है
देखो ये तितलियाँ उसकी खुशियाँ हैं
जिन्हें वो बांध नहीं सकती
बस हाथ फैला कर आने का इंतज़ार कर सकती है….
और तुम देख लेना कि हो जाएगी गायब यह परछाई एक दिन
फिर लौटेगी बन कर
एक रंग-बिरंगी तितली किसी और परछाई की खुशियाँ बन कर
ढ़ूँढता हूँ
चलता हूँ इस सहरा में, तपती रेत के टीलों पर
हवा में बिखरी गर्म धूल चुभती हैँ जो आँखों में
लगता है ले जाएँगी कभी अपनी गर्म आगोश में
और बस खो जाऊँगा मैं इनमें कहीं
डरता हूँ इन मौज–ए–सराब से
जो आब की झलक से हर थोड़ी दूर पर धोखा देती हैं
अपने पीछे बुलाते थका देती हैं
पर अनजान प्यास ही छोड़ देती हैं
ढूँढता हूँ इस सहरा की हदों को अब
कहाँ खत्म होगा ये तपिश का सफर!
अभी देखा है मैने एक नखलिस्तान
हरा भरा बाग़ इस बीच रेगिस्तान
अब जो थक कर बैठा हूँ लगता है यहीं रह जाऊँ
इसकी ही तलाश रही हो जैसे
बचपन में बनायी पहली तस्वीर जैसे
फिर कहीं से एक गर्म हवा का झोंका आया तो याद आया
ये तो नहीं है आखिरी मक़ाम
नहीं है यह मेरी जमीन मेरा आसमान
है ये बस कुछ राहत की साँसें
पर सहरा में ही कहीं हैं ये भी
और मैं तो
ढूँढता हूँ इस सहरा की हदों को अब
कहाँ खत्म होगा ये तपिश का सफर…
कौन हूँ मैं
कल खाली घर में खुद से बात करने का वक्त मिला
जा आईने के सामने खड़े हो गए
कुछ देर सफेद होते बालों की तादाद बढ़ती देखी
कुछ देर चेहरे पर पड़ गए कुछ निशान देखे
कुछ देर अलग-अलग हाव-भाव भी ला कर देखें
कि जब ऐसा मुँह बनाते हैं तो देखने वाले को कैसा लगता होगा
जैसे मानचित्र में अनजाना देश
ये भी देखा कि कितना हँसना अच्छा लगता है और कितने के बाद मुँह कुछ ज़्यादा अजीब लगता है
नहीं नहीं पागलपन नहीं था बस बाहरी छवि को आँका जा रहा था
फिर यूँ ही देखते-देखते आँकने लगा
कैसे बदल गया ये चेहरा इतना, कब बदल गया
जैसे टूट गया हो महादेश टुकडों में
साथ ही कहाँ गयी वो नर्मियाँ
कहाँ गयी वो बेफिक्री , वो ज़िंदादिली,
कब आ गयी ये चिंता की लकीरें और ये वक्त के निशान
और अब क्या पहचान बताता है ये चेहरा मेरी
कौन हूँ मैं
एक खण्डित प्रदेश अपने अतीत से विछिन्न
पुर–सुकून की तलाश में भटकता एक पाबंद ज़ेहन
या और तरक्की के पड़ाव ढूँढता एक उत्सुक मन
अकेलापन खोजता एक दुनियादारी से थका शरीर
शायद जिसकी मंजिल हो कोई घना वन
या अपनो के बीच खिलखिलाने को तरसता खुशमिज़ाज़ दिल
खुद को आगे रखकर अपना हर फैसला करता मैं
या अपने परिवार यार के लिए खुद को पीछे करता मैं
बस अब से सब ईश्वर पर छोड़ दूँगा कहता मैं
या अब से सब अपने हाथ में लेने का निश्चय करता मैं
हूँ एक मस्त मलंग दिल खोल कर जीने वाला फकीर
या बस ’कौन हूँ मैं’ के सवाल का जवाब ढूँढता कोई चित्त अधीर…
सिस्टम रिफ्रेश
आओ चलें कुछ दिन इस शोर से दूर
कहीं जहाँ सुकून आए गर्मी के तपते सूरज से
इतना कि दिल-ओ-दिमाग का शोर भी शांत हो जाए
जहाँ मैं ऊब जाऊँ हो इतना चैन
के फिर तलाशे मन थोड़ी सी बेचैनी
अकेलेपन का टुकड़ा और गीले नैन
चलो चलें पहाड़ों पर किसी झील के किनारे
तुम धूप से पीठ करके बैठो और अखबार बाँचों
और मैं आँख बंद करके धूप सेकूँ
ना कोई आवाज़ ही और बस कभी कभी हवा कुछ बातें कर ले
या चलो किसी दरिया के साथ चलके बैंठे
जहाँ लहरे साहिल से टकराकर शांत हो जाएँ
तुम उन लहरों की आवाज़ के साथ अपना सुरूर पाओ
और मैं उनके आने-जाने में कोई फलसफे तलाश लूँ
या देख लूँ बहते पानी में अपना चेहरा
या उन्हीं लहरों में रख कर पाँव बिता दूँ एक रैन
या आओ बस चलें उस लंबी अनजान सड़क पर
जहाँ हो बस ऊँचे पेड़ों से सजा रास्ता
ना हो कोई और सफरतरीन गाड़ी
बस हो बहुत सी चिड़ियों की चहचहाट और ठंडी हवा
एक बिना मंज़िल का सफर और न कहीं पहुँचने की जल्दी
या आओ यहीं तलाशें वो राहत
बस कुछ दिन अपने ही घर की बालकनी में रोज़ सुबह एक शांत सी चाय पिएँ
ना घर दफ्तर की बातें करें
बस रोज़ एक कोरे कागज़ से दिन शुरू करें
मन की सुने और बस जो अच्छी हो वही कहें
एक ना-उजागर सी सोच
कभी सोचा है क्या ये भी के
घड़ी के दो टिक-टिक के बीच भी गुजरता है एक पल
जो महसूस नहीं होता
जो सुनता नहीं कोई
हर बंदिश में होता है ऐसा एक साज़ भी
हर खूबसूरत नक्श के पीछे भी छुपे होते हैं कुछ रंग शायद
और जो प्यास ना बुझा पाई हो किसी की
होती है हर प्याले के आखिर में ऐसी कुछ बूंदें भी
होते हैं ऐसे ही कितने अनसुने अनदेखे हिस्से हर कहानी के
जो होते हैं तो पता नहीं चलते
पर न हो तो लगती है कुछ कमी सी
ये वो कमी होती है जिसकी कोई तफसीर नहीं होती
पर कहते हैं ना “कुछ तो कमी थी”
तो क्यों न कभी उन ना-उजागर हिस्सों, पलों और लोगों के ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो अर्ज की जाए
क्या पता वो कब ना हों और “कुछ कमी सी” लगने लग जाए…

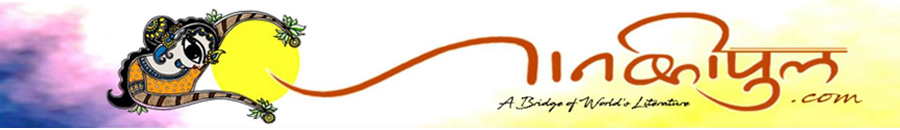

1 Comment
बहुत सुंदर