मनोज रुपड़ा हमारे दौर के बड़े विजन वाले लेखक हैं। उनके उपन्यास ‘काले अध्याय’ के बारे में हाल में वरिष्ठ लेखक धीरेंद्र अस्थाना ने लिखा था कि भारतीय ज्ञानपीठ से उपन्यास के तीन संस्करण आ गया लेकिन इसकी वैसी चर्चा नहीं हुई जैसी कि होनी चाहिए थे। पिछले दिनों यतीश कुमार ने एक फ़ेसबुक पोस्ट में लिखा था कि एयरपोर्ट पर वह इस उपन्यास में ऐसे डूबे कि उनकी फ़्लाइट छूट गई। बहरहाल, मनोज रुपड़ा के उपन्यास ‘काले अध्याय’ पर पढ़िये यतीश कुमार की टिप्पणी- प्रभात रंजन
=================================
किताब को पढ़ते समय बस एक विशुद्ध पाठक बन गया हूँ। जो सिर्फ़ प्राप्ति की आकांक्षा से पंक्ति दर पंक्ति किताब में डूबता जा रहा है। इसे समीक्षा क़तई मत समझियेगा। यह कुछ नोट्स और पाठकीय प्रतिक्रिया के बीच की कोई चीज़ है, कभी कुछ चुन लिया तो कभी गुन लिया माफ़िक़!
पढ़ते हुए लगेगा प्रकृति की चीजें अँगियाती हैं और अर्पित हो जाती हैं। लाफ़ानी लय के लिए तरसते हुए आदमी रचना के संसार में प्रवेश करता है और फिर उसे महसूस होता है कि समय के अंतराल में सिर्फ़ दृष्टि बदलती है, चीजें नहीं। उपन्यास से गुजरते हुए एक बात तो पक्का महसूस होगा कि विखंडन एक शाश्वत क्रिया है। यथार्थ की जटिलताएँ यहाँ एक बद्ध बींधी मिलेंगी जिसकी तहें उधेड़ते हुए लेखक की तटस्थता आपको अचंभित कर देगी ।
यादें लहरों की तरह आती हैं, एक के बाद एक। एक बारगी आ जाती हैं तो लहरों से नहीं, थपेड़ों से मुलाक़ात होती है। जाना अपने पीछे सम्मोहन की छाया छोड़ जाता है, और जाती हुई आवाज़ों का सम्मोहन और तीव्र! पढ़ते हुए इस बात को भी समझ पायेंगे कि कल्पना से ज़्यादा बड़ी वास्तविकता भी हो सकती है।
एक पूरा भरापूरा जीवन कैसे महाभोज के निमंत्रण में ख़ुद के शरीर को अर्पित कर देता हैं, उसकी अकल्पनीय तस्वीर खींची गई है इस किताब में। दिल दहलते हुए भी सोचता है कि कमबख़्त सबसे ख़तरनाक तो नींद है, जो रोज़ मृत्यु की ओर बढ़े कदम की घण्टी ही तो है। नींद ने क्या उस महाभोज को भी निगल लिया? एक उत्तर है लेखक के पास इन सभी अनुत्तरित सवालों का, कि दार्शनिक भाव ऐसे महाभोज को देखते हुए आये तो बेहतर, नहीं तो पूरी ज़िंदगी, वह बूढ़ा लकड़बग्घा पीछा नहीं छोड़ता। छूट गया कंकाल और साथ में ली गई कुल्हाड़ी, दोनों पीछा नहीं छोड़ते। वो अंतिम निगाह अब उसके साथ है, उसके व्यक्तित्व में रोपित निगाह की तरह, और यूँ महावत का साथी अपनी अंतिम निगाह की छाया छोड़ते हुए विलीन हो गया।
लेखक जिस विचारहीनता की बात करता है, जिसके बिना आदमी जानवर समान है उससे पता नहीं क्यों, मैं इत्तिफ़ाक़ नहीं रख पा रहा। लेखक से नहीं इस तथ्य से कि क्या जानवर के पास सच में विचार नहीं?
खामोशी कितनी घातक है यह उस बहन से मिलकर समझा जा सकता है। ममता के कैसे-कैसे नाटक होते हैं, यह माँ की हरकतें बता सकती हैं। समझा जा सकता है कि कैसे ख़ाली पेट की हलचल पानी के घूँट निर्धारित करते हैं। जंगल बहन के असुरक्षाबोध से कैसे और घना हो जाता है और नायक उस घने में दो जुगनू बराबर रोशनी भरी चिंगारी की तलाश में भटकने निकल पड़ता है।
पढ़ते हुए आप भी लेखक की तरह ठिठक कर ख़ुद से कहेंगे कि सच ही तो है कि पगडंडी को सड़क से जोड़ने के लिए किसी न किसी को तो पहली बार चलना पड़ा होगा। फिर इसके बाद यह समझना और आसान हो जाता है कि एक बार कोई चल ले तो फिर पीछे चलने वाले पूरी ज़िंदगी उसे दोहराते हैं, पगडंडी का समतल और सुदृढ़ होता जाता है। यूँ चलना राह बनाना बन जाता है। पगडंडियाँ रास्तों से मिल ले तो सुंदर पर पगडंडियाँ जब रास्ता बन जाएँ तो जंगल की रूह काँप जाती है। लाठी का आक्रमण के हथियार के बदले सुरक्षा की ढाल बनना, चिंतनीय स्थिति है। जंगल में खोना अलग बात है और जंगल में चले जाना अलग। कई राह होने से ज़्यादा ज़रूरी है आपको यह पता होना कि किस दिशा में जाना है। भला आख़िरी सीढ़ी से नीचे उतरना सबको कहाँ आता है!
इस उपन्यास के दो किरदार थोड़े अलग से हैं। एक है खामोशी और दूसरा जुनून। आप अक्सर पायेंगे कि खामोशी में जुनून अपनी हदें पार करने लगता है, तब खामोशी अपनी आँखें बंद कर लेती है और आँखों के संवाद विलोप में बदल जाते हैं। नींद और विचार के गुत्थमगुत्थी होने में कल्पना की झीनी चदरिया अपने धागे उधेड़ने लगती है और फिर पशुवत् अचेतनता घर बनाने लगती है और फिर नायक सफ़र पर निकल पड़ता है।
समझ में आएगा कि क्यों गति को परिवेश से नफ़रत है। जितनी तेज गति उतना कम उस जगह की ख़ुशबू का मिलना। हाई स्पीड रेल आयी तो क्या होगा ये सोच रहा हूँ, यहाँ तो लेखक पैडल वाले रिक्शा और ऑटो के अंतर से ही परेशान है। बासामुड़ा की पगडंडी का सड़क बनना कृत्रिम विकास का संकेत है। यह समझना होगा कि यह अनचाहा है या मनचाहा।
इस किताब को पढ़ते हुए यह महसूस हो रहा है जैसे जंगल नहीं, महाभारत को समझ रहा हूँ। पांडव-कौरव दोनों के हाथों में अब बंदूक़ें हैं। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और दोनों ओर आदिवासी ही हैं जो भाई हैं या बचपन के दोस्त ही हैं। कारण और कारक के साथ जंगल में सबकुछ बदलता जा रहा है, बस एक हिंसा तत्व को छोड़कर। एक दृश्य पर आकर थोड़ा हाँफने सा महसूस करने लगा। जब किसी को अपना पुतला ही शहीद के तौर पर सामने खड़ा दिखे तो उस मनःस्थिति में जाकर वापस आने में वक्त तो लगता है। मिनट तब मिनट नहीं रहता, कालखण्ड बन जाता है, तब उसे समेटना भी उतना ही दूभर हो जाता है। मनोज रुपड़ा ऐसा कर पा रहे हैं। काल को पकड़ कर शब्द में बदल देने की इस अद्भुत कला का अब मैं कायल हो चुका हूँ।
किताब में रह-रह कर हृदयविदारक दृश्य हैं, जो पढ़ते हुए भीतर विस्फोटक की तरह बज उठते हैं और फिर आधे-अधूरे स्फुट विचारों की भगजोगनी चारों ओर बिखरी पड़ी मिलेंगी आपको। किसे समेटूँ, किसे कुचलते हुए निकल जाऊँ! परंतु अभी भी जीवन और मृत्यु को एक पल एक साथ देखने के दृश्य में बींधा पड़ा हूँ। वे चूज़ें जो विस्फोट के समय निर्विकार चैतन्य की दृष्टि लिए ताक रहे थे, वैसी तटस्थता कहाँ से आएगी भला। अंतिम ज्ञान यही है कि जंगल अपने भीतर घटती तमाम क्रूरताओं के बावजूद, अपनी निरंतरता में मग्न है और इंसान एकांत में भी सल्फ़ी का टपकता रस पी कर मस्त है।
जीवन में जब स्पष्टता आ जाती है, तब व्याख्यान की ज़रूरत सिमट जाती है। कम शब्दों में सटीक बात पूरे आत्मविश्वास से कह कर आदमी सहजता के साथ आगे निकल जाता है। जैसा उस सीनियर केडर ने किया। मनुष्य, आदम को कैसे और किन परिस्थितियों में कीड़ा मकोड़ा समझने लगता है, किन मौक़ों में धर्म और मज़हब एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, कैसे मानवता का लिंग काटकर सभ्यता को नंगा कर दिया जाता है, करुणा के चिथड़े उड़ाये जाते हैं, त्रासदी सामान्य घटना हो जाती है, कैसे सरहद सिसकियाँ लेता दिखता है और हिमालय अपना सिर छुपाता नज़र आता है। यह सब इस किताब में यूँ दर्ज है जैसे आपके सामने सब घट रहा हो और आप लगातार सिहरते जाते हैं, सिकुड़ते जाते हैं और सिहरते-सिकुड़ते हुए इसे पढ़ते जाते हैं।
सम्मिलित भाषा का वह जादू, जो सड़क पर गिरे पेड़ को हटाते हुए गूंजा था, वही समवेत स्वर पूरे वातावरण में छाया रहे पढ़ते समय, मैं ऐसी प्रार्थना कर रहा हूँ। सड़क बनाने और न बनने देने के बीच का युद्ध रुक जाये। विस्थापन का ऐसा दंश जिसमें इंसान गोटियाँ बनता जा रहा हैं अतिशीघ्र बंद हो जाये और हे ईश्वर! बुझी और डूबी हुई इंद्रियाँ आप्लावित हो कर साँस लेने लगें और सीना पिरोने का क्रम जल्द से जल्द बंद हो।
अंत में इतना ही कहूँगा कि बिखराव का सिमटना एक शुभ संदेश है और शुभ संदेश है बंदूक़ की नली में फूल लगाना । भाषा में विशिष्टता, शब्दों का चयन, वाक्यों की बुनावट और समय में आने जाने का अनूठा अनुक्रम इस उपन्यास को अत्यंत पठनीय बनाता है। ज़रूरी विषय होने के साथ-साथ यह समय के सच को भी पूरी नग्नता के साथ प्रस्तुत कर रहा है, जो एक ईमानदार मौलिक लेखक ही कर सकता है। बिना उस मिट्टी में धँसे मुश्किल है ऐसे बीज रोपना, जो यूँ फलीभूत होकर आपसे मिले। मनोज ऐसे उपन्यास लिखते रहें और हम जैसे पाठक उन्हें पढ़ते हुए फ्लाइट छोड़ते रहें।
नोट- इस उपन्यास को पढ़ते हुए मेरी लखनऊ की फ्लाइट छूट गई, जबकि मैं समय से एक घण्टे पहले से गेट नंबर 105 पर बैठा था।



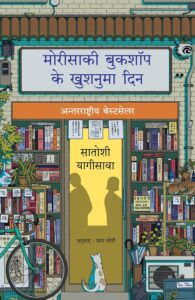
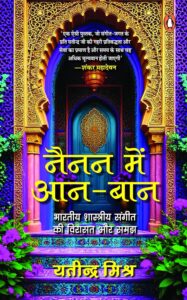
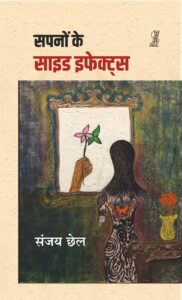

शानदार और जानदार टिप्पणी भाई यतीश जी, और मनोज रूपड़ा जी को फिर से बधाई। मैं पढ़ रहा हूँ।