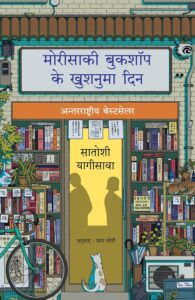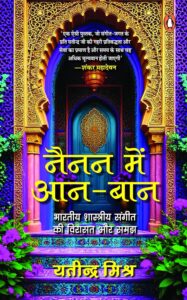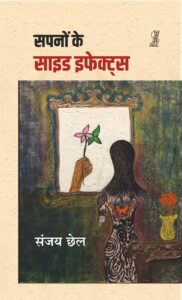विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास ‘दीवार में एक खिड़की रहती थी’ की यह समीक्षा उपन्यास की आरंभिक समीक्षाओं में है जिसे मैंने लिखा था। यह महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की पत्रिका ‘बहुवचन’ में प्रकाशित हुई थी। पत्रिका के प्रथम संपादक पीयूष दईया ने 1999 में मुझसे यह समीक्षा लिखवाई थी। आप भी पढ़ सकते हैं- मॉडरेटर
==============================
महाराज
यह वह अमरावती नहीं कोई और
अमरावती है।
अमरावती है।
(मगध श्रीकान्त वर्मा )
‘शहर फैलते-फैलते नज़दीक के गाँव तक पहुँचता तो गाँव शहर का मुहल्ला बन जाता था। गाँव का नाम मुहल्ले का नाम हो जाता था। जोरा गाँव आठ किलोमीटर दूर था इसलिए जोरा गाँव नाम का मुहल्ला नहीं बना था ( दीवार में एक खिड़की रहती थी )।
विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास ‘दीवार में एक खिड़की रहती थी’ में वे तमाम संकेतक मौजूद हैं जिनके आधार पर हम चाहे तो उसे ‘हाशिए का एक रूपक कह सकते हैं। विकास कथा में छुटे हुओं का रूपक दूसरी तरफ उपन्यास के पाठ में उपस्थित कथा के आधार पर हम चाहें तो यह कहने के लिए भी स्वतन्त्र हैं कि उपन्यास ‘सामान्यीकरण’ के इस दौर में ‘विशेष’ के रोज़मर्रेपन की एक साधारण कथा है जिसे एक असाधारण भाषा में गढ़ा गया है। यह उपन्यास की एक बड़ी विशेषता मानी जाएगी कि इसमें अभिव्यंजकों की एक ऐसी श्रृंखला रची गयी है जो पाठकों को परस्पर विरोधी अर्थों के सञ्जाल का हिस्सा बना देती हैं।
उपन्यास की भाषा में लेखक एक ऐसी दुनिया की ‘उपस्थिति दर्ज कराता है जो धीरे-धीरे परिदृश्य से ओझल होती जा रही है। उपन्यास की कथा में नायक रघुवर प्रसाद हैं, जो कि एक निजी महाविद्यालय में व्याख्याता हैं। कुल आठ सौ रुपये वेतन पाते हैं। उनकी कथा को पूरा करती है उनकी पत्नी सोनसी की कथा। घर परिवार और तमाम पड़ोस के बावजूद उपन्यास में मुख्यतः उनकी ही कथा है। भले ही उसमें हाथी और साधू, विभागाध्यक्ष आदि की कथाएँ भी आती जाती हैं, लेकिन उपन्यास की दुनिया उनके मुताबिक ही चलती हैं। देखने में तो उनकी एक साधारण-सी दुनिया है, कुल एक कमरे और एक तालाबन्द टट्टी की दुनिया। लेकिन उस साधारण सी दुनिया में एक खिड़की भी है, अक्सर कथा उसके पार भी चली जाती है। उस पार की दुनिया में स्वच्छ तालाब है; हरे पेड़ हैं। फुलचुक्की चिड़िया है, लम्बी पूँछवाली शाह बुलबुल है। उस दुनिया में ‘अल्पना की मछली जल में तैरती’ दिखायी देती है। एक बूढ़ी अम्मा है जो कभी चाय पिलाती है, तो कभी बताशे खिलाती है। और कभी हँसते-हँसते सोनसी को सोने के कड़े भी दे देती है। लेकिन इस दुनिया में, इस निष्कलुष दुनिया में सबका प्रवेश सम्भव नहीं। एक दिन जब विभागाध्यक्ष, रघुवर प्रसाद की अनुपस्थिति में उस कमरे की खिड़की के उस पार की दुनिया की तलाश में निकलते हैं तो उसे ढूँढ नहीं पाते हैं। उस दुनिया में स्वतन्त्रता की सत्ता (Power of Freedom) है, जहाँ हर वस्तु की नामहीन उपस्थिति है यानी जिस पर सांसारिक पहचानों का आवरण नहीं है।
इस पार की दुनिया में रघुवर प्रसाद सोचता है ‘उसका वेतन अच्छा होता तो वह बताता कि एक पुत्र अपने पिता की किस प्रकार परवाह करता है।’ पिता की बन्द आँखों में ‘बेटे की गृहस्थी की खटर-पटर’ का सुख है, सोनसी है, माँ है, छोटू है, स्कूटर वाले विभागाध्यक्ष हैं, टेम्पो की भीड़भाड़ है, नीलकण्ठ देखने की अधूरी इच्छा है और सबसे बढ़कर हाथी पर सवार साधु है। यानि यह एक ऐसी दुनिया है जिसमें ‘सामाजिक व्यवस्था की सत्ता’ (Power of Regime) है। ये कथायें साधारण सी दिखने वाली कथा में असाधारणता पैदा कर देते हैं। उपन्यास में ‘जो है’ की कथा बार-बार ‘जो नहीं है’ की कथा की तरफ ले जाती है और उसे गहरे अर्थ-संकेतों से भर देती है। यह विनोद कुमार शुक्ल की विशेषता है। उनकी कविताओं में भी भूले हुओं का सन्दर्भित स्मरण होता है।
कथा में इन दो दुनियाओं के परस्पर विरोध की अन्तर्पाठीयता चलती रहती है। परस्पर विरोध उस अर्थ में जिस अर्थ में उपन्यासों को ‘पैराडॉक्सिकल’ कहा जाता है। वह ‘पैराडॉक्स’ ही इस उपन्यास की एकरेखीय -सी दिखने वाली कथा को बहुअर्थीय बनाता है। यह ‘पैराडॉक्स’ बाहर की दुनिया और खिड़की के उस पार की दुनिया जिसकी सारी जगह रघुवर प्रसाद के मन की जगह थी। गोबर की लिपी पगडंडी मन की पगडंडी थी । साफ-सुथरा आकाश उड़ने के लिये मन का आकाश था’ के द्वन्द्व में और भी स्पष्ट होता है। अमरीकी उपन्यासकार ई. एल. डॉक्ट्रो ने उपन्यास को ‘प्राईवेट आई’ (1) कहा है, कुछ वैसा जो लिखा नहीं जाता। इस उपन्यास में दो दुनियाओं का द्वन्द्व कुछ वैसा ही ‘प्राईवेट आई (1)’ और ‘पब्लिक आई (I)’ के बीच का द्वन्द्व है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे ‘प्राईवेट आई’ एक लम्बी कथा – यात्रा पर निकल गया हो जिसमें ‘कितने दिन हो गए को कितने हो गए में ही रहने देना चाहिये। दिन को गिनती में नहीं समझना चाहिये। किसी को भी नहीं गिनती चारदिवारी की तरह है जिसमें सब मिट जाता है। अन्तहीन जैसे का भी गिनती में अन्त हो जाता था।’
विश्व- गाँव में बदल चुके संसार में यह उपन्यास अपनी कथा यानी भाषिक-संसार में एक ऐसे ‘स्पेस’ को पकड़ने की कोशिश है जिसे हम अब तक एक ‘सामान्य’ के रूप में ही गढ़न में समझते आए हैं- अलग-अलग वर्गों के ‘सामान्य’ के रूप में। इन विराट रूपकों के जो कुछ छूट गया है उस ‘स्पेस’ को पकड़ने का प्रयास करता दिखायी देता है उपन्यासकार। उपन्यास का आरम्भिक वाक्य है- ‘हाथी आगे-आगे चलता जाता था और पीछे हाथी की जगह छूटती जाती थी।’ हाथी यानि विशाल रूपकों को देखते-देखते हम व्यक्ति के सामान्य रोज़मर्रेपन को भूल गये। उसके निजीपन को भूल गये। विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास जैसे उसी की याद दिला रहा हो। उपन्यास की प्रस्तावना में उपन्यासकार ने एक कविता लिखी है- ‘उपन्यास में पहले एक कविता रहती थी जिसका अन्त होता है इन पंक्तियों में ‘अनगिन से अकेली एक संगिनी जीवन भरा’ हिन्दी में यथार्थवादी उपन्यास की धारा बहुत कुछ ‘गज़ट लेखन’ की तरह रही है जिसमें नामों पहचानों की प्रधानता रहती है, व्यक्ति का अपना कुछ छूट जाता है। यह उपन्यास जैसे बड़े-बड़े रूपकों की विदाई का संकेतक बन जाता है।
यह अकारण नहीं है कि उपन्यास में साधू एक दिन अचानक ही बनारस चला जाता है और उसके बाद रघुवर प्रसाद जाकर हाथी की जंजीर खोलकर उसे आज़ाद करा देते हैं; शासन की सत्ता से मुक्ति दिलाकर स्वतन्त्रता की सत्ता का आनन्द उठाने देने के लिये। आश्चर्य कि उसके बाद हाथी किसी को नहीं दिखता। हाँ, रघुवर प्रसाद ज़रूर ‘हाथी के आने की दिशा एक साधू को साईकिल पर आते’ देखते हैं। जैसे महानगरों में किसी बड़े पुल के नीचे किसी बस्ती के बाहर यह बोर्ड टँगा रहता है ‘यहाँ हाथी रहते हैं।’ यानि हाथी एक कौतुक होकर रह जाता है, शोभा की वस्तु होकर। हमारे दैनन्दिन जीवन में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता। उपन्यास में रघुवर प्रसाद भी अपने दैनन्दिन जीवन में हाथी के साथ संगति बिठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस क्रम में अपने-आपको असफल पाते हैं । अन्ततः टेम्पो और साईकिल से ही उनकी दैनन्दिन संगति बैठती है। शायद इसी कारण खिड़की के उस पार की दुनिया में हाथी का प्रवेश नहीं हो पाता – ‘मन की खिड़की और बड़ी होती तो ठीक था। मन का हाथी बड़ा है।’
यह उपन्यास स्वप्न और यथार्थ के बीच की असंगति का पाठ नहीं दिखायी देता, बल्कि उनके बीच की संगति ढूँढने की एक कोशिश की तरह लिखा गया है। हमारा संसार सिर्फ ‘सच’ का संसार नहीं होता, बल्कि उसमें हमारे छोटे-छोटे सपने भी रहते हैं । उपन्यास में विडम्बना का स्वर नहीं दिखायी देता है, बल्कि विरोधधर्मियों में संगति बिठाने की कोशिश ही अधिक दिखती है । यहाँ बने बनाए साहित्य – सिद्धान्त इस उपन्यास के ‘पाठ’ को किसी भी रूप नहीं पकड़ पाते, बल्कि हर प्रकार की शास्त्रीयता इस उपन्यास की कथा के सामने लाचार दिखायी देती है। इसी कारण खिड़की के बाहर की दुनिया अम्बर्टो इको के ‘सिटी ऑफ रोबोट्स’ के ‘फैंटेसीलैंड’ की ‘डिजाईनर’ दुनिया जैसी नहीं दिखती है, बल्कि वह मनुष्य की सम्पूर्णता की सामूहिक इच्छा का विस्तार ही दिखाई देती है।
अमरीकी उत्तर-संरचनावादी जे. हिलिस मिलर ने कहीं कहा कि ‘अगर नयी दुनिया में कोई ईश्वर है तो उसे सांसारिक वस्तुओं के भीतर ही होना चाहिए न कि उससे बाहर कहीं दूर ।’ विनोद कुमार शुक्ल की आस्था सुन्दरता में दिखायी देती है । उपन्यास में भविष्य की डिस्टोपियाई कल्पना नहीं है, बल्कि इसमें यह विश्वास मौजूद है कि भविष्य में दुनिया में सुन्दरता बची रहेगी। इसीलिए उनके अन्य उपन्यासों की तरह यहाँ भी स्थित निश्छल बच्चे अपनी किलकारियों और बदमाशियों के साथ उपस्थित दिखायी देते हैं। शायद यही कारण कि उपन्यास में बच्चे रघुवर प्रसाद के घर में सामने नहीं खिड़की झाँकते हैं यानी दूसरी दुनिया से और खिड़की से आकाश दिखता, इसलिए खिड़की से झाँकते हुए बच्चे आकाश से झाँकते हुए लगते थे। वे छोटे-छोटे देवता की तरह खिड़की से कूदकर अन्दर आना चाहते थे।’
वैलेस स्टीवेन्स की एक प्रसिद्ध कविता है ‘नॉट आईडियाज़ अबाउट द थिंग बट द द ईटसेल्फ’ जिसके अन्त में एक नए यथार्थ के ज्ञान की बात की गयी है। उपन्यास में दोनों संसारों की सम्बद्धता-असम्बद्धता यथार्थ की एक नयी भाव-भूमि की ओर ले जाती है, जो निश्चय ही हिन्दी उपन्यास – साहित्य की एक नयी भाव – भूमि है। उपन्यास में कथा ही नहीं भाषा भी कई स्तरों में उपस्थित है, भाषिक संसारों की अलग-अलग संरचनाएँ। रघुवर प्रसाद, सोनसी, विभागाध्यक्ष, बच्चे, साधू, पिताजी सबकी अपनी-अपनी भाषिक दुनिया है-
समझ गया। पर सर। गाय एक समय पालतू नहीं रही होगी। वह भी जंगली जानवर होगी। मनुष्य जंगली था। भालू भी धीरे-धीरे पालतू हो जाता।’
“थक गए तो एक टिपरिया चाय की दुकान में चाय पी।”
“थक गए तो एक खण्डहर जैसी पुरानी सराय में केसरिया दूध पिया- पत्नी ने सुना।”
‘अच्छी गरम चाय थी।’
‘गाढ़ा गरम दूध था पत्नी ने सुना।’
“थक गए तो एक टिपरिया चाय की दुकान में चाय पी।”
“थक गए तो एक खण्डहर जैसी पुरानी सराय में केसरिया दूध पिया- पत्नी ने सुना।”
‘अच्छी गरम चाय थी।’
‘गाढ़ा गरम दूध था पत्नी ने सुना।’
मैं कहाँ हूँ?’ रघुवर प्रसाद ने कमरा झाँकते हुए सोनसी से पूछा, जैसे कमरे से पूछा। “मेरे पास हो।” कमरा झाँकते हुए सोनसी ने कहा, जैसे कमरे ने कहा ।
तुम ‘और मैं!’ खाली कमरा देखते हुए सोनसी ने आश्चर्य से कहा।
‘तुम यहाँ मेरे पास हो।’ रघुवर प्रसाद ने कहा, इसके बाद दोनों कमरे में कूद गये।’
इन छोटे-छोटे निजी भाषिक-अनुभवों से उपन्यास की कथा में निजत्व आता है। यह एक विरल भाषा है, जो विनोद कुमार शुक्ल के प्रयोगों में जीवन्त हो उठी है। कहीं-कहीं तो वह कविता का आनन्द दिलाती है। यह भाषा निश्चय ही हिन्दी कथा – साहित्य की उपलब्धि कही जा सकती है।
कुल मिलाकर इस उपन्यास का संसार एक अभाव के जीवन की दुख की कथा नहीं है, बल्कि उसमें अभावों से भरे जीवन के छोटे-छोटे सुखों के बेजोड़ संस्मरण हैं जिसमें प्रेम और अपनेपन का सम्मिश्रण दिखाई देता है । उपन्यास ‘आज की सुबह’ के वर्णन से शुरू होता है और एक सबेरे समाप्त हो जाता है। इस बीच उपन्यास में अनेक दिन-रातों के सपने है। भूले-भटके प्रसंग हैं। दांपत्य-जीवन है और उसके तमाम प्रसंग हैं- प्रेम और विरह के प्रसंग ‘दरवाजा खोलकर वे आकाश को देख लेते थे, सोनसी की चिट्ठी है। सोनसी भी देख लेती होगी कि रघुवर प्रसाद की चिट्टी है। कभी आकाश में बहुत तारे । कभी इक्के-दुक्के दिखाई देते।
इक्के-दुक्के तारों का आकाश लिखने का समय नहीं मिला जैसा या थोड़ी-थोड़ी लिखी जा रही चिट्टी जैसा था।’
दाम्पत्य-जीवन का ऐसा प्रेम और ऐसा विरह लेखक की जीवन में आस्था का पाठ ही बनाता दिखायी देता है जो इस ‘सिनिकल’ बनाने वाले समय में जीवन को जीने लायक जगह बनाने का सन्तोष देता है। यह एक ऐसी दुनिया है जिसकी सम्भावना अब भी नष्ट नहीं हुयी है।
तुम ‘और मैं!’ खाली कमरा देखते हुए सोनसी ने आश्चर्य से कहा।
‘तुम यहाँ मेरे पास हो।’ रघुवर प्रसाद ने कहा, इसके बाद दोनों कमरे में कूद गये।’
इन छोटे-छोटे निजी भाषिक-अनुभवों से उपन्यास की कथा में निजत्व आता है। यह एक विरल भाषा है, जो विनोद कुमार शुक्ल के प्रयोगों में जीवन्त हो उठी है। कहीं-कहीं तो वह कविता का आनन्द दिलाती है। यह भाषा निश्चय ही हिन्दी कथा – साहित्य की उपलब्धि कही जा सकती है।
कुल मिलाकर इस उपन्यास का संसार एक अभाव के जीवन की दुख की कथा नहीं है, बल्कि उसमें अभावों से भरे जीवन के छोटे-छोटे सुखों के बेजोड़ संस्मरण हैं जिसमें प्रेम और अपनेपन का सम्मिश्रण दिखाई देता है । उपन्यास ‘आज की सुबह’ के वर्णन से शुरू होता है और एक सबेरे समाप्त हो जाता है। इस बीच उपन्यास में अनेक दिन-रातों के सपने है। भूले-भटके प्रसंग हैं। दांपत्य-जीवन है और उसके तमाम प्रसंग हैं- प्रेम और विरह के प्रसंग ‘दरवाजा खोलकर वे आकाश को देख लेते थे, सोनसी की चिट्ठी है। सोनसी भी देख लेती होगी कि रघुवर प्रसाद की चिट्टी है। कभी आकाश में बहुत तारे । कभी इक्के-दुक्के दिखाई देते।
इक्के-दुक्के तारों का आकाश लिखने का समय नहीं मिला जैसा या थोड़ी-थोड़ी लिखी जा रही चिट्टी जैसा था।’
दाम्पत्य-जीवन का ऐसा प्रेम और ऐसा विरह लेखक की जीवन में आस्था का पाठ ही बनाता दिखायी देता है जो इस ‘सिनिकल’ बनाने वाले समय में जीवन को जीने लायक जगह बनाने का सन्तोष देता है। यह एक ऐसी दुनिया है जिसकी सम्भावना अब भी नष्ट नहीं हुयी है।