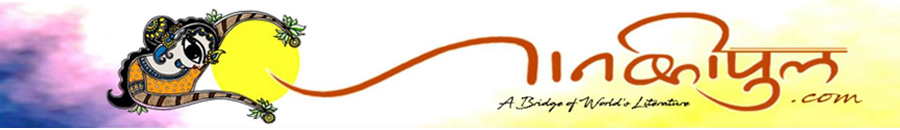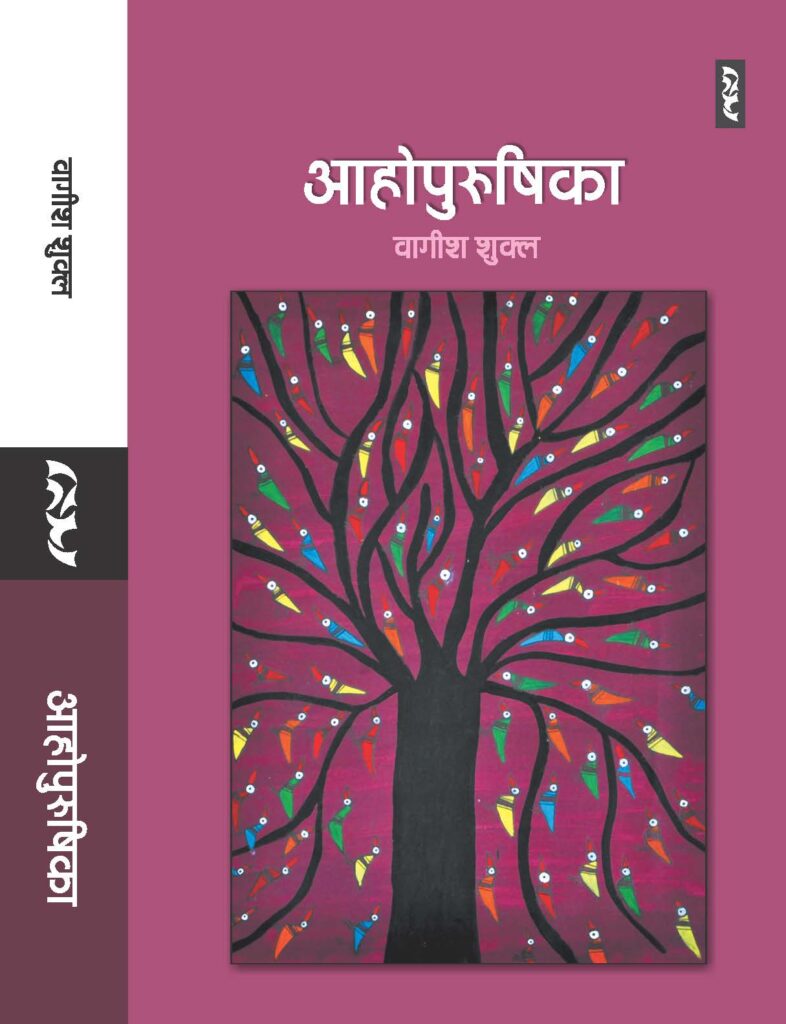वागीश शुक्ल अपने अद्वितीय निबन्धों, टीकाओं और अपने लिखे जा रहे उपन्यास के लिए प्रसिद्ध हैं। वे सम्भवतः हिन्दी के अकेले ऐसे लेखक हैं जो हिन्दी के अलावा अंग्रेज़ी, संस्कृत, फ़ारसी और उर्दू पर समानाधिकार रखते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा में बहुकोणीय समृद्धि अनुभव होती है। उनकी नवीन पुस्तक ‘आहोपुरुषिका‘ सनातन धर्म में विवाह पर विस्तृत चर्चा है।
पुस्तक की परिचयात्मक टिप्पणी मृदुला गर्ग के शब्दोँ मेँ :
आहोपुरुषिका की विषाद झंझा उसका एक तिहाई हिस्सा है। बाकी दो तिहाई में, विवाह सूक्त का शास्त्र सम्मत और अत्यन्त विद्वत्तापूर्ण विवेचन है। सनातन धर्म में जहाँ वह देवानुप्राणित कौटुम्बिक कर्म है, वहाँ अब्राहमी धर्मों में; ईसाई, मुस्लिम व यहूदी; व्यक्ति विशेष से सम्बन्धित कर्म है, पर मजे की बात यह है कि उसका पूरा अनुष्ठान व चयनित व्यक्ति; चर्च, पादरी व परिवार निर्धारित करते हैं। तमाम शास्त्र सम्मत विवेचना के बावजूद, सनातन विवाह सूक्त में कुछ दिलचस्प और क्रान्तिकारी लगते तथ्य भी हैं। लिखा है, ‘लिव इन’ पद्धति से कोई परहेज नहीं है, बशर्ते वह लोकाचार का हिस्सा बन चुकी हो !
मुझे जो वाक्य विशेष रूप से याद रह गये, वे थे : शब्द के रूप में ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है। जब सृष्टि हो जाती है तो वह प्राणियों की देह के भीतर अर्थ के रूप में विस्तृत हो जाता है। समागम में प्रेक्षण ही है जो काम को सनातन में उसे धर्म और अर्थ के समकक्ष पुरुषार्थ के रूप में स्थापित करता है। कामसूत्र का यह पद; स्त्री को भोग्या होने का अभिमान होता है, पुरुष को भोक्ता होने का। किन्तु अभिमान एक ही है।
शायद इसीलिए परम स्थिति वह है जब पति-पत्नी में अभेद हो।
आहोपुरुषिका को महत्त्वपूर्ण साहित्यिक कृति मानते हुए प्रचण्ड प्रवीर का संक्षिप्त आलेख पाठकोँ के लिए-
****************************
आजकल की साहित्य चर्चा मेँ बहुचर्चित प्रश्न होता है गम्भीर और लोकप्रिय साहित्य। इसमेँ अधिकतर विद्वान लोकप्रिय साहित्य की व्याख्या और मुख्यधारा मेँ उसकी उपस्थापना के लिए प्रयासरत नजर आते हैँ। वहीँ गम्भीर के सम्बन्ध मेँ किसी के पास कोई योजना नज़र नहीँ आती। जिसे आमतौर पर गम्भीर कहा जा रहा है, वह मेरी दृष्टि मेँ नीमहकीमी है। कड़वे किन्तु सीधे लफ्जोँ मेँ यह कहा जाना चाहिए कि हमारी आधुनिक कविता और कहानी का बहुलांश जिसे हिन्दी के कुछ पत्रिकाएँ और स्वनामधन्य ‘पत्रकार-बनाम-साहित्यकार’ मुख्यधारा मेँ स्थापित करते हैँ वह दरअसल बोझिल, उबाऊ, चलताऊ ही नहीँ अपितु दोयम दर्जे का भी है। गम्भीर का अर्थ दुरूह होना नहीँ होता, न ही उसका अनर्गल होना होता है। उपदेश देना या झण्डा फहराना गम्भीरता के नहीँ बल्कि ‘क्रियमाणता’ के गुण हैँ, जो बहुधा आह्वान और पालन की स्थिति मेँ दास मानसिकता के परिचायक हैँ। यह बहुत हद तक फतवा जारी करना और उसके अमल मेँ मर मिटने का सिद्धान्त है।
बहुत विस्तार मेँ जाने की अपेक्षा मैँ केवल दो बातेँ कह कर अपनी बात प्रारम्भ करूँगा। पहली बात यह कि पारम्परिक साहित्य मेँ शब्द अलङ्कारोँ मेँ श्लेष और अर्थ अलङ्कारोँ मेँ उपमा श्रेष्ठ मानी जाती है। हमने आधुनिक साहित्य मेँ ‘ध्वनि’ के साथ-साथ, अलङ्कारोँ को भी तिलाञ्जलि दे दी है। उसमेँ भी श्लेष अलङ्कार विस्मृत कर दिया गया है। ऐसी विस्मृति सामूहिक प्रयासोँ से सम्भव हुई है, जिसने अभिधाशक्ति को मुख्यता अपनी अहमान्यता से और अर्जित मूर्खता से प्रतिपादित की है। दूसरी बात यह कि गाम्भीर्य का अर्थ श्रमसाध्य ही समझा जाए तो हिन्दी के तमाम फुटपाथी आलोचक, जिन्हेँ किताबेँ चुन लेती हैँ, जो पानी पी-पी कर पितृसत्ता और ब्राह्मणवाद को कोसते हैँ (वह इसलिए कि इस सारहीन संसार मेँ जो कुछ भी अधर्म है, वह इसी मेँ समाहित है – इस तरह की प्रतिपादित परिभाषा से ही सिद्ध), वे लम्बे श्रम के उपरान्त लिखी गई आनन्द कुमार सिंह की ‘अथर्वा: मैँ वही वन हूँ’ हाथ लगाने से पहले सौ बार सोचेँगे कि ऐसा करने मेँ उनकी निरर्थकता, अज्ञानता और टुच्चापन प्रकट न हो जाए। यह टिप्पणी ‘अथर्वा’ की प्रशंसा मेँ न हो कर दुष्कार कार्य की सिद्धि मेँ हाथ गन्दे न करने को प्रवृत्ति को लेकर हैँ क्योँकि आज का ‘साहित्यकार बनाम आलोचक’ अब कलम का मजदूर या कलम का सिपाही न होकर, रेख़्ता फाउण्डेशन का मजदूर या रजा फाउण्डेशन का सिपाही या वामपन्थ द्वारा पोषित अभिकर्ता के अतिरिक्त कुछ बचा ही नहीँ! उसके पास गहन चिन्तन और अनुसन्धान के लिए न अवकाश है और न योग्यता।
लेकिन पिछले पच्चीस साल के हिन्दी साहित्य की तमाम असफलताओँ के रहते आदरणीय श्री वागीश शुक्ल उन सम्मानीय अपवादोँ मेँ हैँ जिनके वैदुष्य का लोहा लगभग सभी मानते हैँ। हालाँकि हिन्दी मेँ ऐसे नामुरादोँ की कोई कमी नहीँ जिनमेँ पाण्डित्य समझने की मामूली काबिलियत या किसी के विद्वत्ता स्वीकार करने की साधारण शराफत भी नहीँ है, मैँ उनकी बात नहीँ करता। वागीश शुक्ल की नवीन पुस्तक ‘आहोपुरुषिका’ सेतु प्रकाशन से सद्य: प्रकाशित है। इस पुस्तक को मैँ मृदुला गर्ग जी के शब्दोँ मेँ ‘पत्नी वियोग मेँ झंझावाती विषाद’ की दृष्टि से नहीँ देख पाता। इस पुस्तक को मैँ वागीश जी की पुस्तकेँ – “छन्द छन्द पर कुमकुम” (२००२), “शहंशाह के कपड़े कहाँ हैँ’ (२०१२), ‘चन्द्रकान्ता (सन्तति) का तिलिस्म’ (२०१९) और ‘प्रतिदर्श-कुछ निबन्ध’ (२०२१) के क्रम मेँ उल्लेखनीय और महत्त्वपूर्ण कृति मानता हूँ जो मार्क्सवादी नज़रिए का ‘पुनरुत्थानवाद’ नहीँ है, और न ही शुष्क भारतविद् चिन्तन के वेदोँ के समय समाज क्या रहा होगा, अपितु सभ्यता चिन्तन और गम्भीर समालोचना है। यह वागीश शुक्ल ही हैँ, जो रोमिला थापर की ‘शकुन्तला’ (१९९९) मेँ उनकी नासमझियोँ, मक्कारियोँ (?) या अज्ञानता को उजागर करते हैँ जिसका कोई प्रत्युत्तर कहीँ नज़र नहीँ आता। उदाहरण के लिए ‘यजमान’ जो कहानी सुन रहा है, उसे रोमिला थापर कहानी सुनाने वाला क्योँ कह रही है? यह तो कोई छठी-सातवीँ कक्षा का बालक भी बता देगा कि जनमेजय यजमान है और वह वैशम्पायन ऋषि से महाभारत की कथा सुन रहा है, किसी यज्ञ मेँ सुना नहीँ रहा।
दरअसल वागीश जी का समस्त लेखन गहरी वैचारिकी और गम्भीर दार्शनिक भूलोँ और नासमझियोँ को प्रकट करने का प्रयास है। यह प्रयास व्यक्तिगत लगते हुए भी परम्परा से निबद्ध है और तमाम अल्पज्ञात दार्शनिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक सन्दर्भोँ से आम पाठक को विस्मित करता है। आम पाठक इसे दुरूह क्योँ न माने जब हिन्दी के स्वनामधन्य मूर्खोँ ने यह परिपाटी चला रखी है कि जब भी कोई गहरे चिन्तन से सम्बन्धित हल्की-फुल्की या गलत-सलत बात भी करे, तो उसपर ‘दर्शन आ गया, दर्शन आ गया’ की सियारनुमा चीख-पुकार की जाए। उदाहरण के लिए हिन्दी के कर्णधारोँ को सामान्य समझ भी नहीँ है कि बौद्ध दर्शन मेँ ‘क्षण’ काल का न हो कर सत्ता का प्रत्यय है, इसलिए कोई भी अधकचरा कुछ भी कह दे तो दर्शन के भेड़िए के भय से सियारोँ के समवेत स्वर मेँ ‘हुआँ-हुआँ’ की सलामी देने और दुम हिलाने के अलावा किया भी क्या जा सकता है? और जब ऐसे अज्ञानी साहित्यकार और लेखक होँगे तो हिन्दी पाठकोँ से क्या उम्मीद करेँगे। हिन्दी पट्टी के रद्दी साहित्यिक आस्वाद और बौद्धिक स्तर के पतन की महती जिम्मेदारी सङ्गठित नारेबाजियाँ हैँ जहाँ शालीन चिन्तन-मनन, वाद-प्रतिवाद या संवाद के लिए कोई स्थान शेष नहीँ है। हमारी सामूहिक बौद्धिक विफलता का कारण यह है कि किसी को यह समझ नहीँ कि जयशङ्कर प्रसाद या तुलसीदास केवल शिल्प के कौशल पर कवि नहीँ कहे जाते, बल्कि उन प्रत्ययोँ पर गहरी पैठ रखते हैँ, जो अर्थ की बहुलता रखते हैँ। जब तक उन प्रत्ययोँ की पड़ताल न की जाए, कैसे समझा जा सकता है कि उन प्रत्ययोँ मेँ कुछ गम्भीर बात छिपी है। गम्भीरता से मेरा आशय कुछ वैसा ही है जो इस पुस्तक मेँ वर्णित सूत्र के गुणोँ से लेखक का है। (आहोपुरुषिका के पृष्ठ १९६-१९७ मेँ सूत्र के छ: लक्षण का उल्लेख है – १. अल्पाक्षर २. असन्दिग्ध ३. सारवान् ४. विश्वतोमुख ५. अस्तोभ तथा ६. अनवद्य (निर्दोष)। सूत्र के असाधारण धर्म ‘विश्वतोमुख’ का आशय है उसका चेहरा सब ओर होगा, वह सब ओर बोलेगा।)
संयोगवश ‘प्रतिदर्श’ और ‘आहोपुरुषिका’ मेँ श्री वागीश शुक्ल आग्रह करते हैँ कि हमारी भाषा मेँ ‘पोएट’ के लिए कोई समानार्थी शब्द नहीँ है, इसलिए वे कवि को पोएट कहने का विरोध करते हैँ। ऐसा इसलिए क्योँकि वे कवि को क्रान्तदर्शी मानते हैँ, इसी क्रम मेँ वे ‘विप्र’ के अभिप्राय (=inspired poet) तक भी आते हैँ। यह स्थापना है कि क्रान्तदर्शी होने के कारण वैदिक ऋषि कवि हैँ, पोएट नहीँ। हिन्दी साहित्य ने जो बड़े कवियोँ को ना समझने की, या दरकिनार करने की जो बड़ी गलती की है उसकी नतीजा है कि सामान्य साहित्य अध्येता, लेखक और कवि दोयम दर्जे का निकलता है, झूठे अहंकार से ग्रसित मूर्खता का मात्र प्रारूप। यह स्पष्ट होना चाहिए कि मूर्खता का अभिप्रेत अज्ञानता न हो कर कुछ और है।
मैँ समझता हूँ ‘आहोपुरुषिका’ उस बिन्दु से शुरू होती है जहाँ पर हम अपनी इस नासमझी को स्वीकारेँ कि सभी धर्म एक हैँ या एक ही बातेँ करते हैँ। ये कहना कि सभी नदियाँ अलग-अगल निकलती हैँ और अन्तत: एक ही सागर मेँ मिलती हैँ, अत: सभी पन्थ आदेशित कृत्योँ का गन्तव्य और फल एक है, वह है पारलौकिक सत्ता मेँ विश्वास और ईश्वर की महानता स्वीकार करना तथा उनसे पुरस्कृत होना। यह रेखाङ्कित करना अनिवार्य है कि भारत मेँ ही जैन और बौद्ध मतावलम्बी ईश्वर को नहीँ मानते। ईश्वरकृष्ण का साङ्ख्य, कणाद मुनि का वैशेषिक दर्शन आदि भी ईश्वर को नहीँ मानते। जैनी पारलौकिक सत्ता को मानते हैँ पर उनके लिए ईश्वर सृष्टि का कर्ता नियन्ता न हो कर एक योनि मात्र है, जिसे कोई-कोई महापुरुष पाता है जिन्हेँ ‘कैवल्यज्ञान’ होता है।
पहला मूलभूत प्रश्न उठता है कि हम धर्म या पन्थ के बारे मेँ क्योँ जाने? वह इसलिए क्योँकि आधुनिक प्रजातन्त्र, आधुनिक न्याय व्यवस्था, जिससे सबका पाला पड़ता ही है वह गहरे स्तर पर सामी या अब्राह्मिक चेतना से प्रभावित है, करीब-करीब वैसी ही चलती है कि ईश्वर इस दृश्य जगत मेँ नहीँ है, अपितु अतिक्रामी है। नीत्शे ने यह रेखाङ्कित किया था कि आधुनिक प्रजातन्त्र की बुनियाद ईसाइयोँ की ’दास-मानसिकता’ पर टिकी है, किन्तु अस्वीकारी नहीँ जा सकती। हुस्सर्ल और हेडेगर के चिन्तन मेँ स्पष्ट होता है कि अब्राह्मिक पन्थोँ की अवधारणाएँ किस तरह हमारी सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्था को आकार देती हैँ। कोई भी व्यवस्था या चिन्तन दर्शन से बाहर नहीँ हो सकता और कोई भी दर्शन तत्त्वमीमांसा (या कहेँ परमार्थमीमांसा) से बाहर हो जाए, ऐसा कठिन है। हालाँकि भातिवादी (फेनोमोलॉजिस्ट) ऐसा प्रयास करते हैँ कि वे तत्त्वमीमांसा से दूरी बना कर चलते हैँ। लेकिन यह सत्य स्वीकार करना चाहिए कि दुनिया की अधिकांश तन्त्र/ व्यवस्था के पीछे तत्त्वमीमांसीय विचार चाहे-अनचाहे परिनिष्ठित हैँ।
मूलभूत प्रत्यय जो वैदिक चिन्तन को समस्त अवैदिक चिन्तन से अलग करता है वह यह नहीँ है वैदिक चिन्तन सभी को चैतन्य मानता है; या वह विषय, विषयी और उनसे अतिक्रामी (किन्तु मन्त्रोँ मेँ पर्यवसित) देवता की त्रिपुटी से अपनी बात शुरू करता है; बल्कि यह है कि वैदिक चिन्तन ने काम को पुरुषार्थ माना है। ऐसा अब्राह्मिक पन्थोँ (यहूदी, ईसाई या इस्लाम) ने नहीँ माना है, बल्कि वहाँ काम को पापकर्म का द्योतक समझा गया है। जो काम वासना को विजय नहीँ कर सकते हैँ वही परिवार मेँ रहेँ, इसलिए वहाँ सैदान्तिक रूप से स्त्री काम पिपासा को बुझाने का साधन मात्र है। (देखेँ पृष्ट १५८ – …जैसा कि सेन्ट पॉल ने कहा है,अब्राहमी चिन्तन मेँ विवाह की अनुमति उनके लिए है जो अपनी कामेच्छा पर नियन्त्रण नहीँ रख सकते और यह पुरुष की कामेच्छा-तुष्टि के लिए वैध घेराबन्दी मात्र है।) बौद्ध और जैन भी काम को पुरुषार्थ नहीँ मानते, किन्तु उसे पापकर्म भी नहीँ मानते अपितु कैवल्य या निर्वाण मेँ बाधा मानते हैँ। कबीर की तथाकथित स्त्रीविरोधी दृष्टि भी यही है कि वह साधना मेँ बाधा है।
इसी नाते यदि भारत मेँ कन्यादान के चलन को गाली देने से पहले या विवाह मेँ जीवनसाथी चुनने की स्वतन्त्रता से पहले भारतीय चिन्तन मेँ काम और विवाह के वर्णित स्वरूप को समझना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।
लेकिन उससे पहले हम किताब के इस अंश को देखेँ-
यहाँ थोड़ा ठहर कर हमेँ उन धर्मोँ का एक संक्षिप्त इतिहास देख लेना चाहिए जिन्हेँ ‘अब्राहमी मजहब’ कहा जाता है। दुनिया के अन्य समाजोँ की तरह ही मूलत: सामी लोग भी छोटे गाँवोँ मेँ रहते थे और उनकी राजनीति पंचायती थी किन्तु धीरे-धीरे शहर भी बने और मुखिया से राजा तक की यात्रा पूरी हुई। इसी के समानान्तर ‘एक पूज्य-वाद (= monolatry), जिसे एक व्यापक ग़लतफहमी के तहत प्राय: ‘एकदेव-वाद (=monotheism)’ की संज्ञा दी जाती है, का विकास हुआ। इसका मुख्य लक्ष्य देवताओँ मेँ से एक का उच्चस्थापन और शेष का निरास करना था।
– २.२.१, पढ़-पढ़ के सोचता हूँ किताबोँ की शक्ल मेँ, आहोपुरुषिका
यह सोचने का विषय है कि जिसे बहुदेव-वाद (=Polytheism) कहा जा रहा है, वस्तुत: बहुपूज्य-वाद (= Polylatry) है, जिसे मानने मेँ बहुतोँ को, जैसे कि स्वामी दयानन्द सरस्वती को गहरी आपत्ति है। लेकिन यह तो बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि वेदवाक्य [ एकम् एवद्वितीयं ब्रह्म – इस ब्रह्माण्ड की रचना से पहले, केवल एक परम वास्तविकता थी, दूसरा कोई नहीं था” – छान्दोग्य उपनिषद ६.२.१; सर्वं खल्विदं ब्रह्मम् – “सब ब्रह्म ही है – छान्दोग्य उपनिषद ३.१४.१ ] दरअसल ब्रह्म की अद्वितीयता ही बताती है (इसलिए वहाँ कोई अन्य है ही नहीँ)। वहीँ एकपूज्यवाद वस्तुत: बहुदेव का समर्थन करता है (वहाँ अन्य का अस्तित्व तो है, मगर उसका तिरस्कार आवश्यक है), इसलिए वह तार्किक रूप से बहुदेव-वादी ही है। देखा जाए तो सामी महा-आदेश -Thou shalt have no other gods before Me” (Hebrew: לֹא יִהְיֶה לְךָ אֱלֹהִים אֲחֵרִים עַל פָּנָי, romanized: Lōʾ yihyeh lək̲ā ʾĕlōhîm ʾăḥērîm ʿal pānāi) – तुम्हारे मेरे सामने कोई और देवता न हो- दरअसल मूर्तिभञ्जन का आदेश है (२.२.२ – अहदनामोँ की वैश्विक व्याप्ति, आहोपुरुषिका)। मूर्तिभञ्जन उसी का होगा जिसे आप देवता की मान्यता देकर तिरस्कार कर रहे हैँ। वहीँ सनातनी चिन्तन मेँ ब्रह्म की अनन्त शक्तियोँ मेँ देवता भी शक्ति मात्र है।
इस प्रकरण मेँ पुस्तक के दो अनुच्छेदोँ को मैँ उद्धृत करना चाहता हूँ-
‘समरियाई’ अर्थात् Samaritan शब्द का जो ‘परोपकारी’ अर्थ है उसकी जड़ मेँ हजरत ईसा द्वारा सुनायी गयी एक कथा है जो बाइबिल के ‘न्यू टेस्टामेन्ट’ के अन्तर्गत ‘ल्यूक की किताब’ मेँ दी गयी है। इसके अनुसार एक घायल यहूदी को दो यहूदी तो छोड़ कर चले गये किन्तु एक samaritan ने उसकी मदद की। यह कथा इस प्रश्न के उत्तर मेँ थी कि दस महा-आदेशोँ मेँ से एक अपने पड़ोसी से प्यार करने को कहता है लेकिन ‘पड़ोसी’ का क्या मतलब है। हज़रत ईसा का तात्पर्य यह है कि पड़ोसी वह है जो तुम्हारा हितैषी हो चाहे वह तुम्हारे मजहब को माने चाहे नहीँ।
बाद मेँ St Augustine ने इस कथा का यह तात्पर्य मानने से इनकार कर दिया और यह प्रतिपादित किया है कि इसका आशय यह है कि जो लोग सत्पथ से भटक गये हैँ उन्हेँ हज़रत ईसा सत्पथ पर लाते हैँ। इस प्रकार यह सिद्धान्त बना कि करुणा केवल ईसाइयोँ मेँ पायी जाती है। यह सिद्धान्त परवर्ती ईसाइयत की आधार-शिला है और इस प्रकार तीन मज़हब – इस्लाम, ईसाइयत, और कम्युनिज़्म- ऐसे तैयार हुए जिनमेँ से मानवीय गुणोँ पर किसका एकाधिकार है और वञ्चितोँ-शोषितोँ-पीड़ितोँ-पथभ्रष्टोँ का कौन एकमात्र हितैषी है, इसको ले कर छिड़ी लड़ाई अभी थमी नहीँ है।
– (पृष्ठ १३०, २.२.२ देवलोक की राजनीति : लिखित का वर्चस्व-स्थापन)
‘आहोपुरुषिका’ कुछ ३६३ पृष्ठोँ मेँ फैली पाँच अध्यायोँ मेँ है। पहला अध्याय प्रिया विरह (शोक?) की कविताओँ का है, शेष चार अध्याय सनातन पद्धति मेँ विवाह की वैचारिकी और सम्बन्धित वैदिक मन्त्रोँ के बारे मेँ है। दूसरा अध्याय ‘समागम मेँ प्रेक्षण’, तीसरा अध्याय ‘क्षन्तव्यो मेऽपराध:’, चौथा अध्याय ऋगवेद दशममण्डल, सूक्त ८५ और पाँचवा अध्याय अथर्ववेद, काण्ड १४ मेँ वर्णित विवाह सूक्त के बारे मेँ है। पुस्तक का शीर्षक आदि शङ्काराचार्य की ‘सौन्दर्यलहरी’ के सातवेँ श्लोक से लिया गया है, जहाँ आहोपुरुषिका (अरे, मैँ पुरुष हूँ) देवी पार्वती के विशेषण के रूप मेँ आया है।
किताब मेँ अधिक जाने से पहले यह मूलभूत बात हमारे सामने रखी जा सकती है वह है आधुनिक जीवन मेँ विवाह का निर्णय का अधिकार किसके पास है? क्या वह वर और वधू दोनोँ के परिवार से सम्मत है या केवल अभ्यर्थी के विवेक द्वारा तय होना चाहिए। यहाँ मैँ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि मूल्य का आशय इच्छित और विवेक का द्वन्द्व ही है। जिसकी अभीप्सा की जा रही हो वह विवेक सम्मत भी हो, तभी वह होना चाहिए, संक्षेप मेँ मूल्य ऐसे ही समझा जाता है। आज का आधुनिक सामाजिक अभ्यर्थी यह कहेगा कि मैँ पहले प्रेम करूँगा, फिर तय करूँगा कि इसका फल विवाह होगा या नहीँ। श्री वागीश शुक्ल का कहना है कि यह विचार पद्धति सामी चेतना से सञ्चालित है। (देखेँ पेज १५८, … यही ‘पहले प्रेम, फिर विवाह’ के सिद्धान्त का मूल है- ले दे कर अब्राहमी विवाह परिवार निर्मिति का एकमात्र अदण्डनीय उपाय है जिसको अपनाते हुए मनुष्य ख़ुदावन्द के सामने मुँह दिखाने लायक रह सकता है। इसमेँ स्त्री की यौनिकता का कोई महत्त्व नहीँ है।)
सनातन विचार जिसमेँ आठ तरह के विवाह आते हैँ। वे हैँ – ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापात्य, गन्धर्व, असुर, राक्षस और पिशाच विवाह। वागीश जी का कहना है कि पहले चार विवाह धर्म सम्मत विवाह हैँ, या कहेँ कि धर्म्य हैँ। गन्धर्व विवाह मध्यम स्तर का है, अ-धर्म्य है और अन्तिम के तीन विवाह भी अ-धर्म्य हैँ किन्तु विवाह हैँ (२.४.५ – विवाह और प्रेम, आहोपुरुषिका)। ऐसे विवाह की सन्तान को समाज को मान्यता और विरासत मिलेगी जो कि अन्य विवाहोँ मेँ मिलती है। असुर विवाह में कन्या के माता-पिता वर पक्ष से धन लेने के बाद अपनी कन्या का विवाह करते हैं, जहाँ कन्या की इच्छा कोई महत्त्व नहीँ रखती है। राक्षस विवाह मेँ बलपूर्वक, छलकपट से कन्या का अपहरण करके उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह होता है। पैशाच विवाह मेँ कन्या के अज्ञान मेँ (बेहोशी मेँ, निद्रा मेँ, नशे मेँ) जबरदस्ती सम्बन्ध स्थापित कर के विवाह होता है।
जहाँ तक मेरी जानकारी है कि धर्म्य और अधर्म्य विचार धर्मशास्त्रोँ मेँ (मनुस्मृतिऔर याज्ञवल्क्य स्मृति आदि मेँ) सीधे-सीधे नहीँ है, बल्कि यह बाद मेँ व्याख्याकारोँ (कुल्लूक भट्ट आदि) द्वारा जोड़ी गई है। अत: इसे मैँ चिन्तन-मनन का विषय मानता हूँ। हालाँकि यह स्पष्ट है कि राक्षस और पैशाच विवाह सभी जगह निन्दित हैँ। किन्तु ब्राह्म विवाह सर्वश्रेष्ठ है, यही सनातन मेँ निश्चित विचार है, कहा नहीँ जा सकता। मेरी समझ से ब्राह्म विवाह को श्रेष्ठ कहना ‘धर्मशास्त्र’ या सामाजिक परिस्थितियाँ जैसे उत्तराधिकार, स्त्री का भरण-पोषण आदि से सन्दर्भ न हो कर मूल दर्शन को लेकर है।
लेखक के अनुसार सनातन विचार मेँ अनुराग या प्रेम विवाह का फल है, बीज नहीँ। यहाँ तक कि गन्धर्व विवाह तक मेँ भी नहीँ। वहाँ भी पुराने बीज (अनुराग) को हटा कर नए फल (निरन्तर प्रेम) की कामना की जाती है। यहाँ ‘पहले इस्तेमाल करेँ फिर विश्वास करेँ’ का नियम नहीँ है क्योँकि स्त्री कोई प्रदत्त वस्तु नहीँ है। यह भी नहीँ है कि एक बार प्रेम मिल गया तो हमेशा मिलता रहेगा। विवाह सूक्तोँ मेँ निरन्तर प्रेम मिलते रहने की अभ्यर्थना की गयी है। यहाँ मूलभूत अन्तर यह है कि विवाह दो भिन्न व्यक्तियोँ के सहजीवन का प्रश्न नहीँ है, अपितु भिन्नता को अभिन्नता मेँ परिवर्तित करने का प्रयास है। इस हेतु समस्त प्रकृति, देवताओँ का आशीर्वाद, वर-वधू के परिवार, समाज – सभी आवश्यक घटक है, क्योँकि व्यक्ति उससे परिछिन्न (अलग-थलग) नहीँ समझा जाता। पुस्तक के खण्ड २.४.५.१ और २.४.५.२ मेँ लेखक ब्राह्म विवाह के प्रसङ्ग मेँ कहते हैँ कि इसके अवयव मन्त्र प्रदत्त धर्म्यता, अग्निसाक्षित्व और उभयकुल-सहमति है। ब्राह्म विवाह प्रकृति है और शेष विवाहविधियाँ उसकी विकृति मात्र है।
सनातन पद्धति से विवाह मेँ जो मन्त्र आज भी पढ़े जाते हैँ उनमेँ से एक यह कहता है कि स्त्री का मानवीय पति उसका चौथा पति होता है, इसके पहले उसके तीन दैवी पति हो चुके होते हैँ- सोम, गन्धर्व और अग्नि – जिनसे गुजरती हुई वह मानवीय पति को प्राप्त होती है। इस विचार के पीछे सङ्कल्पना के लिए हमेँ ऋगवेद और अर्थववेद के विवाह सूक्तोँ और उस पर श्री वागीश शुक्ल की टिप्पणियोँ को पढ़ना चाहिए।
विवाह सूक्तोँ के बारे मेँ यह स्पष्ट है कि स्मृतियोँ मेँ वर्णित ‘विवाह’-सञ्ज्ञक आठ विधियोँ मेँ से यह उस विवाह की बात हो रही है जिसे ‘ब्राह्म विवाह’ कहा जाता है। मैँ समझता हूँ इसी के नाते वागीश शुक्ल ब्राह्म विवाह को प्रकृति कह रहे हैँ। इसमेँ ‘कन्यादान’ का प्रमुख स्थान है, अर्थात् पिता अपनी पुत्री को वर के लिए ‘दान मेँ देता है और वर उसे ‘प्रतिग्रह’ के रूप मेँ स्वीकार करता है। यहाँ ध्यातव्य है कि यह वैदिक देवता ‘सविता’ द्वारा अपनी बेटी ‘सूर्या को सोम से विवाहने की कथा है और ‘सविता’ का अक्षरार्थ ‘पिता’ ही है, उसका ‘सूर्य’ अर्थ हम गौणत: करते हैँ।
‘दान’ को जब व्याकरण से समझते हैँ तब उसका एक पूर्वांश है, दाता का स्वत्व हटाना और एक उत्तरांश है, प्रतिग्रहिता का स्वत्व स्थापित करना । लेखक प्रकाश डालते हैँ कि यह ‘स्व-त्व’ क्या है? इसमेँ रक्षण और भोग दो हिस्से हैँ- जब तक गाय आपकी थी तब तक उसे चारा देना और पशुतस्करोँ से बचाना भी आपका काम था और उसका दूध भी आप ही पी सकते थे और उसके गोबर से खाद बनाना आप ही के अधिकार मेँ था किन्तु जब आपने उसे ब्राह्मण को दे दिया तो ये दोनोँ आपके पास नहीँ रह गए, अब चारा भी वही खिलायेगा और दूध भी वही पियेगा। (पृष्ठ १४३)
पुस्तक के दो अनुच्छेदोँ का उद्धरण देकर मैँ अपनी बात को समाप्ति को ओर ले जाना चाहूँगा।
“कीर्कगार्द ने कहा कि प्राचीन ग्रीक ट्रैजेडी मेँ दो तत्त्व होते थे, विषाद (= sorrow) और पीड़ा (=pain) जबकि आधुनिक ट्रैजिडी मेँ से विषाद-तत्त्व लुप्त हैँ। इस विषाद तत्त्व की उपस्थिति का कारण यह था कि प्राचीन ग्रीक सङ्कल्पना मेँ मनुष्य एक ‘व्यष्टि-शेष (= individual)’ है, सारी जिम्मेदारी उसी की है और इस प्रकार आधुनिक ट्रैजिडी केवल पीड़ा को अपना विषय बना सकती है।
मैँ यहाँ कहना चाहता हूँ कि ‘व्यष्टि शेष’ की यह सङ्कल्पना, और फलत: आधुनिकता, एक पूर्णतया अब्राहमी देन है। इस सिलसिले मेँ मैँ बाइबिल के ‘जेनेसिस २-२४’ की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ: “एक पुरुष अपने पिता और माता को छोड़ता है और अपनी पत्नी का आलिङ्गन करता हुआ उससे एकदेह होता है”। इसके विपरीत वैदिक विवाह-सूक्तोँ मेँ आप देखेँगे कि वर और वधू का व्यष्टिगत अस्तित्व उनकी कौटुम्बिकता मेँ उनके या उनके पारिवारिक जनोँ के पुरुष-कार की प्राण-प्रतिष्टा दैव से ही हो सकती है।
– पृष्ठ १३८, २.३.१ – कवि को वीजा नहीँ, आहोपुरुषिका
वागीश शुक्ल जी के लेखन पर बहुधा आरोप यह लगता है कि उन्हेँ पढ़ने के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। मुझे सामान्य पाठकोँ के आलस्य के विषय मेँ क्या कहना होगा? मैँ बस इतना ही कहूँगा कि कुछ हिन्दी के विद्वान कालिदास के ‘रघुवंश’ को चारण काव्य कहते हैँ इसलिए क्योँकि उनकी गति बस उतनी ही है। यह काव्य की जिम्मेदारी नहीँ बनती कि वह पाठक के सामने हवामिठाई की तरह प्रकट हो जाए जिसे गप-गप गटक लिया जाए। ऐसी अपेक्षाओँ ने ही हमारा बंटाधार कर दिया है। यह वही प्रवृत्ति है कि हम पाठ्यपुस्तक नहीँ पढ़ेगे बल्कि सस्ती कुञ्जिकाओँ मेँ दिए हुए कामचलाऊ उत्तरोँ को रट कर परीक्षा मेँ किसी तरह उत्तीर्ण हो कर चौपट डिग्रीधारी बन जाएँगे।
अफसोस है कि इस काहिलियत का कोई इलाज़ नहीँ, जैसे नीत्शे प्रजातन्त्र की तमाम बुराइयोँ के बावुजूद उसका कोई इलाज नहीँ ढूँढ पाते।
(मार्गशीर्ष अमावस्या, संवत् २०८१)
***********************
पुस्तक प्राप्त करने हेतु इस क्रय-लिङ्क पर क्लिक करेँ – https://www.setuprakashan.com/books/aahopurushika-by-wagish-shukla/