वरिष्ठ कवि दिनेश कुमार शुक्ल की कुछ कविताएँ. उनकी कविताओं में लोक-भाषाओं की गूँज सुनाई देती है जो सघन स्मृति-बिम्बों के बीच दूर से उम्मीद की तरह टिमटिमाती दिखाई देती हैं. उनकी समकालीनता में अतीत रचा-बसा दिखाई देने लगता है. आज उनकी कुल तीन कविताएँ आपके लिए- जानकी पुल.
चौथ का चंद्रमा
वह गली उधर से उधर ही
किसी तरफ़ मुड़ती चली जाती थी
और जाने कहाँ जा निकलती …
बहुत प्रयत्न के बाद भी
उन पाँच में से
एक भी कभी जान नहीं पाया
गली का गंतव्य
तब रातें बहुत जल्द ही
शुरू हो जाती थीं,
कण्ठ कुछ देर से फूटता था,
हाफ़पैण्ट पहन कर एक अच्छी उमर तक
लड़के स्कूल जाया करते थे
यानें नवें दसवें ग्यारवें तक भी
उस गली में उड़ती हुई साइकिलें
दिखाई पड़तीं अचानक
जैसे साइबेरिया की चिड़ियों का
कोलाहल अचानक ही
आसमान को भरता चला आये
और फिर दूर क्षितिज में
धीरे-धीरे मंद होता हुआ घुल जाय
चिड़ियाँ आँखों-सी थीं
आँखें चिड़ियों-सी
गौरैयाँ, गलरियाँ, मैनायें, ललमुनियाँ …
साइकिलें लोहे की नहीं
बल्कि टाफ़ी या चीनी की बनी हुई
और आवाज़ें फूलों के गले से
आती हुई सुगंध की तरह
धीरे-धीरे हवा में घुल जाने वाली …
हाँ भाई,
होते हैं कुछ आस्वाद
जो अनुभूति को छूते ही घुल जाते हैं
और शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गंध को
चपत लगा कर
कहाँ-कहाँ कैसे रोमावलियों को
जगाते हुए, अल्पजीवी
नदियों की तरह शरीरों पर
बहते निकल जाते हैं
शरीर की चट्टानों पर
उन धाराओं के निशान छूट गये हैं
चक्रिल, ऋजु, वलय, परवलय,
गड्ढे… अजब-अजब आकृतियाँ
कहीं-कहीं तो अब भी बचा रह गया है
किसी-किसी गोखुर में थोड़ा-सा पानी
जिसमें चौथ के चंद्रमा का प्रतिविम्ब
घात लगा कर बैठा रहता है
वह गली अब भी है
सिर्फ़ इतना पता चला है कि
वह एक नदी है
और यह भी कि उसका एक छोर
आकाशगंगा से जुड़ा है
चीलें आकाश में मंडला रही हैं
अपने अण्डे चीलें आकाश में सेती हैं
चीलें ग्रीष्माकाश की प्रचंडता को
कम कर रही हैं
गली में
सायकिलें अब नहीं आतीं
सायकिलें अब नहीं आतीं
वहाँ दोनों तरफ़ सिर्फ़ दूकानें ही दूकानें हैं
इसीलिए आते हैं भृंग-पतंग
कि उनके गुंजार से लिपट कर
फूलों का पराग-पुंकेसर
वृक्षों वनस्पतियों को फलीभूत करता
उड़ता चला जाय वसन्त के गर्भ में
ताकि निदाघ की प्रचंडता को
महुआ कर सके मद से स्निग्ध
और आम उसे नहला दे अमृत से
इसीलिए आती है रात
बिना कुछ कहे
कि दिन भर की थकान,अपमान, वंचना को
धो कर बहा ले जायें
धारायें स्वेद की,
उड़ा ले जायें निश्वास उन्हें दूर
गहरी नींद की दुनिया में …
कभी-कभी इसलिए आता है एक क्षण
कि सधा हुआ तीर
उथले पानी की मछली को
बींध कर
खुद भी काँपे पीड़ा में
कि पानी में लहरों का भूकम्प भर जाय …
अभी-अभी केंचुल छोड़कर
आया हुआ धामिन
पानी के कम्पन को छूता है जीभ से
क्षण भर धूप में
स्टील की तरह चमकता है धामिन
क्षण भर …
लेकिन लगता है वक्त
सरसों की तीखी, पसीने में डूबी,
मत्स्यगंधा-आहट के घटाटोप में,
भावाकुल होने में
वक्त लगता है
गंध की वर्णमाला सीखने में
कि पूरा संसार ही बयान किया जा सके
इस नये माध्यम से
और पहचाना जा सके
भयानक दुख में भी छिपी
मनुष्यता की गंध को
जो अफ्रीका से, मंगोलिया से,
चिली के रेगिस्तानों से,
ताहिती के टापू से आती है
बिल्कुल एक जैसी –
तीखी सरसों और लहसुन के स्वेद में डूबी
फ़ास्फोरस और सेवार के आयोडीन में सीझी
क्लोरीन और कैल्शियम के प्रवाह-सी …
अब तुमसे कैसे कहूँ
कि लगभग दौड़ कर पकड़ा मैने
पृथ्वी को इस बार प्रदक्षिणा में
वरना मैं भी चाँद की तरह
पीछे छूट जाता
और घूमता रह जाता अपने आवर्त में
वक्त लगता है
पृथ्वी की गति से
अपनी गति मिलाने में,
वक्त लगता है
दूसरे को समझने में,
वक्त लगता है
कदम से कदम मिला कर
जीवन भर साथ-साथ
चलना सीखने में …
तुमने तो वो किया मोबाइल
तुमने तो वो किया मोबाइल
जो अनंग भी सोच न पाया
किस्साख़ानी की गलियों की
कलियों की ख़ुशबू से तुमने
क्वांगतुंग के युवा मिक्खु की
प्रज्ञा की परिमिति के भीतर
सौरभोत्कलित प्रश्नाकुल उदग्रता भर दी …
सात-सात पर्दों के भीतर
बंदी पाटल की आभा को
गजनी से, गांधार-स्वात से मुक्त करा कर
जन-विमुक्ति के कवि के मन में
रत्नद्वीप की अरुणाभा में
सप्तसिंधु के पार जगाया
तुमने तो वो किया मोबाइल
जो अनंग भी सोच न पाया
पैंसठ की वृद्धा के मन में
जिज्ञासा की भूख जगाई,
ब्लॉग सिखाया चैट सिखाया
नई कूट भाषा सिखलाई
सिखलाया संदेश भेजना
एक नया संसार दिखाया
कट्टरता के कोट तोड़ कर
बिना एक भी गोला दागे
तुमने दुर्गम दुष्तर पथ को
सहज प्रेम का पंथ बनाया
तुमने तो वो किया मोबाइल
जो अनंग भी सोच न पाया








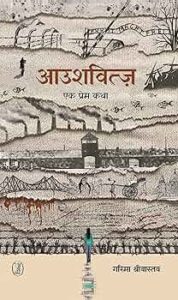


"भयानक दुख में भी छिपी मनुष्यता की गंध" को पहचानने वाले दिनेश शुक्ल की कविताएँ जब यह कहते हैं कि "…गली में सायकिलें अब नहीं आतीं, तहाँ दोनों तरफ सिर्फ दूकानें ही दूकाने हैं", तो ऐसा लगता है कि कवि ने बाजारवाद की विभीषिका से जूझते अपने उस समाज की कलई खोल दी है जहाँ संवेदना की बात दूर, नॉस्टैल्जिक होने तक की गुंजाइश बची नहीं रह गयी है! लेकिन साथ ही कवि पाठकों को संबल देता है और स्वयं कहता है कि "…कहीं-कहीं तो अब भी बचा रह गया है किसी-किसी गोखुर में थोड़ा पानी…।" इतनी सुन्दर कविताओं को प्रकाशित करने के लिए प्रभात रंजन साधुवाद के पात्र तो हैं ही, प्रदक्षिणा में दौड़कर पृथ्वी को पकड़ लेने वाले दिनेश कुमार शुक्ल भी कोटि-कोटि बधाई के हकदार हैं…।
—-अनुज, कथाकार, नई दिल्ली
पहली कविता विशेष अच्छी लगी। नोस्टेल्जिया ..बहुत देर तक बना रहा इस कविता को पढ़कर।
दिनेश जी मेरे प्रिय कवि हैं। ये तीनों ताजी कविताएँ उनकी रचनात्मकता का विस्तार है।
pahalee kavitaa bha gayee