रविकांत मूलतः इतिहासकार हैं लेकिन साहित्य की गहरी समझ रखते हैं. मंटो की जन्मशताब्दी के अवसर पर उनका एक यादगार लेख आपके लिए- जानकी पुल.
=========================================
मंटो ने रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए कला की कोई भी दिशा चुनी हो, हंगामा किसी न किसी तरह अवश्य हुआ। – –बलराज मेनरा व शरद दत्त
कोई सत्तावन साल पहले महज़ बयालीस की उम्र में तक़सीम–ए–हिन्द और शराबनोशी के मिले–जुले असर से अकालकालकवलित मंटो आज सौ का होने पर भी उतना ही हरदिलअज़ीज़ है, जितना हैरतअंगेज़, उतना ही लुत्फ़अंदोज़ है, जितना तीरेनीमेकश। शायद आज भी उतना ही मानीख़ेज़। बल्कि यूँ मालूम होता है कि वक़्त के साथ उसके अनपढ़ आलोचकों की तादाद कम होती गई है और पिछले दो–तीन दशकों में मुख़्तलिफ़ विधाओं में पसरे उसके लघु–कथाओं व बड़े अफ़सानों, मज़ामीन, रेडियो नाटकों, मंज़रनामों, ख़तों, फ़िल्मी संस्मरणों और अनुवादों के बारीकतरीन पाठों का सिलसिला थमने की जगह ज़ोर पकड़ने लगा है। और पाठ–पुनर्पाठ की ये धारा सिर्फ़ उर्दू या हिन्दी में ही नहीं, बल्कि अंग्रेज़ी में भी मुसलसल बह निकली है। जिसके बूते दक्षिण एशिया का यह अप्रतिम कहानीकार अब समस्त दुनिया की एक नायाब धरोहर बन गया है। यह वाजिब भी है क्योंकि मंटो के अदब व फ़लसफ़े में पश्चिम व पूर्व का अद्भुत संगम हुआ। मोपासाँ, चेखव व गोर्की वग़ैरह से उसने अगर तुला हुआ, मुख़्तसर अंदाज़े–बयान सीखा तो एशियाई माहिरों से रस बरसाने वाली दास्तानगोई का चमत्कार, और तफ़्सीलात का इज़हार। अपनी शैली में आधुनिक होकर भी वह सांस्कृतिक तौर पर लोकस्थित और राजनीतिक तौर पर लोकोन्मुख लेखक था, वैसे ही जैसे लाहौर, पाकिस्तान जाकर भी अनबँटा बंबइया हिन्दुस्तानी रहा। देशभक्ति, तरक़्क़ी, आज़ादी, हिन्दुस्तान–पाकिस्तान, स्वराज, नवनिर्माण जैसे नारों और तहरीक़ों को उसने नारों और तहरीक़ों की ही तरह लिया, आप्त वाक्य या आख़िरी मंज़िल के रूप में नहीं। पंडित नेहरू और चचा सैम को उसने एक–साथ आड़े हाथों लिया। विचारधाराओं और अस्मिताओं की इतनी बड़ी और बेशुमार आँधियों में उसके अब तक साबुत टिके रहने की यही वजह है कि क़लम चलाते हुए उसकी आत्मा सन्नद्ध रहते हुए भी तटस्थ रही, उसकी नैतिकता चालू नैतिकता नहीं बन पाई, ज़हर–बुझे उसके औज़ार बेशक मारक थे, और उसके वर्णन निहायत ईमानदार और परतदार। उससे भी अहम बात, उसके चरित्र पाखंडी और विषम समाज के लतियाए, दुरदुराए और उठल्लू किए हुए लोग हैं, जिन्हें आज हाशिए के किरदार कहा जाता है। ख़ास तौर पर, तक़सीमे–हिन्द के नए जनवादी या सबॉल्टर्न इतिहास का आलातरीन हमदर्द मसीहा तो मंटो है ही।
मंटो से मेरी पहली मुलाक़ात युवावस्था की दहलीज़ पर हुई, उस कमबख़्त उम्र में, जब आप किसी मांसल और लज़ीज़ किताब पर आँख फेरने की जुगत में होते हैं। होशियार प्रकाशकों को भी हमारे–जैसे ग्राहकों के अस्तित्व का इल्म रहा होगा, वरना ‘मंटो की बदनाम कहानियों‘ का रेलवे स्टेशनों पर मिलना क्या इतना आसान होता। बहरहाल उनका शुक्रिया कि मंटो से त‘आरुफ़ करवाया, भले ही मंटो ने अपने पाकिस्तानी जीवन–काल में ही हिन्दुस्तान में अपनी रचनाओं की चोरी की शिकायत प्रधानमंत्री नेहरू से लगा दी थी, जो ज़ाहिर है बेअसर रही। अगर आप भी मेरी दशा में मंटो के पास गए होंगे तो शायद सहमत होंगे कि प्यास तो ख़ैर मंटो जगाता है, बुझाता नहीं। लिहाज़ा बतौर पाठक मुझे जिस्मानी ज़रूरियात के लिए साहित्य की दीगर तरह की ‘पंक पयोधि‘ में डूबना पड़ा, जिससे बतौर लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी अपनी जवानी में बड़ी सफ़ाई से बच निकले थे। लेकिन मंटो को पढ़के दो ख़ास फ़ायदे ज़रूर हुए: 1. जिन्सी मसायल पर बुज़ुर्गाना वर्जनात्मक संस्कारों का जो अपराधबोधनुमा साया था, वह कट गया, ज़ाहिर हुआ कि यह बिल्कुल नैसर्गिक चीज़ है, इससे कोताही की कोई ठोस वजह नहीं। 2. समझ में आया कि शरीर से मुताल्लिक़ कहानियाँ सिर्फ़ शरीर की नहीं होतीं: वह प्रकारान्तर से समाज, परिवार, धर्म, जाति, नस्ल, राष्ट्र, स्त्री–पुरुष संबंधों, और सत्ता आदि की कहानियाँ होती हैं। चाहे वह शरीर टेटवाल के कुत्ते का ही क्यों न हो, ये अहसास तो कई साल बाद जाकर हुआ जब विभाजन के दरमियान लोगों पर क्या गुज़री, यह जानने के लिए हिन्दी–उर्दू के बाक़ी कहानीकारों–उपन्यासकारों के साथ मंटो को दुबारा पढ़ने–गुनने लगा। शुक्रिया एक बार फिर उपेन्द्र नाथ अश्क(संस्मरण), देवेन्द्र इस्सर (मंटो की राजनीतिक कहानियाँ), नरेन्द्र मोहन(कहानियाँ, संस्मरणों, व मुक़द्दमों की किताबें) व बलराज मेनरा तथा शरद दत्त (दस्तावेज़, 5 खंड) जैसे संपादकों का कि वे नागरी में मंटो को पुस्तकाकार लेकर आते रहे, क्योंकि उर्दू पढ़ना तो बाद में सीख पाया, और कुछ हद तक मंटो से मोहब्बत के असर में भी। अंग्रेज़ी में उपलब्ध मंटो–साहित्य तब तक मुख़्तसर, बुरी तरह अनूदित और नाकाफ़ी ही था, बल्कि आज भी है। फिर जब हमारी दोस्त फ़रीदा मेहता ने काली शलवार बनाने की ठानी तो मंटो का एक बार फिर पारायण किया गया, और सामूहिक कोशिश से उस पुरानी कहानी में नई अर्थ–छायाएँ हासिल की गईं। आजकल जब भी सिनेमा या रेडियो पर कुछ सोचने या लिखने बैठता हूँ, तो बरबस याद आ जाता है कि जहाँ मैं बैठा हूँ, यानि सिविल लाइन्स में, वहीं ऑल इंडिया रेडियो का दफ़्तर होता था, जहाँ से पाँचवें दशक में मंटो और कृष्ण चंदर के लिखे नाटक प्रसारित होते थे, वे यहाँ आसपास रहते भी थे। और मंटो ने फ़िल्मिस्तान से जुड़कर सिनेमा के लिए भी ख़ूब लिखा – अफ़सोस कि उसकी लिखीं ज़्यादातर फ़िल्में फ़िलहाल गुमशुदा हैं, लेकिन कटारी पढ़कर ये अहसास होता है कि क्या कसा हुआ मंज़रनामा है। और सिनेमाई संस्मरणों की किताब मीनाबाज़ारतो मंटो की पैनी नज़र और साफ़गोई के लिए मशहूर है ही।
ग़रज़ ये कि मंटो ने जिस विधा को चुना, उसमें शिल्प या कथानक के लिहाज से कुछ न कुछ नया जोड़ा, कुछ नए लेखकीय प्रतिमान गढ़े, नई ज़मीनें तोड़ीं। किंवदंती है कि फ़रमाइशी कहानियाँ तो वह अमूमन एक ही बैठक में, कभी–कभार तो कहवाघर में बाज़ी लगाकर कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए, लिख मारता था। एक ज़माने में पापी पेट के लिए लगभग रोज़ाना लिखता था। मेनरा व दत्त के अनुसार, दिल्ली में मंटो की रिहाइश और ऑल इंडिया रेडियो में मुलाज़िमत तक़रीबन उन्नीस महीने की है। इस छोटी अवधि में उसने कोई सौ रेडियो नाटक व फ़ीचर लिखे, जो एक रिकॉर्ड होगा। बक़ौल मंटो ये ऐसे नाटक थे, जिन्हें पढ़कर लोगों को भले ही हँसी आती हो, उसे तो कतई नहीं आती थी। इंपले को बहुत हँसी तो नहीं आती लेकिन मुस्कुराए बिना भी नहीं रह पाता। अपनी बात समझाने के लिए ‘आओ…’ शृंखला के रेडियो नाटक लिए जा सकते हैं। अव्वल तो, नाम बड़े दिलचस्प हैं: ‘आओ कहानी लिखें‘, ‘आओ ताश खेलें‘, ‘आओ चोरी करें‘, ‘आओ झूठ बोलें‘, ‘आओ अख़बार पढ़ें‘, ‘आओ बहस करें‘, वग़ैरह–वग़ैरह। इस शृंखला में अपवादों को छोड़ दें तो मूल किरदार तीन ही हैं – पति किशोर, जो किसी दफ़्तर में काम करता है, उसकी पत्नी लाजवंती जो घर संभालती हैं, और उनका दोस्त नारायण, जो मूलत: किशोर का ही दोस्त है, जो ठुकुरसुहाती तो भाभी की करता है, लेकिन अंतिम विश्लेषण में पक्ष किशोर का ही लेता है। दोनों मिलकर कभी–कभी लाजवंती को उल्लू बनाकर अपना काम निकाल लेते हैं, लेकिन दीगर मौक़ों पर बातचीत में माहिर लाजवंती उनसे एक–दूसरे का भाँडा फुड़वाकर अपनी ज़हानत का लोहा मनवा लेती है।
अब ‘आओ रेडियो सुनें‘ की थोड़ी तफ़सील में जाएँ, इसलिए कि ये दौर हिन्दुस्तान में रेडियो के लिए बुनियाद डालने का दौर था, जब बीबीसी से आए लायनेल फ़ील्डेन की अगुआई में पितरस बुख़ारी और उनके छोटे भाई ज़ुल्फ़िक़ार बुख़ारी ऑल इंडिया रेडियो का संजाल बिछाने में जी–जान से लगे हुए थे। एक ओर उदारवादी फ़ील्डेन कोशिश कर रहा था कि रेडियो का इस्तेमाल कॉन्ग्रेसी नेता भी अपनी जनता से मुखामुखम होने में करें, दूसरी ओर गांधी व नेहरू जैसे नेता और महाकवि निराला–जैसे हिन्दी कार्यकर्ता इस माध्यम को साम्राज्यवादी भोंपू, इसलिए कलंक और छूत की निशानी मानते हुए इससे एक सुरक्षित दूरी बनाए रखने के पक्ष में थे। लेकिन साथ ही प्रसारण की अंतर्वस्तु व उसकी ज़बान को लेकर रेडियो के अंदर और बाहर हिन्दी व उर्दू वालों के बीच बाक़ायदा एक अखाड़ा खुला हुआ था। हिन्दी वाले इसे ‘बीबीसी‘ यानि ‘बुख़ारी ब्रदर्स कॉरपोरेशन‘ के ख़िताब से नवाज़ते नहीं थकते थे, और रविशंकर शुक्ल जैसे नेता इसकी ज़बान यानि हिन्दुस्तानी को अपदस्थ कर शुद्ध हिन्दी की ताजपोशी के हामी थे। इस प्रसंग में रेडियो के लिए मंटो, कृष्ण चंदर, इम्तियाज़ अली ताज जैसे लेखकों का ख़ूब लिखना रेडियो के लिए निहायत फ़ायदेमंद साबित हुआ। अपने रेडियो–नाटकों में, और कटारी–जैसे दूसरे नाटकों में भी, मंटो रेडियो–जैसे अपेक्षाकृत नए माध्यम के प्रचार–प्रसार में कार्यकर्तानुमा मुस्तैदी दिखाता है, क्योंकि उसके लिखे कई अप्रत्याशित प्रसंगों में रेडियो की बात घूम–फिरकर आ ही जाती है। एक और ग़ौरतलब बात यह है कि मंटो के रेडियो–नाटकों की ज़बान उसके अफ़सानों से अलहदा, अर्थात आमफ़हम, सरल–सहज–सुबोध है, जो कि उसके फ़िल्मी मंज़रनामों के लिए भी बिला शक कही जा सकती है। हर माध्यम के लिए माक़ूल भाषा के प्रयोग का नुस्ख़ा मंटो ने पारसी नाटकों के सुपरस्टार लेखक आग़ा हश्र कश्मीरी–जैसे अग्रजों की मिसाल से सीखा होगा, जिनके लिए उसके मन में अगाध श्रद्धा–मिश्रित–श्लाघा है। इसके अलावा, जैसा कि उसने ऑल इंडिया रेडियो में अपनी नौकरी की दरख़्वास्त को मज़बूती देने के उद्देश्य से लिखा था: कि उसके पास रंडियों और उनके ग्राहकों, भड़वों और उनके तौर–तरीक़ों, देह–व्यापार और उसके वातावरण के बारे में पूरा ज्ञान मौजूद है। याद रखने की ज़रूरत है – और इस बात की ताईद उस समय कार्यरत रेडियोकर्मियों की कई आत्मकथाओं से होती है – कि उस दौर में पारसी नाटक, सिनेमा और रेडियो में काम करने को भले घरानों के लड़के–लड़कियों (लड़कियों पर ज़्यादा ही सख़्ती थी) के लिए उचित नहीं माना जाता था। तो मंटो की उस ‘दरख़्वास्त‘ को ऐसे माहौल बनाने वाले दकियानूसी समाज पर छोड़ा गया व्यंग्य–बाण भी माना जा सकता है, जिससे पहले फ़ील्डेन और बाद में बुख़ारी–बंधु अपने–अपने तरीक़ों से जूझते रहे थे, और जिन्हें मंटो का यह तुर्श हास्य सहज भाया होगा, तभी तो उसे रेडियो की मुंशीगिरी मिली। दावे चाहे जो हों, देखने लायक़ बात यह है कि ‘आओ…’




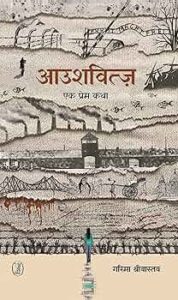






मंटो पर शानदार आलेख। लेखक को बधाई और 'जानकी पुल' का आभार…
मंटो की लेखनी के दीवाने रविकांत के मंटो को जानना वाकई दिलचस्प है. बहुत-बहुत ख़ूब भाई रविकांत जी, नया पाठ और भाई प्रभात रंजन के जानकी पुल को भी. शुक्रिया. – शशिकांत.