वह एक ऐसी सतह पर था जिसके ऊपर उठना ही नहीं चाहता था
मित्र लेखक शशिभूषण द्विवेदी के निधन के बाद मैंने उसको याद करते हुए यह लेख ‘हंस’ में लिखा था। आज उसकी जयंती है तो इसे आप भी पढ़ सकते हैं-
=======================
शशिभूषण द्विवेदी के निधन के बाद फेसबुक पर जब लोग बड़ी तादाद में उसको श्रद्धांजलि दे रहे थे मुझे गोविंद निहलानी की फ़िल्म ‘पार्टी’ याद आ रही थी। फ़िल्म में एक वरिष्ठ नाटककार के सम्मान में पार्टी दी जाती है। उस पार्टी में अनेक युवा-वरिष्ठ लेखक मौजूद हैं। लेकिन अमृत मौजूद नहीं है। धीरे धीरे उस पार्टी में अमृत के बारे में बात होने लगती है जो साहित्य राजनीति की दुनिया को छोड़कर आदिवासियों के बीच काम करने के लिए चला गया है। उस पार्टी में सब साहित्य की सत्ता से जोड़-तोड़, विदेश यात्राओं के जुगाड़ की बातें कर रहे हैं। लेकिन अमृत सबसे दूर है। वह उन सभी की अंतरात्मा को कचोट रहा है। जब वे सोते हैं तो उनके सपने में अमृत का संघर्षरत चेहरा आ जाता है। मैं यह नहीं कह रहा कि वह अमृत की तरह संघर्ष कर रहा था। लेकिन हम सब भौतिक सफलताओं के लिए तीन तिकड़म में लगे रहे, उसको जैसे कुछ चाहिए ही नहीं था। वह इन सबसे दूर बैठा चुटीले वाक्य लिखता रहता था। कभी कुछ चुभता हुआ मैसेज कर देता था।
शशिभूषण द्विवेदी का नाम, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने पहली बार 2002 में सुना था। उन दिनों मैं महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका ‘बहुवचन’ का संपादन कर रहा था। डाक से रचनाएँ आती रहती थीं। पत्रिका में नए लेखकों की रचनाएँ कम ही प्रकाशित हो पाती थीं लेकिन मैं पढ़ता सबकी रचना था। ऐसे ही एक दिन डाक में एक लिफ़ाफ़ा आया। जिसमें संपादक के नाम पत्र के साथ एक कहानी थी। वह कहानी थी ‘काला गुलाब’। शशिभूषण द्विवेदी नामक एक लेखक की डाक से आई हस्तलिखित कहानी को पढ़कर मैं यही सोचता रहा कि यह कैसी कहानी है जो बहुत कुछ कहना चाहती है लेकिन कहती कुछ नहीं है। अव्यक्त की एक गहरी टीस थी उस कहानी में जिसमें उस समय की कहानी का एक प्रचलित फ़ॉर्म्युला बेरोज़गारी का तो था लेकिन प्रेम की पीड़ा, विरसे में मिली बेघरी और एक घर का सपना। मैं बने बनाए साँचे में उसको डिकोड नहीं कर पाया था। जब आप बने बनाए फ़ॉर्मूले से अलग हटकर कुछ पढ़ते हैं तो आप एकबारगी कुछ कह नहीं पाते। कहानी प्रकाशित तो नहीं हो पाई। बाद में मैं भी उस नौकरी से भी निकल गया।
ख़ैर, अच्छी तरह से याद है मुझे उस कहानी को पढ़कर मैंने अखिलेश जी को फ़ोन किया था। उन दिनों उन्होंने ‘तद्भव’ नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था और उनकी कहानियों की तरह पत्रिका की भी धूम मची हुई थी। जब उनसे मैंने शशिभूषण द्विवेदी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके पास भी डाक से उसकी एक कहानी आई थी ‘एक बूढ़े की मौत’ जो उनको अच्छी लगी और वे प्रकाशित करने जा रहे थे। लेकिन उनकी मुश्किल यह थी कि पत्र में उसने उन दिनों उसकी कहानियाँ सबको प्रभावित कर रही थीं। ज़िक्र चला है तो बताता चलूँ कि उसकी कहानियों पर सुधीश पचौरी और राजकिशोर ने अपने अपने स्तम्भ में लिखा था। दोनों अपने जमाने के स्टार स्तंभकार थे।
हिंदी कहानियाँ उस काल में उदय प्रकाश और बाद में अख़िलेश के मुहावरे के सम्मोहन में थी। अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरे पहले कहानी संग्रह ‘जानकी पुल’ की कई कहानियों में यह सम्मोहन दिखाई देता है। लेकिन शशिभूषण की आरम्भिक कहानियों में कहीं से भी वह सम्मोहन नहीं दिखाई देता है। उसके जीते जी उसकी कहानियों का ठीक से विश्लेषण नहीं किया गया लेकिन आज लिखते हुए मैं इस बात को ईमानदारी से रेखांकित करना चाहता हूँ कि इक्कीसवीं शताब्दी में परिदृश्य पर आए युवा लेखकों में वह उन गिने चुने आरम्भिक लेखकों में था जो अपना मुहावरा विकसित करना चाहता था। मैं और मेरी पीढ़ी के कुछ अन्य लेखक सफलता के सुरक्षित मुहावरे में लिखकर अपने आपको स्वीकृत करवा रहे थे। जबकि वह बहुत विनम्रता से विद्रोह कर रहा था। प्रसंगवश, हम दोनों ने अपने अपने पहले कथा संग्रहों का समर्पण अखिलेश को किया था। बाद में मैं तो उनसे दूर होता गया, विद्रोह करता गया लेकिन वह उनसे आजीवन जुड़ा रहा। यह नहीं कह सकता कि अखिलेश जी भी उससे जुड़े रहे या नहीं लेकिन वह अपनी तरफ़ से उनसे जुड़ा रहा। वह उनको फ़ोन करता था, जो बात होती थी मुझे सुनाता और इस तरह उसने मुझे भी कभी अखिलेश से पूरी तरह अलग नहीं होने दिया। उस दौर का शशिभूषण अपने जीवन और अपने लेखन में बहुत अलग था। 2007-08 के बाद का शशिभूषण बहुत बदल गया था। उसका जीवन फैल गया था। लेकिन उससे पहले बहुत अलग था वह। उसके जीवन में कम लोग थे, वह नियमित लिखता था, नौकरी करता था। और हाँ, गुटका तब भी खाता था।
मुझे याद है उससे पहली मुलाक़ात ब्रजेश्वर मदान ने करवाई थी। उन दिनों ब्रजेश्वर मदान सहारा में पत्रकारिता की अपनी आख़िरी पारी खेल रहे थे। शशिभूषण और ब्रजेश्वर मदान के बीच की मैत्री, रिश्तों को लेकर, दोनों की शराबनोशी आदि को लेकर बहुत कहा-सुना गया है, कई लेखकों ने लिखा भी है, लेकिन उन दोनों के रचनात्मक संबंधों को लेकर किसी ने नहीं लिखा। कुछ बातें लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ब्रजेश्वर मदान से मेरे संबंध बहुत पुराने थे, तब जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र था। मेरे एक सीनियर मित्र नरेश शर्मा उनकी कहानियों से बहुत प्रभावित थे और वे उनकी कुछ कहानियों के ऊपर फ़िल्म बनाना चाहते थे। उनके प्रभाव में ही मैं उनसे पहली बार दरियागंज में मिला था। वे ‘फ़िल्मी कलियाँ’ के संपादक थे। शाम में दफ़्तर खत्म होने के बाद वे ‘पउआ पार्टी’ करते और फिर जहाँगीरपुरी स्थित अपने घर के लिए निकल जाते। उनकी पउआ पार्टी में मैं भी अक्सर मौजूद रहने लगा। कई बार भागीदार के रूप में भी लेकिन अक्सर दर्शक के रूप में ही। तब मैं लेखक बना नहीं था लेकिन उनकी संगत में कई लेखकों से उन्हीं महफ़िलों में परिचय हुआ जिनके नाम लिखना यहाँ उचित नहीं होगा।
ख़ैर, बाद में, अपने जीवन भर की कमाई से मदान साहब ने नोएडा में एक बड़ी कोठी बनवा ली थी। यह उन्हीं दिनों की बात थी जब वे सहारा समूह के लिए काम कर रहे थे। उन्हीं दिनों दुबारा उनसे जुड़ना इसलिए हुआ क्योंकि मैं नोएडा बॉर्डर पर रहने लगा था और मेरे घर से सहारा के दफ़्तर की दूरी बहुत कम थी और सहारा के दफ़्तर से मदान साहब के घर की दूरी बहुत कम थी। पुराने दिनों की तरह उनकी महफ़िलें जमने लगी थीं। उन महफ़िलों में शशिभूषण की उपस्थिति स्थायी भाव की तरह होती थी, हरेप्रकाश उपाध्याय भी संचारी भाव की तरह आ जाते थे। मैं अक्सर जाता पहले सहारा के दफ़्तर, वहाँ से सेक्टर 12 के मार्केट के ठेके में। उनकी पार्टी का स्टाइल वही पउआ पार्टी वाला ही रहा। यानी एक पउआ ख़रीदा और बिना पानी के गटागट। मैंने यह ध्यान दिया कि शशिभूषण ने भी मदान साहब की शैली अपना ली थी। मैं ब्रीजर से काम चलाता था। इस तरह गटागट पीना मेरे बस की बात नहीं थी।
इस साहचर्य पर इतना विस्तार से मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि उसके जीवन के इस काल ने उसको रचनात्मक रूप से समृद्ध भी किया। वह अपने जीवन में सबसे सकारात्मक इसी काल में दिखा था। एक प्रसंग की तरफ़ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। सहारा समय कथा चयन का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रथम पुरस्कार मेरी कहानी ‘जानकी पुल’ को दिया गया था। शशिभूषण की कहानी ‘शिल्पहीन’ को तृतीय पुरस्कार मिला था। इस बात को लेकर बहुत विवाद हुआ कि मुझे प्रथम पुरस्कार इसलिए मिला क्योंकि फ़ाइनल ज्यूरी में मनोहर श्याम जोशी और सुधीश पचौरी थे और दोनों मेरे गुरु थे। लेकिन इस बात पर किसी का ध्यान नहीं गया कि सहारा समूह की तरफ़ से उस पुरस्कार के संयोजक ब्रजेश्वर मदान थे।
जो काम टेबल पर ही हो गया था हिंदी वाले उसका इल्ज़ाम कुर्सी को देते रहे। मुझे याद है एक बार पुरस्कार की इस घटना के बहुत बाद मैंने उससे कहा था कि शिल्पहीन आपकी कमजोर कहानी है क्योंकि यह एक ऐसी कहानी है जिसमें आपने आपने मुहावरे को छोड़कर हिंदी के प्रचलित मुहावरों में एक साम्प्रदायिकता के मुहावरे को अपनाया था। उसने जवाब दिया था- ‘आपने तकनीक के जाल को कहानी में उलझाकर एक नया मुहावरा बनाने की कोशिश की थी। लेकिन मुझे मदान साहब ने बताया था कि मीटिंग में मनोहर श्याम जोशी ने आपकी कहानी के बारे में बोला था कि आपकी यह कहानी एक मेक्सिकन कहानी से प्रभावित है।‘
किस लेखक की किस कहानी से- यह वह बता नहीं पाया। उसी दौर में वह उपन्यासों की योजना पर बात करता था। वह क़स्बों के छोटे मोटे बदमाशों पर उपन्यास लिखना चाहता था, वह एक ऐसे नेता के जीवन की कहानी लिखना चाहता था जो समलैंगिक था। लेकिन लिखा कुछ नहीं। वह कहानी इस तरह सुनाता मानो पूरी लिख चुका हो, माँगने पर बमुश्किल एक पन्ना भेजता था और पूछता कैसी लगी?
यह बात अलग है कि शशिभूषण को ईनाम इकराम मिलते गए लेकिन वह उस दौर में भी एक ऐसी कुर्सी का इंतज़ाम नहीं कर पाया जिसके ऊपर बैठकर वक कुछ चैन से जी सके। उसी दौर में ब्रजेश्वर मदान ने उसको अपनी छाँह दी थी और वह सुकून महसूस कर रहा था। कुणाल सिंह दिल्ली आ गया था और हरेप्रकाश, शशिभूषण, कुणाल की दोस्ती का एक अलग स्तर था, जिनके ऊपर बहुत लिखने का मैं अधिकारी नहीं हूँ। लेकिन मदान साहब वह अंतिम आदमी थे जो सबके बावजूद उसको लेकर बहुत संवेदनशील थे। वह मुझसे कहते थे कि इसको शादी के बाद अपने घर में रहने का ठिकाना दे दूँगा। रात में उसकी शिकायत करते थे, दिन में उसको लेकर परेशान हो जाते थे।
सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक ब्रजेश्वर मदान को लकवा मार गया। इलाज के लिए उनको उनके भाई के घर ले ज़ाया गया। मदान साहब के परिदृश्य से जाने के बाद मैं बोहेमियन से घरेलू हो गया और शशि आज़ाद। उन्हीं दिनों उसको लेकर क़िस्से कहानियों की शुरुआत हुई। उसके जीवन में कुछ अच्छे दोस्त और जुड़ते गए, कुमार अनुपम, रामजनम पाठक, सुधांशु फ़िरदौस, अविनाश मिश्र। वह अक्सर इनकी गति-प्रगतियों से मुझे अवगत करवाता रहता था। लेकिन इनमें से कोई उसकी दिशा मोड़ नहीं पाया। सब अपनी-अपनी दिशा में मुड़ गए। वह अपने अंधेरे में बढ़ता जा रहा था।
उसने आख़िरी नौकरी हिंदुस्तान टाइम्स समूह की पत्रिका ‘कादम्बिनी’ में की, जो उसको विष्णु नागर के संपादक रहते मिली थी और उसके पीछे कारक की भूमिका हरेप्रकाश ने निभाई। मैं ज़ाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में पढ़ाने लगा था, जो कस्तूरबा गांधी स्थित हिंदुस्तान टाइम्स के दफ़्तर के पास था। मैं अक्सर हिंदुस्तान के दफ़्तर जाता था, लेकिन उससे मिलने नहीं राजेंद्र धोड़पकर से मिलने। उसके क़िस्से-कहानियों को सुन-सुन कर या अपनी मशरूफ़ियत के बढ़ते जाने के कारण उनसे मिलना कम होता जा रहा था। लेकिन मैं अक्सर हिंदुस्तान के दफ़्तर से बिना उनसे मिले निकल आता। उस अख़बार के बड़े बड़े पत्रकार मेरे दोस्त थे, उनके संपादक से मेरी सीधी बात होती थी। सार्वजनिक रूप से उनसे मिलने में मैं भी थोड़ा कटने लगा था। सब कटने लगे थे।
लेकिन इस बात का वह बुरा नहीं मानता था। सोशल मीडिया की सक्रियता के दिनों में ज़रूर वह अक्सर मेरे बारे में ऐसी टिप्पणियाँ कर देता था जो बुरी लगने वाली होती थीं लेकिन न मैंने उनका बुरा माना न उसने दोस्ती का सिरा तोड़ा। वह फ़ोन पर जुड़ा रहा। अपनी शादी की बात भी उसने मुझे फ़ोन पर ही बताई। लम्बी लम्बी बातें करता। पत्नी की तारीफ़ें करता। उसकी एक कहानी याद आ रही है ‘छुट्टी का दिन’। यह अकेली कहानी है जो मध्यवर्गीय जीवन को लेकर है। पारिवारिकता को लेकर है। ऐसा लगने लगा था कि वह रमने लगा था, लेकिन किसी चीज़ में पूरी तरह रम जाना उसका स्वभाव ही नहीं रहा। वह मिलता था, बातें करते-करते अचानक बिना विदा माँगे चला जाता था। फ़ोन पर वह कई बार ऐसी ऐसी बातें करता था जिनके सूत्रों को जोड़कर मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जब वह कादम्बिनी में गया ही था तो एक दिन कहने लगा, जानते हैं अब हिंदी के लेखक वही होंगे जिनको कोरपोरेट में मोटी मोटी तनख़्वाह मिलेगी। साहित्य उनके लिए अपनी ऐश्वर्य की दुनिया से निकलने या उसको फैलाने का माध्यम बनेगा। अब कलम के मज़दूरों का दौर नहीं रहा। आने वाला समय कलम के व्यापारियों का होगा। जब मैं उसको लिखने के लिए कहता तो फ़ोन काट देता था। वह ख़ुद भी कई बार महीनों फ़ोन पर ग़ायब हो जाता था, न फ़ोन करता न फ़ोन उठाता। फिर अचानक ऐसे प्रकट हो जाता जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह आगे पीछे के सिरे ग़ायब करता जा रहा था। उसकी बातों से कई बार मुझे अहसास होता था। लेकिन मैं समझ गया था कि उसको अपने अंधेरों से प्यार हो गया था। उजाले में आते ही जैसे उसकी आँखें चौधियाने लगती और वह फिर ग़ायब हो जाता।
एक बात मैंने महसूस की थी कि शशि हमेशा ऐसे लेखकों के नाम लेता था जिनको हिंदी समाज में उपेक्षा बहुत मिली। सबसे पहले उससे मेरी लड़ाई भीमसेन त्यागी को लेकर हुई थी। उन दिनों वह जनसत्ता में मुझसे मिलने आता और बिना किसी प्रसंग के कहने लगता, जानते हैं भीमसेन त्यागी बहुत बड़े लेखक हैं। एक दिन इसी बात से चिढ़कर मैंने ग़ुस्से में उसको डाँटकर भगा दिया। यह मैंने महसूस किया कि जब भी उससे लड़ता या उसको झाड़ पिलाता तो वह कभी प्रतिकार नहीं करता था। चुपचाप चला जाता, या फ़ोन रख देता। बाद में मैंने महसूस किया कि ब्रजेश्वर मदान, राजकमल चौधरी ऐसे सारे लेखक उसके लिए आदर्श थे जिनको सामाजिक स्वीकृति नहीं मिली। हम बड़े बड़े लेखों से जुड़ने के जुगाड़ में रहते थे वह उनके जिनको ‘छोटा लेखक’ कहा जाता था।
हम सब बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं के पीछे भागते रहे वह हमेशा छोटी छोटी इच्छाओं के पीछे। वह प्रूफ़ के काम के अलावा कोई और काम न माँगता था, न करता था। वह लिखने के कमिटमेंट पूरे नहीं करता था, अनुवाद के प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ देता था लेकिन प्रूफ़ के काम हमेशा पूरा करता था। अपने आख़िरी दिनों में उसके घर में दो किताबें थीं जो रॉयल कोलिंस प्रकाशन ने उसको दी थीं। वह उनके प्रूफ़ पढ़ चुका था और उनको भिजवाने के लिए बेचैन था। कभी कहता पैदल चला जाऊँ देने क्या, कभी कहत कुरियर से भिजवा दूँ क्या? आख़िर फ़ोन उसने मुझे 5 मई को किया था और पूछा था कि उस प्रूफ़ को किस तरह भेजा जा सकता था। मैंने कहा कि उन लोगों का दफ़्तर करोलबाग में है, लॉकडाउन में कुछ नहीं किया जा सकता। उसके निधन की खबर जब मैंने रॉयल कोलिंस प्रकाशन के निदेशक महोदय को दी तो वे बोले कि तीन-चार दिन पहले उससे उनकी लम्बी बात हुई थी। उन्होंने उसको आश्वस्त किया था कि ‘लॉकडाउन के बाद पहुँचा दे प्रूफ़, कोई जल्दी नहीं है। अजीब आदमी था, उसको मैंने संपादन, अनुवाद हर तरह के काम के लिए कहा लेकिन एक साल से वह केवल प्रूफ़ का काम ही कर रहा था। और किसी काम के लिए राज़ी नहीं होता था।‘
वह एक ऐसी सतह पर था जिसके ऊपर उठना ही नहीं चाहता था। वह एक बेहतरीन कहानी के आइडिया की तरह था जिसको पूरा नहीं करना चाहता था। जाने के बाद अमृत की तरह हमारी अंतरात्मा को झकझोरता रहेगा।


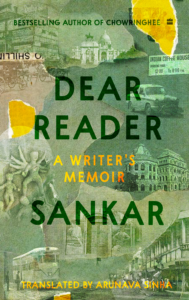


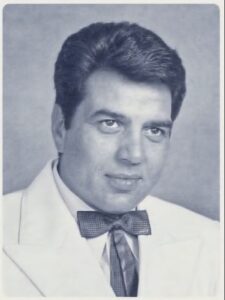


संस्मरण पढ़ा,,, अब समझ नहीं आ रहा क्या कहें.. बस इतना कह सकते हैं कि शशिभूषण जी की कहानियों की को पढ़ने की इच्छा जागृत हो गयी है…