अम्बुज पाण्डेय अपनी आलोचना और टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। गगन गिल की कविताओं पर उनका आलेख पाठकों के लिए विशेष
***************
‘गगन गिल’ की काव्य यात्रा में पिछले चार दशकों से अधिक का समय स्पंदित हो रहा है। इस दीर्घावधि में हिन्दी साहित्य में अभिव्यक्ति, अनुभूति और काव्य संवेदना के धरातल पर बहुत कुछ परिवर्तित हुआ है। स्त्री लेखन अपनी स्वानुभूति, विषयों की विविधता और आत्मबल से पहले की तुलना में अधिक समर्थ सिद्ध हुआ है। संकोच और वर्जनाओं की तमाम सीमाओं को अतिक्रमित करता स्त्री लेखन गुण और परिमाण दोनों दृष्टियों से परिशंसन पा रहा है। जो विषय काव्य वस्तु के लिए उपेक्षित और त्याज्य समझे जाते थे, आज उन विषयों पर अलग-अलग कथ्य और शिल्प स्वतंत्र अभिव्यक्तियाँ पा रहे हैं। कहना न होगा, गगन गिल ने अपने स्तर पर इस विस्तृत व वेगवती धारा को अलग पहचान दी है।
गगन गिल किसी वांछित सुख या प्रत्याशा की चाह से प्रेरित हो कर कविता नहीं लिखतीं, और न ही कविता से उन्हें बहुत काम लेना है। उनके लिए काव्य सृजन अहैतुक, किंतु अपरिहार्य कर्म जैसा है। हाँ, रचना के क्षणों में भीतर का जमा हुआ शीशा तिल-तिल कर जरूर निकलता है। लेकिन इस दुख से तब भी मुक्ति नहीं। इससे यदि कुछ सार्थक और रचनात्मक बन पड़ता है तो भली बात है। बहुत बार यह रचनात्मकता और सृजन दुख और वेदना को अधिक गहनतर करता जाता है। इसका कोई अंत नहीं। बिलकुल महादेवी वर्मा की तरह “तुमको पीड़ा में ढूँढा, तुम में ढूँढूँगी पीड़ा।” महादेवी रहस्योन्मुख हो उठती हैं। उनका रहस्यवाद पारंपरिक विधान से अनुमोदित है और स्वयं लेखिका द्वारा स्वीकृत भी। लेकिन गगन गिल के यहाँ एक अलग तरह की एंबीग्विटी है। चाहे वह स्थूल काव्य परिपाटी से संबंधित हो अथवा स्त्री प्रश्नों से। एक स्त्री लेखिका के तौर पर वो मानती हैं कि लिखते वक्त जिस पीड़ा की अनुभूति उन्हें होती है, ऐसे में वो लेखिका न होतीं, कुछ और होतीं तो ज्यादा श्रेयस्कर होता।
यह आत्मवक्तव्य उस पारंपरिक अवधारणा का प्रत्याख्यान सा जान पड़ता है जहाँ लेखक किसी मुक्ति की अभीप्सा में लेखन करता है। और बार-बार वह इसे उद्धृत भी करता है। यह स्वीकारोक्ति अतिरंजित नहीं है। बहुत से लेखकों और कलाकारों ने सृजन से मुक्ति की बात की है। उन्हें इससे अपरिमित तोष मिलता है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन गगन गिल का सृजनलोक भिन्न समवायों से ही निर्मित हुआ है। वहां मुक्ति और मार्ग जैसे एक-दूसरे से गुथे हों। हाँ, सबका पर्यवसान करूणा में ही होता है।
‘पिता ने कहा’ कविता में वे लिखती हैं…
“पिता ने कहा
मैंने तुझे अभी तक
विदा नहीं किया
तू मेरे भीतर है
शोक की जगह पर
शोक मत कर
पिता ने कहा
अब शोक ही तेरा पिता है।”
उक्त छोटी सी कविता में संश्लिष्ट अर्थ संघनित होकर फूटते हैं। मितकथन का ऐसा चमत्कार कि हाइकू सदृश कविता में अर्थछटाएँ चित्त पर सदा के लिए अंकित हो जाती हैं।
गगन गिल की कविताओं में केन्द्रीय तत्व करूणा है।
कविताओं में पिरोये हुये छोटे-छोटे शब्द करूणा की एक शांत नीरव झील रचते जाते हैं। यहाँ न कोई नारा है, न किसी वाद का घोषित नैरेटिव। यहाँ नैसर्गिक कविता का स्पेक्ट्रम है जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी स्त्री जाति अपना दुख भोगती और अपनी बेटियों में वही दुख रोपती चली जाती है। सहजात भाव और संवेगों का रिसता एक ऐसा सोता, जो बहुत देर तक मस्तिष्क को नम बनाए रहता है। कभी न समाप्त होने वाला यह दुख ‘अँधेरे में बुद्ध’ कविता में मुखरित हुआ है…
“रोती हुई
उठती है वह
एक दिन
नींद से
हो गयी है पार
इस बार
गर्दन से
इसी तरह
मरा करती थी
माँ
उसकी नींद में
बचपन में
माँ की माँ
माँ के बचपन में।”
नींद के भीतर नींद, माँ के भीतर माँ, स्त्री के भीतर स्त्री और मरण के भीतर मरण। पीढ़ियों की कैसी त्रासद लड़ी है। न तो यह गल्प है, और न ही फैंटेसी। यह स्त्री जाति का लोमहर्षक हलफनामा है जो कल्प-कल्पांतर से उसकी नियति के साथ मढ़ दिया गया है। कवयित्री दुःख की अंतहीन गाथा चीत्कार से नहीं, मस्तिष्क को सुन्न कर देने वाली ऐसी ही विलक्षण काव्य-शैली से व्यक्त करती है।
गगन गिल की काव्य संवेदना पर बुद्ध की करूणा का प्रत्यक्ष प्रभाव है। बौद्ध दर्शन से वे प्रेरित हैं। वह उन्हें निर्देशित भी करता है और बहुत बार उनके रचना कर्म का प्रस्थान भी वही है। लेकिन जहाँ बौद्ध दर्शन समस्त सांसारिक दुखों से उपराम होने की बात करता है, भेद रहित दृष्टि का संदेश देता है, वही गगन गिल की स्त्री भवसागर से पार होने का कोई उद्यम नहीं करती। पता नहीं भवसागर के उस पार क्या होगा। वहां भी पितृसत्ता और भेद से मुक्ति मिलेगी या नहीं। उसका जीवन तो स्वयं में भेद का शाश्वत प्रतिदर्श ठहरा। उसे मुक्ति के लिए अवकाश कहाँ। परंपराओं में उसकी मुक्ति का मार्ग भी अवरूद्ध है। ऐसे में वह अगले जन्म में भी मनुष्य ही रहने की कामना करती है। उसकी कामना कितनी सहज और निर्व्याज है….
“चिड़ियाँ बेघर थीं हमारे शहर में
हम डरे हुए लोग थे
हम चूहों से डरते आए थे
और छिपकलियों से, इन दिनों
मच्छर हमारे आतंक का कारण थे
और उनके पेट में पलते अदृश्य जीवाणु
हम इतना डरे हुए थे
कि अगले जन्म में भी मनुष्य रहना चाहते थे
इसके लिए
हम कोई भी पाप कर सकते थे।”
गगन गिल की कविता में बार-बार ‘माँ’ और ‘माँएँ’ की आवृत्ति होती है। ‘माँ’ जो ‘स्त्री’ होती बेटी में कायांतरण करती रहती है। माँ के साथ ही उसकी करुणा, सहिष्णुता, उदासियाँ और दुखों का अंबार भी बेटी में यथावत अंतरित होता जाता है। ध्यातव्य है, ‘माँएँ’ यहाँ एक वचन से बहुसंख्यक मात्रा का बोधक भर नहीं है। यह सातत्य की एक अंतहीन शृंखला है जो न जाने कब से सब का ‘योग क्षेम’ वहन करती आ रही है। वह अपनी सारी इच्छाओं को दूसरों पर न्यौछावर कर देती है। सच तो ये है कि उसकी अपनी कोई इच्छा ही नहीं। दूसरों की इच्छाओं में ही उसकी समस्त इच्छाओं का अंतर्भाव हो जाता है। इन इच्छाओं से परे उसकी एक ही नियति है…हर बेटी माँ से और हर माँ बेटी से छूटती किसी रहस्यलोक में गुम होती जाती है….
“अक्सर उन्हें हिम्मत देती
कहती हैं माँएँ,
बीत जाएँगे, जैसे भी होंगे
स्याह काले दिन,
हम हैं न तुम्हारे साथ!
कहती हैं माँएँ
और बुदबुदाती हैं ख़ुद से
कैसे बीतेंगे ये दिन, हे ईश्वर!
बुदबुदाती हैं माँएँ
और डरती हैं
सुन न लें कहीं लड़कियाँ
उदास न हो जाएँ कहीं लड़कियाँ।”
संसार के पसारे में फैले इतने विषयों को छोड़ कर कवयित्री अपनी करूणा का सारा अभिनिवेश स्त्री चिंता पर करती है। यह उसकी जातीय चिंता है, साथ ही आत्मिक भी। इससे ज्यादा गंभीर और आवश्यक उसके लिए कुछ भी नहीं। यहाँ आधी आबादी की उपेक्षित दुनिया है, उसका संघर्ष और अपूरित मनोरथ है। उसे लेकर गढी गयी अनेक किंवदंतियाँ हैं, उनपर चढाया गया मुलम्मा है। अतः स्त्री के अवचेतन को टटोलती, उसकी उदासियों का थाह लेने कवयित्री आखिरी तह तक पहुँचना चाहती है। इस काव्य-उद्यम में ‘गगन गिल’ की स्त्री केन्द्रित कविताएँ बहुधा हमें रहस्य और यथार्थ के संधिबिंदु पर ले जाकर छोड़ देती हैं। उनके यहाँ कथ्य इतना धूमिल और गतिमान है कि सहसा किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता। धीरे-धीरे शब्दों का तिरोधान होता है और कवयित्री का अभिप्रेत स्नायु में आकार लेने लगता है। कविता में सब कुछ सपाट ढ़ंग से व्यंजित कर देने का उतावलापन कवयित्री में नहीं है। वो पाठकों को काव्य मर्म का संकेत भर कर देती हैं, अर्थ संधान करना स्वयं पाठक के श्रम, अनुभूति और आस्वाद पर निर्भर करता है। यह वैशिष्ट्य उन्हें अन्य लेखकों से अलग करता है…
“जिस एक काँटे से
बचने के लिए
तैरती रही मछली
समुंदर-दर-समुंदर
उसकी देह में छिपा था।”
‘उसकी देह में छिपा काँटा उससे अब तक अलक्षित रह गया।’ इस भोले और सपाट कथन में व्यंग्य की तीव्रतम अनुगूँज है जो भीतर तक चीस मारती है। उसकी देह स्वयं उसके लिए भले देह हो, लेकिन दूसरों के लिए उसके मायने अलग हो जाते हैं। यह देह ही उसके दुखों का बड़ा कारण है। उसकी पीड़ा और छटपटाहट तक दृष्टि पहुँचने से पहले देह आड़े आ जाती है।
कभी-कभी वो ऐसे प्रतीकों का चयन करती हैं जहाँ अर्थ झिलमिलाते रहते हैं। न तो उनका भाव पूरी तरह गोपन रह पाता है, और न ही चमकदार ढ़ंग से व्यंजित होता है। कवयित्री की यह शैली कलात्मक औदात्य का स्पर्श करने लगती है। ‘तुम सुई में से निकलती हो’ कविता में वो लिखती हैं…
“तुम सूई में से निकलती हो
मैं धागे में से, माँ
कभी सूई में से मैं
धागे में से तुम
कौन सी बखिया ,माँ
हम सिले जा रहीं
सदियों से
कौन सा टांका
पूरा होने में नहीं आता
कब उतरेंगे सितारे
मैली अपनी चादर पर
खिलेगा कोई फूल
अपनी इस फुलकारी पर।”
सूई और धागे का यह रूपक बहुत अर्थपूर्ण है। उक्त रूपक का गुंजलक तैयार होता है माँ-बेटी के युग्म से जो परस्पर एक दूसरे से आबद्ध हैं। सूई-धागा निर्जीव यंत्र है। उसके श्रम और व्यापार का फलागम उसे कभी नहीं होता। काव्य संवेदना के स्तर पर सूई-धागे की यह यांत्रिकता धीरे से माँ और बेटी में संक्रमित हो जाती है।
गगन गिल को पढ़ते समय कई बार विमल राय की याद ताजा हो उठती है। विमल राय ने अपने सिनेमा में जिन स्त्री चरित्रों को साकार किया है, गगन गिल की सिरजी स्त्री छवियाँ उनसे से जा मिलती हैं। दोनों जगह स्त्री अपने त्रासद रूप में उपस्थित है। दोनों जगह जीवन की निरूपायता और दारुण दशा अवसन्न कर देने वाली है। ये स्त्रियाँ क्रियाशील हैं, इनमें जीवन-संघर्ष का माद्दा है। कहीं ये पछाड़ खाकर गिरती नहीं, सारी बाधाओं को पार करती जाती हैं। लेकिन एकाएक इनके आगे की राह गुम हो जाती है। और ये स्वयं को यथास्थितिवाद से निकालने में पूरी तरह विफल रहती हैं। यद्यपि यह दो विधाओं के मेल का सरलीकरण है, लेकिन दोनों रचनाकारों के अंतस्थल में जैसी करूणा और सहिष्णुता है, वो सब एक साथ मनस पटल पर कौंध उठती हैं।
‘चीटियाँ’ कविता में गगन गिल लिखती हैं…
ढूँढ़ती वे चलती जातीं पृथ्वी के एक सिरे से
दूसरे की ओर।
वे अपने दाँत गड़ातीं
हर जीवित व मृत वस्तु में।
उनके चलने से पृथ्वी के दुख हल्के होने लगते
कि दिशाएँ घूमने लगतीं, भ्रमित हो।
ध्रुव बदलने लगते अपनी जगह।
चींटियों का दुख लेकिन कोई न जानता था।
बहुत पहले शायद कभी वे स्त्रियाँ रही हों।
‘चीटी’ की आवश्यकताएँ सीमित हैं, लेकिन उसका श्रम अपरिमेय है। चींटी की क्षुधा अल्प में ही तृप्त हो जाती है, लेकिन उसका उद्यम उसकी काया से वृहत्तर है। उसके सामर्थ्य की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। उसकी घ्राणशक्ति अचूक है, लेकिन खाद्य-अखाद्य, जीवित-मृत सबका वह परीक्षण करती धरती को नापती रहती है। शायद वह शापित है। उसकी दृढ़ता और धीरज देखकर ध्रुव भी अपना स्थान बदल देते हैं। शायद वह मुक्ति की आकांक्षा में एक सिरे से दूसरे सिरे तक अनथक चक्कर लगाती रहती है। लघुकाय चींटी के इतने गुणों का साम्य केवल स्त्री से हो सकता है। और इस तरह अंतिम पंक्ति में कविता का केन्द्रीय अर्थ चमक उठता है…
“बहुत पहले शायद कभी वे स्त्रियाँ रही हों!”
स्त्री सरोकारों को लेकर गगन गिल का मानदंड अन्य रचनाकारों से थोड़ा भिन्न और उदार है। उनकी रचनाओं में स्थूल लैंगिक विभाजन या पितृसत्ता के प्रति प्रचलित ध्वंसात्मक पैटर्न नहीं दिखाई देता। यद्यपि स्त्री के पददलन और पराधीनता के मूल में पितृसत्ता ही है, लेकिन इस संबंध में वो बहुत संवेनशील और संतुलित दृष्टि लेकर चलती हैं। उनकी धारणा है कि स्त्री के भीतर भी स्त्री दृष्टि हो यह जरूरी नहीं, और मात्र पुरुष होना स्त्री का प्रतिलोम या स्त्री विरोधी होने का कोई मानक नहीं है। समाज में बहुतेरे ऐसे लोग हैं जो स्त्री की स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं है। वे यथास्थितिवाद के प्रबल समर्थक और पोषक हैं। साथ ही सारी पीड़ा और यातना झेलती अधिकांश स्त्रियाँ भी ऐसे समर्थकों की सहकार ही बनती हैं। उनके भीतर उस बौद्धिक त्वरा का नितांत अभाव है जो स्त्री की स्वतंत्रता को तार्किक और न्यायोचित ठहरा सके। फलतः करुणा और सहनशीलता से इतर दूसरी स्त्री जो गगन गिल के मनोलोक में आकार लेती है, वह बड़ी विलक्षण है। वह जिस तेवर और तार्किक शक्ति से संवलित है उसे लोक-परलोक का कोई प्रलोभन डिगा नहीं सकता। वह बड़ी भास्वर है। उसकी देह और आत्मा पराधीन नहीं है। उसका चयन कवयित्री पोंगापंथी समाज की छाया और संस्कारों से दूर ‘वनकन्या’ के नव अवतार में करती है। ‘वनकन्या’ सभ्यता और संस्कृति के दबाव से निर्लिप्त है। सो कवयित्री उसका आह्वान करती है …….
“देवता हो, चाहे मनुष्य
देह मत रखना किसी के चरणों में
देह बड़ी ही बन्धनकारी, वनकन्या!
सुलगने देना
अपनी बत्ती
अपना दावानल
× ×
अपनी मज्जा
अपनी अग्नि
परीक्षा अपनी
डरना मत किसी से, वनकन्या
× ×
अपनी देह
अपना यज्ञ
अपनी ज्वाला
नग्न और देह विहीन
लौटना मत इस बार
किसी कन्दरा
किसी कुटिया में
देवता हो
चाहे मनुष्य।”
जब ऐसी अंतर्दृष्टि लेकर गगन गिल अपनी कविताओं की निर्मिति करती हैं, तो एक सबल और ओजपूर्ण स्त्री का अवतरण होता है। वह जितनी चेतनासम्पन्न है, उतना ही अपने तेज और साहस से चकित भी करती है। ‘वनकन्या’ में जैसा प्रतिघाती वेग और प्रभंजन है, वैसा अन्य कविताओं में देखने को नहीं मिलता। उसकी क्षीप्रता देख जैसे कवयित्री स्वयं ठिठक जाती है और संवेदनात्मक प्रबोध देने लगती है…
“ज़रा धीरे चलो, वनकन्या
बीज सो रहा है
मिट्टी में
घास चल रही है
धरती में
बर्तन लुढ़क रहे हैं
भीतर तुम्हारे आले से
जहाँ भी रखती हो पाँव
दरक रही है धरती
ज़रा धीरे चलो, वनकन्या
पछाड़ दिया है तुमने
ऋतु-चक्रों को
पुरखों को
गिद्धों को।”
संबोधन और प्रबोध से शुरू होती कविता मध्य तक पहुँचते-पहुँचते एक दूसरा ही रूपाकार ले लेती है। ‘पुरखों’ और ‘गिद्धों’ की शाब्दिक व्यंजना समूचे इतिहास और अमानवीयता को न केवल उद्घाटित करती है, बल्कि सारी परंपरा को प्रश्नांकित करते हुये उसे कटघरे में खड़ा कर देती है। ऐसी कविताएँ समाज में जड़ीभूत पितृसत्तात्मक संस्कारों का उच्छेदन कर देती हैं। लेकिन उनकी कविताओं का यह स्थाई स्वभाव नहीं है। फलतः परिमाण में गगन गिल के यहाँ ऐसी कविताएँ कम हैं।
कविता और स्त्री को गगन गिल एक धुँधली सी धुन मानती हैं। इस कथन के आलोक में उनकी कविताओं पर अंतिम निर्णय नहीं हो सकता। एक आकृति जो कभी पकड़ में आती है, कभी नहीं आती। जितना पकड़ में आती है वह आधा सच है, पूरी तरह वह कभी पकड़ में आयी ही नहीं। उसका जीवन भी तो पूरी तरह खुद उसका अपना नहीं है। वह कभी स्वतंत्र नहीं है। यदि उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर भी दिया जाय तो अपने चारो तरफ वह आत्मानुशासन का घेरा बना लेती है। वह बार-बार स्वयं को निर्वासित करती रहती है। निर्वासन और वापसी दुख के दो छोर हैं। इन दो छोरों के बीच चक्कर लगाती स्त्री की आकृतियाँ गगन गिल की कविताओं में आकार लेती रहती हैं।
*****************
अम्बुज पाण्डेय ने स्नातक और स्नातकोत्तर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से पूर्ण किया है। वहीं से पत्रकारिता में पीएच-डी पूरी की। शोध कार्य के दौरान सांस्थानिक पत्र-पत्रिकाओं पर उल्लेखनीय काम। आलोचना, मधुमती, हिमांजलि और लमही समेत अन्य पत्रिकाओं में समय-समय पर आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। इन दिनों हिन्दी विभाग, के.बी.पी.जी. कालेज मीरजापुर में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत।
डॉ. अम्बुज कुमार पाण्डेय
असि.प्रो. हिन्दी विभाग,
के.बी.पी.जी. कॉलेज मीरजापुर
उ.प्र. 231001
mailtoambuj@gmail.com
mob. 9451149575

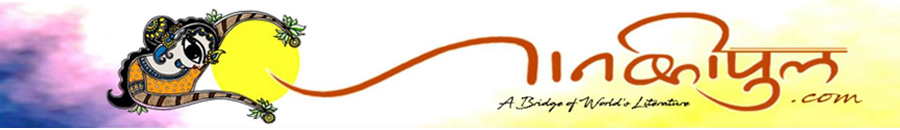

1 Comment
मैंने गिल को इसके पहले कभी पढ़ा नहीं, पर इस टिप्पणी पढ़ने के बाद इनको पढ़ने की ईच्छा बलवती हो गई | चुकी जिनकी टिप्पणी मैने यहां पढ़ी वो मेरे अग्रज भी हैं और साहित्यिक अग्रज भी हैं, जिनके शाब्दिक और व्यावहारिक बाजुओं के छत्रछाया में हमलोगों ने साहित्य को पढ़ा और समझा,सो जितनी समझ का पौरुष हमलोगों ने धारण किया वो इनका हमलोगों पर स्नेह और आशीर्वाद का परिणाम है, इनकी टिप्पणियां और आलोचनाएं हमेशा ही गूढ़ार्थ एवम निष्पक्ष होती हैं, मुझे जब भी इसका अवसर मिलता है तो मैं इसको पढ़ता नहीं बल्कि सहर्ष ही ज्ञानार्थ और रसास्वादन हेतु इसका अध्ययन करता हूं | आशा है इसी तरह का अवसर हमलोगों को आपके इस website के माध्यम से मिलता रहेगा |
हमारी तरफ से इस प्रयास के लिए शुभेक्षा