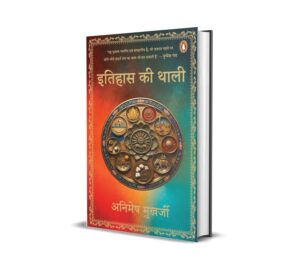आज पढ़िए वेब सीरिज़ कोहरा सीजन 2 पर प्रसिद्ध संस्कृतिकर्मी वाणी त्रिपाठी की यह टिप्पणी- मॉडरेटर
============================
पंजाब की सर्द सुबहों में उतरती धुंध केवल मौसम की घटना नहीं, वह एक सामाजिक मनःस्थिति का रूपक है। धुंध में दृश्य अस्पष्ट होते हैं, दिशाएँ गड्डमड्ड हो जाती हैं, और सत्य अपनी स्पष्टता खो देता है। कोहरा का दूसरा सीज़न इसी धुंध को कथा में बदल देता है। यह अपराध की जाँच भर नहीं करता; यह हमारे समय की नैतिक उलझनों, संस्थागत दबावों, प्रवासी आकांक्षाओं और पारिवारिक विघटन की गहरी पड़ताल करता है।
भारतीय वेब–श्रृंखलाओं के परिदृश्य में अपराध अब केवल मनोरंजन नहीं रहा; वह सामाजिक और राजनीतिक पाठ बन चुका है। कोहरा 2 इसी परंपरा को आगे बढ़ाता है। यहाँ “किसने किया” से अधिक महत्वपूर्ण है “क्यों हुआ”- और यही प्रश्न इसे एक सामान्य थ्रिलर से अलग कर एक वैचारिक दस्तावेज़ में बदल देता है।
अपराध के बहाने समाज की परतें
दूसरे सीज़न की कथा एक नए केस से आरंभ होती है। पर शीघ्र ही स्पष्ट हो जाता है कि हत्या की जाँच यहाँ कथानक का केंद्र होते हुए भी अंतिम लक्ष्य नहीं है। अपराध यहाँ परिणाम है—उन सामाजिक संरचनाओं का, जो वर्षों से भीतर ही भीतर सड़ रही हैं।
पंजाब की धरती, जो कभी हरित क्रांति और समृद्धि का प्रतीक थी, अब बेरोज़गारी, पहचान-संकट और प्रवासन की तीव्र आकांक्षा से जूझ रही है। विदेश जाना केवल आर्थिक अवसर नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन चुका है। पर जब यह सपना छलावा सिद्ध होता है, तो उसका टूटना केवल व्यक्ति को नहीं, पूरे परिवार को घायल करता है।
सीरीज़ इस विडंबना को सूक्ष्मता से पकड़ती है कि आधुनिकता केवल आर्थिक प्रगति से नहीं आती; वह भावनात्मक परिपक्वता और सामाजिक संवेदना से आती है। यदि समाज संवेदना खो देता है, तो प्रगति भी हिंसक हो जाती है।
पटकथा: रहस्य से अधिक समाज का पाठ
इस सीज़न की पटकथा तेज़-रफ्तार थ्रिलर की तरह नहीं दौड़ती। वह ठहरती है, देखती है, और दर्शक को भी ठहरने के लिए बाध्य करती है। संवादों में शोर नहीं है; वहाँ एक संयत बेचैनी है। कई बार पात्रों का मौन उनके शब्दों से अधिक मुखर हो उठता है।
लेखन की सबसे बड़ी शक्ति उसकी परतदार संरचना है। उपकथाएँ केवल सजावट नहीं, बल्कि मुख्य कथा की वैचारिक गहराई को विस्तृत करती हैं। हाँ, यही वैचारिक भार कभी-कभी उसे बोझिल भी बनाता है। कुछ क्षणों में कथानक की तात्कालिकता धीमी पड़ती है, और दर्शक से धैर्य की अपेक्षा की जाती है। पर यह धीमापन भी एक कलात्मक चयन है—यह सीरीज़ उत्तेजना नहीं, आत्ममंथन चाहती है।
निर्देशन: दस्तावेज़ी यथार्थ का सौंदर्य
निर्देशक–निर्माता सुदीप शर्मा ने पहले सीज़न की यथार्थवादी परंपरा को यहाँ और परिपक्वता से आगे बढ़ाया है। उनकी दृष्टि में अपराध दृश्यात्मक सनसनी नहीं, बल्कि सामाजिक विश्लेषण का उपकरण है।
उनका पूर्व कार्य, विशेषकर NH10, ग्रामीण–अर्धशहरी भारत की हिंसक संरचनाओं को उजागर करने के लिए जाना जाता है। उसी दृष्टि की गूंज यहाँ सुनाई देती है, पर अधिक संयम और आत्मविश्वास के साथ।
कैमरा अक्सर ठहरता है- चेहरों पर, खाली गलियों पर, धुंध से ढके खेतों पर। लंबे शॉट और ठहरी हुई फ्रेमिंग यह संकेत देती है कि सत्य तत्काल प्रकट नहीं होता; वह धीरे-धीरे उभरता है। यह वातावरण-निर्माण केवल सौंदर्यशास्त्र नहीं, एक राजनीतिक वक्तव्य है।
हालाँकि, यही वातावरण कभी-कभी नाटकीय तनाव को कम कर देता है। निर्देशक का झुकाव मनोवैज्ञानिक गहराई की ओर अधिक है, जिससे कुछ दृश्य कथानक की तीव्रता खो बैठते हैं। फिर भी, इसे असफलता नहीं कहा जा सकता; यह थ्रिलर से अधिक सामाजिक-मनौवैज्ञानिक विमर्श को प्राथमिकता देने का सचेत निर्णय है।
अभिनय: मौन की तीव्रता
यदि यह सीज़न कहीं पूर्णतः सफल होता है, तो वह उसके अभिनय में।
मोना सिंह इंस्पेक्टर धनवंत कौर के रूप में एक जटिल, कामकाजी, संघर्षशील स्त्री को जीवंत करती हैं। उनके चेहरे पर अनुशासन है, पर आँखों में निजी थकान भी। वे अपने चरित्र को न तो आदर्श बनाती हैं, न शहीद- बल्कि मनुष्य के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिसकी दृढ़ता के भीतर करुणा भी है।
दूसरी ओर बरुन सोबती संयमित अभिनय का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनका चरित्र भीतर से टूटा हुआ है, किंतु वह टूटन प्रदर्शन में नहीं, बल्कि सूक्ष्म संकेतों में दिखाई देती है। उनका मौन संवादों से अधिक प्रभावी है।
दोनों कलाकार “पुलिस अधिकारी” की रूढ़ छवि से आगे जाकर मनुष्य को सामने लाते हैं- उसकी पारिवारिक उलझनें, व्यक्तिगत पछतावे और नैतिक दुविधाएँ। सहायक कलाकार भी इस यथार्थ को विश्वसनीय बनाते हैं। यह सामूहिक अभिनय है, जहाँ कोई पात्र बनावटी प्रतीत नहीं होता।
परिवार और संस्थाएँ: दो ध्रुव, एक संकट
सीज़न का सबसे मार्मिक पक्ष परिवार की पड़ताल है। घर- जो सुरक्षा का प्रतीक होना चाहिए- यहाँ संवादहीनता का स्थल बन जाता है। पिता-पुत्र के बीच पीढ़ीगत दूरी, पति-पत्नी के बीच अविश्वास, और बच्चों की चुप्पी- ये सब अपराध की कथा के समानांतर चलते हैं।
साथ ही, पुलिस व्यवस्था और राजनीतिक दबाव का चित्रण सूक्ष्म है। सत्ता यहाँ प्रत्यक्ष खलनायक नहीं, बल्कि अदृश्य दबाव की तरह उपस्थित है। सत्य की खोज केवल अपराधी तक पहुँचने का प्रश्न नहीं; वह सत्ता-संरचनाओं से जूझने की प्रक्रिया भी है।
अपराध व्यक्तिगत नहीं, संरचनात्मक है। और यही इस सीरीज़ का केंद्रीय तर्क है।
प्रवासन और पहचान का संकट
दूसरे सीज़न में प्रवासी आकांक्षाएँ और मुखर हैं। पंजाब के युवाओं के लिए विदेश केवल रोजगार नहीं, बल्कि पहचान का वादा है। पर जब यह वादा टूटता है, तो भीतर एक शून्य जन्म लेता है-एक ऐसी रिक्तता, जिसे भरने के लिए कभी-कभी हिंसा जन्म लेती है।
यह सीरीज़ संकेत देती है कि आर्थिक विकास के साथ यदि सांस्कृतिक और भावनात्मक आधार कमजोर हो जाए, तो समाज भीतर से खोखला हो जाता है। धुंध केवल खेतों में नहीं उतरती; वह चेतना पर भी छा जाती है।
धुंध का रूपक: दर्शन और राजनीति
धुंध यहाँ दृश्यात्मक तत्व से अधिक दार्शनिक प्रतीक है। वह सच को ढँकती भी है और उजागर भी करती है। जब तक धुंध रहती है, सब कुछ अस्पष्ट है; जैसे ही वह हटती है, कठोर यथार्थ सामने आता है।
सीरीज़ का अंत समाधान से अधिक प्रश्न देता है- और यही उसकी कलात्मक ईमानदारी है। वह दर्शक को उत्तर नहीं थमाती; वह उसे असहज करती है, सोचने पर मजबूर करती है।
निष्कर्ष: मनोरंजन से आगे, एक सामाजिक दस्तावेज़
कोहरा 2 को केवल ‘क्राइम थ्रिलर’ कहना उसके वैचारिक आयामों को सीमित करना होगा। यह समकालीन भारत का सांस्कृतिक पाठ है- जहाँ अपराध व्यक्तिगत नहीं, संरचनात्मक है; जहाँ धुंध बाहर कम और भीतर अधिक है।
सुदीप शर्मा का विचारशील निर्देशन, मोना सिंह और बरुन सोबती का सधा हुआ अभिनय, और पूरी टीम का यथार्थवादी दृष्टिकोण- सब मिलकर इस श्रृंखला को महज़ वेब-कंटेंट से उठाकर एक गंभीर सामाजिक वक्तव्य में बदल देते हैं।
यह सीज़न हमें उत्तेजित नहीं करता; वह हमें असहज करता है। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है।
धुंध छँटती है या और घनी होती है—यह प्रश्न दर्शक के मन में छोड़ दिया जाता है। और शायद कला का उद्देश्य भी यही है: उत्तर देना नहीं, बल्कि सही प्रश्न जगाना।