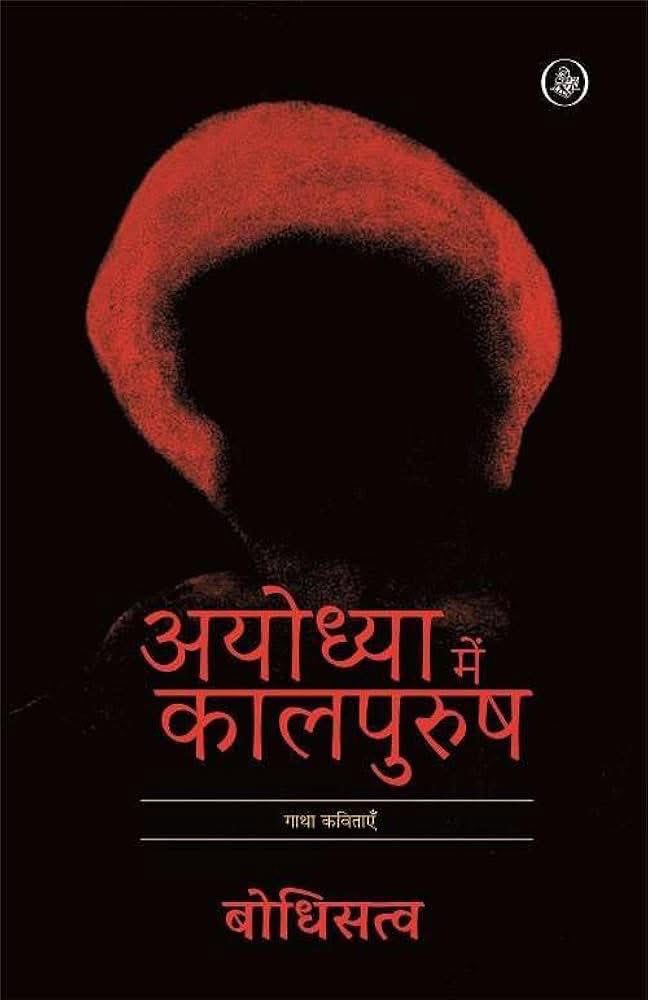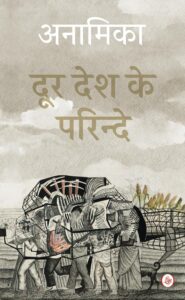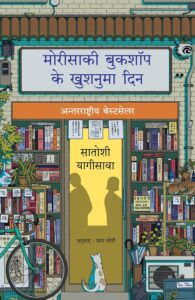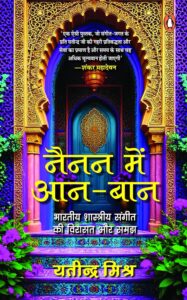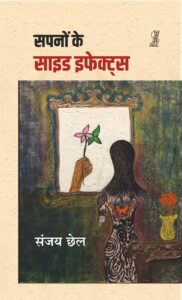बोधिसत्व के नवीनतम काव्य संग्रह ‘अयोध्या में कालपुरुष’ पर संजय जायसवाल की यह समीक्षा प्रस्तुत है – अनुरंजनी
============================================
लोकतांत्रिक मूल्यों की पक्षधरता का आख्यान: अयोध्या में कालपुरुष
‘अयोध्या में कालपुरुष’ गाथा कविताएं हिंदी के चर्चित कवि बोधिसत्व का नवीनतम काव्य संग्रह है। यह संग्रह मिथकीय एवं ऐतिहासिक कथाओं का एक ऐसा फ्यूजन है, जिसका संबंध इस दौर के यथार्थपरक घटनाओं से है। इस पुस्तक में संग्रहित कविताएं कवि निराला को समर्पित हैं और कवि कुंवर नारायण एवं कैलाश वाजपेयी की स्मृति में अर्पित हैं।
इस संग्रह को गाथा कविताओं के संकलन के तौर पर तैयार किया गया है। इस गाथा श्रृंखला में पुराण एवं इतिहास के आख्यानों से सजी नई मिज़ाज की कुल 11 कविताएं शामिल हैं। यह संग्रह स्वागतयोग्य है ।इसमें मिथकीय चरित्रों के साथ इतिहास-पुरुषों का काव्यात्मक पुनर्मूल्यांकन है या यूँ कहें कि उन पर गाथाएं लिखी गई हैं। बोधिसत्व की ये कविताएं एक लंबे कालखंड का रचनात्मक साक्षात्कार लगती हैं। त्रेता युग की रामकथा से लेकर वर्तमान के भारत-दुर्दशा तक की दर्जनों घटनाओं को पकड़ना एवं एक नए फॉर्म में फिट करना बिना व्यापक काव्यात्मक दृष्टि के संभव नहीं। बोधिसत्व का यह संग्रह भले ही मिथकीय रामायण, महाभारत एवं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के आधार पर लिखा गया है। परंतु इसका संदर्भ वर्तमान समय के मूल्यों से गहरे जुड़ा है।
बोधिसत्व ने निराला की ‘राम की शक्तिपूजा’ के राम की तरह ही अपने सभी महाकाव्य पुरुषों को सामान्य भाव भूमि पर खड़ा किया है जहाँ तमाम उदात्त, विराट एवं दिव्य नायक हताश, निराश, चिंतित एवं असहाय दिखते हैं। बोधिसत्व का यह संग्रह राजतांत्रिक व्यवस्था की पृष्ठभूमि पर भले ही लिखा गया है परंतु इसमें कवि लोकतांत्रिक मूल्यों के पक्ष में खड़ा दिखता है और ‘लोक’ के पक्ष में सवाल भी खड़ा करता है। इसमें संकलित ‘हिरणी को अयोध्या की रानी कौशल्या से विनय-पत्र’ कविता में बोधिसत्व मारे गए हिरण की पत्नी हिरणी की पीड़ा को समझते हैं। इस गाथा में राजा दशरथ हिरण को मांस के लिए मार देते हैं। इतना ही नहीं उसकी चमड़ी का ढपली बनाकर राम को खेलने के लिए भी दे दिया जाता है। यहां कविता का मार्मिक प्रसंग का जिक्र करते हुए कवि लिखता है- राम जब भी ढपली से खेलते हैं, उस ढपली की आवाज सुनकर हिरणी और उसके छौने हिरण की याद में व्यथित हो जाते हैं। हिरणी एकमात्र बचे चमड़ी को यादगार के तौर पर रखने के लिए हिरण की खाल यानी चमड़ी को वापस करने के लिए रानी कौशल्या से विनय करती है ताकि वे ऐसी स्मृतिजन्य वेदना से मुक्त हो सकें।यहां कवि की संवेदना परदुःखकातरता के भाव से भरकर हिरणी के मन तक पहुँच जाती है- “चमड़े की ध्वनि मन बहलाती है राम और महारानी माताओं का/ महाराज दशरथ का राजकुमारों का/ मंत्रियों सेनापतियों/ धनुर्धारी अहेरियों का/ वही आवाज मथ जाती है मन/ विवश हिरणी का/ उसके छोटे अबोध छौनों का।” यह गाथा सिर्फ हिरनी की पीड़ा का आख्यान भर नहीं है। दरअसल यहाँ कवि व्यवस्था, सत्ता और प्रभुत्वशाली लोगों की मानसिकता का भी जिक्र करता है। हमें समझना होगा आज विकास के नाम पर आदिवासियों का विस्थापन, धर्म और संप्रदाय के नाम पर जो रक्तपात हो रहा है दरअसल वह सुविधा संपन्न लोगों के लिए ‘सुख’ और मनोरंजन का विषय हो सकता है। ऐसे ही चरम सुख के स्वाद के लिए आज आम आदमी, गरीब, स्त्री, निर्धन जनता, आदिवासी, दलित सब ‘हिरण’ बन गए हैं। संवेदनशून्य और शक्तिशाली लोग धीरे-धीरे अपनी सत्ता और शक्ति के अहं में दूसरे की पीड़ा भूलते जा रहे हैं । हिरणी जब कौशल्या से निवेदन करती है, तब लगता है कवि बोधिसत्व की यह काव्य प्रतिभा दरअसल संवेदना और परदु:खकातरता के भाव से उपजी है। समभाव के कारण ही कवि ऐसा लिख पाता है- “कुंवर राम को खेलने के लिए कुछ और दिया जाए/ मेरे हिरण का चमड़ा खिलौना नहीं बना रह सकता/ उसे मारा राजा ने/ हमारे वन में घुसकर/ जब वह अपने छौनों के साथ खेल रहा था।” यह कविता जबरन अतिक्रमण, हिंसक मनोवृत्ति, लोभ के बढ़ते ग्राफ की ओर भी संकेत करती है। इस कविता में कवि एक और भयानक सच की ओर संकेत करता है। दरअसल रानी हिरणी की याचना के बाद उसकी भावना का कद्र करने की जगह उसपर अपनी इच्छा लादती है। वह चाहती है कि हिरणी को भी यहाँ रख लिया जाए ताकि वह ढपली का सामीप्य पा सके। यह भी आदेश हुआ कि हिरणी के खुरों से वन की मलीनता को धो-पोंछकर उसमें सोना मढ़वा दिया जाए। कवि बोधिसत्व शासक की मंशा को समझते हैं। वन की मलीनता को धोना असल में उसकी नैसर्गिकता और आदिम-वैशिष्ट्य को मिटाना ही है। आज विकास और प्रगति के नाम पर स्थानीयता पर सबसे ज्यादा प्रहार हो रहे हैं। विविधताओं को मिटाने की साजिश के विरुद्ध यह कविता हमें सचेत करती है। इतना ही नहीं इन दिनों जिस तेजी से झूठ और प्रलोभन की परते चढ़ाई जा रही हैं, वह भी चिंताजनक है। सोने का खूर मढ़वाने का अर्थ ही है- सच को ढंकना, इतिहास को विकृत करना या उसका पुनर्लेखन करना। कवि की सजग दृष्टि अपने समय के ऐसे बदलावों को चिन्हित करने में सफल है।
दूसरे गाथा ‘दाराशुकोह का पुस्तकालय और औरंगजेब के आँसू’ में कवि सत्तालोलुपता की घटना के जरिए मानवीय मूल्यों के अवमूल्यन की बात कहता है।इस कविता में हम देखते हैं कि किस तरह से ज्ञान के आकांक्षी, विद्याप्रेमी विद्वान दारा शुकोह को अपने ही छोटे भाई औरंगजेब की महत्वाकांक्षाओं का शिकार होना पड़ता है और बंदी बना लिया जाता है। दारा शुकोह को सत्ता से ज्यादा वेद पढ़ना, महाभारत का अनुवाद करना, काशी जाना और संस्कृत सीखना और उपनिषद को समझना पसंद था। यहां दारा शुकोह की हत्या असल में ज्ञान, विवेकपरकता, संवेदनशीलता, परस्पर सांस्कृतिकता और सांप्रदायिक सौहार्द की हत्या है। ऐसी हत्याएं सिर्फ मध्ययुगीन घटना नहीं है बल्कि आधुनिक समय में भी मानवीय मूल्यों के ऐसे शत्रु मौजूद हैं। आज सत्ता के चाटुकारों ने बड़े मूल्यों को विस्थापित कर दिया है।लोगों की स्वार्थपरता ने जन आंदोलनों की जमीन को भी कमजोर किया है। हालांकि कई लोग दारा के पक्ष में खड़े थे और कई लोगों को औरंगजेब ने अपने पक्ष में कर रखा था। दरअसल सत्ताएं हमेशा ज्ञान और शिक्षा को अपनी शत्रु समझती हैं। यही वजह है कि दारा शुकोह को कैद करना जरूरी हो जाता है।इस संदर्भ में कवि लिखते हैं- “कोई औरंगजेब नहीं चाहता कि/ दारा जिंदा होकर लौट आए/ सबको अपने पुस्तकालय ले जाकर/ सत्ता के खिलाफ सोचना सिखाए।” कवि को यहां जन सामान्य की उदासीनता भी चुभती है इसलिए कवि का यह मानना है कि बिना संगठित हुए और विवेकपूर्ण प्रतिरोध के हमारे लिए अपने ज्ञान और प्रेम के केंद्रों को बचाना मुश्किल है- “कोई दारा आंसुओं से नहीं बचता/ किसी भी दारा का पुस्तकालय/ केवल सदिच्छा से नहीं बचता।” ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि आज सबसे ज्यादा खतरा सद्भाव, ज्ञान, इतिहास और लोकतंत्र पर है।
दारा शुकोह की तरह ही बिम्बिसार भी अपने ही पुत्र अजातशत्रु की महत्वाकांक्षा का शिकार होता है। ‘अजातशत्रु और बिम्बिसार गाथा’ में बुद्ध में आस्था रखने वाले बिम्बिसार ताउम्र सत्य, प्रेम, समन्वय के पक्ष में खड़े रहने की बात सोचते हैं। बावजूद इसके वे सत्ता का मोह नहीं त्याग पाते हैं। वे बौद्ध धर्म के निकट थे फिर भी वे अपने भीतर के राजा को भला कहां दूर कर पाते हैं? राजा का स्वांग हो या स्वांग का राजा हो सब बस सत्ता, शक्ति और सुख के त्रिकोण में उलझकर रह जाता है – “पथ परिवर्तन से/ मन परिवर्तित नहीं हुआ करता अक्सर/ बिम्बिसार के साथ भी हुआ कुछ ऐसा ही/ युद्ध से मोह न छूटा उनका/ विजय की आकांक्षा न गई थी/ हिंसा से मन विमुख न हुआ था/ खड़ग रक्त से रंजित रहा सदैव।” बिम्बिसार के ऐसे कृत्य से उसके अपनों का विचलित नहीं होना ही स्वाभाविक है।यही वजह है कि रानी कोसला का अपने राजा के अन्यायपूर्ण कृत्य पर ग्लानि की जगह गर्व होता है। आज हिंसा को, शुद्धतावाद को, अंधराष्ट्रवाद को और अतार्किकता को ‘ग्लोरीफाई’ किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। रानी का यह कहना- “ सत्ता में बने रहने के लिए/ शक्ति अपने हाथ में रखना अनिवार्य है/ आपने विचार बदले हैं/ सत्ता के सूत्र साधे रहिए ” यह चिंताजनक है। हालांकि ऐसी मनोवृत्तियों के उभार के कारण आगे चलकर बिम्बिसार को गंभीर परिणाम भुगतना पड़ता है। इतिहास गवाह है जब सत्ता के लिए हिंसा ढाल बनती है तब क्रूरता का ग्राफ बढ़ता है। संभवतः यही वजह है कि कवि की आस्था राम, बुद्ध और गाँधी जैसे लोगों में है। हालांकि उनका ज्येष्ठ पुत्र अजातशत्रु गद्दी पर बैठने का आकांक्षी था। बिना तप के वह बुद्धत्व और सत्ता दोनों को हस्तगत करना चाहता था। इस गाथा में बोधिसत्व जिन संकटों की ओर संकेत करते हैं, एक दिन उसी विपर्यय का शिकार बिम्बिसार होते हैं- “एक संध्या जब बुद्ध को विदा करके/ लौट रहे थे राजभवन/ सम्राट बिम्बिसार/ उनको शयन कक्ष ले परिपथ से/ मोड़ दिया सैनिकों ने कारागार के पथ पर/ वीथिका में ही उतार लिया गया राजमुकुट/ राज-वस्त्र परिवर्तित किया गया/ कारागार पहुँचने के पहले/ यही नियम था राजबंदी के लिए।” ऐसी घटनाएं संबंधों के साथ पूरी सभ्यता को कलंकित करती हैं। ऐसी अन्यायपूर्ण परम्पराएं किसी भी सभ्य समाज के लिए घातक हैं।
इतिहास बोध से संपन्न कवि बोधिसत्व ने अपने आलोचकीय विवेक से सच और झूठ के बीच अपनी इस कविता को एक हस्तक्षेप की तरह दर्ज किया है। वे तमाम ऐतिहासिक एवं मिथकीय चरित्रों के जरिए अलग-अलग सभ्यताओं के बन रहे खंडहरों में मनुष्यता की तलाश करते हैं। वे राजतंत्र के हिंसा-प्रतिहिंसा के बीच ‘संस्कृत के कवि और फारसी बोलने वाले लड़की का प्रेम’ गाथा में प्रेम का विराट रूपक निर्मित करते हैं। इसमें प्रेम एक ओर तमाम तरह के बंधनों एवं जड़ताओं से मुक्ति के लिए संघर्षरत है वहीं दूसरी ओर धर्म के ठेकेदार प्रेम को लहूलुहान करने के लिए कूद पड़े हैं। काशी में रहने वाले ही भूल चुके हैं शिव-गंगा के विश्व प्रसिद्ध प्रेम को। कवि को इस बात की पीड़ा है कि उसी शिव की काशी में गंगा एक यवनी और अपने भक्त कवि को पवित्र न कर पाई- “जिस त्रिशूल पर काशी टिकी है वहीं/ शिव का त्रिशूल/ प्रेम करने वालों की छाती में गड़ा है/ हत्यारों का पक्ष आज भी बड़ा है/ डूबते को बचाने वाले मारे गए काशी में/ प्रेम करने वाले मारे गए काशी में/ घृणा करने वाले संहारक/ बने रहे काशी उद्धारक।” कवि एक पुरानी गाथा से नए जमाने के सच को उकेरता है। आज संस्कृति रक्षा के नाम पर हमारे यहाँ हत्यारे घूम रहे हैं।
इस संग्रह की पहली कविता ‘भारत दुर्दशा’ खो गए भारत की खोज है। बोधिसत्व देश के भीड़ बनने से चिंतित हैं। जिस देश को भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा के साथ, राम-कृष्ण, कबीर, सूर-तुलसी, रसखान, जायसी, मीरा, भारतेंदु, गाँधी, अम्बेडकर, रवीन्द्रनाथ, लोहिया, नेहरू आदि के साथ होना चाहिए आज वह देश सड़क पर है। सड़क पर होना एक अराजक स्थिति है। कवि भारत की वर्तमान दुर्दशा से मर्माहत है- “रास्ते में देश मिला/ भागता-दौड़ता चला जा रहा था/ मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो/ बहुत जल्दी में हो/ बोला उधर ही जिधर सब ले जा रहे हैं हांक कर।” आज भारत को नेता, धर्माचार्य, व्यापारी, निजीकरण के समर्थक, जातिवादी, प्रांतीयतावादी, अनपढ़, कट्टरवादी सब मिलकर अपने-अपने ढंग से हांक रहे हैं। दरअसल आज पूरे देश में एक तरह का विभाजन चल रहा है। सब बंटे हैं। अलग-अलग एक दूसरे से कटे। जबकि भारत के बनने को लेकर जो स्वप्न देखा गया था वह समावेशिकता की बुनियाद और भावात्मक अखंडता की जमीन पर खड़ा था । उसमें परस्पर सहभागिता और संबद्धता का भाव था। देश कभी भी आज की तरह खुदगर्ज़ और अकेला बिलकुल न था। कवि की यह कविता भारत की दुर्दशा से मुक्ति और अपने गौरव को वापस पाने का आख्यान है।
परिचय – डॉ. संजय जायसवाल, सहायक प्राध्यापक ,हिंदी विभाग, विद्यासागर विश्वविद्यालय, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल, मोबाइल- 9331075884