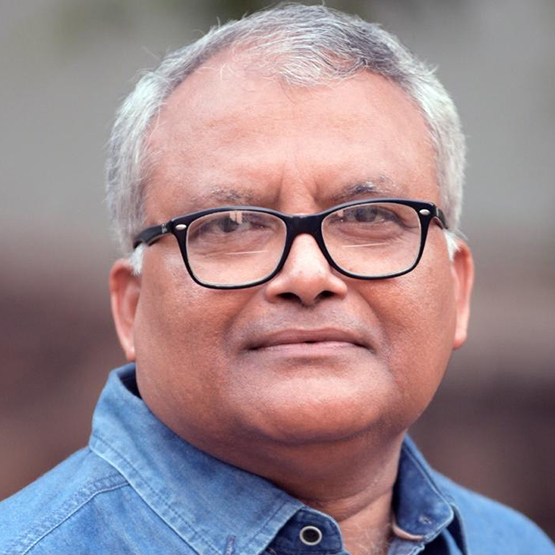विकास कुमार झा ऐसे उपन्यासकार रहे हैं जिन्होंने कुछ दशक पहले ‘मैकलुस्कीगंज’ नामक उपन्यास लिखकर एक भुला दिये गये क़स्बे को परिदृश्य पर ला दिया था। उनके प्रत्येक उपन्यास में एक भौगोलिक परिदृश्य होता है और उससे जुड़ी कहानी होती है, जिसे गोवा के परिदृश्य को लेकर लिखा गया उपन्यास ‘राजा मोमो और पीली बुलबुल’, या ‘वर्षावन की रूपकथा’ जैसा उपन्यास जो कर्नाटक के अगुम्बे गाँव को आधार बनाकर लिखा गया था, जहां ‘मालगुडी डेज़’ की शूटिंग हुई थी। उनके लेखन कर्म पर यह सुविचारित लेख लिखा है अंग्रेज़ी-हिन्दी के प्रसिद्ध लिटरेरी क्रिटिक आशुतोष कुमार ठाकुर ने- मॉडरेटर
===================
आशुतोष कुमार ठाकुर
हिन्दी साहित्य और पत्रकारिता में कुछ लेखक ऐसे हैं, जो सिर्फ़ शब्द नहीं लिखते; वे भूगोल, इतिहास और स्मृति को एक साथ साधते हैं. विकास कुमार झा ऐसे ही रचनाकार हैं. 10 जुलाई, 1961 को बिहार के सीतामढ़ी ज़िले के बैरगिनिया में जन्मे विकास कुमार झा हिन्दी पत्रकारिता के समर्थ हस्ताक्षर हैं. लेकिन उन्हें केवल पत्रकार कह देना उनके रचनात्मक विस्तार को सीमित कर देना होगा. वे उपन्यासकार हैं, कवि हैं, नाटककार हैं, जीवनीकार हैं और सबसे बढ़कर वे उस बेचैन भारतीय आत्मा के कथाकार हैं, जो लगातार अपने घर, अपनी जड़ों और अपनी पहचान की तलाश में भटक रही है.
विकास कुमार झा का लेखन सत्ता और समाज, इतिहास और वर्तमान, प्रकृति और मनुष्य, स्मृति और विस्मृति के बीच फैले जटिलताओं का लेखन है. उनकी रचनाओं में पत्रकार की तथ्यपरक दृष्टि है, लेकिन उसके साथ ही कवि का संवेदनशील हृदय और कथाकार की कल्पनाशीलता भी है.
पत्रकारिता: लोकतंत्र की बेचैनी
विकास कुमार झा की पत्रकारिता सत्ता से संवाद नहीं करती, उससे सवाल करती है. ‘बिहार में राजनीति का अपराधीकरण’ और ‘सत्ता के सूत्रधार: आज़ादी के बाद का भारत’ जैसी कृतियाँ भारतीय लोकतंत्र के उस पक्ष को प्रत्यक्ष करती हैं, जिसे अक्सर उत्सवधर्मिता के शोर में दबा दिया जाता है. यहाँ राजनीति आदर्श व्यवस्था के रूप में नहीं आती, बल्कि अपराध, जाति, धन और सत्ता के गठजोड़ के रूप में सामने आती है.
यह पत्रकारिता किसी सनसनी का निर्माण नहीं करती. असल में यह धीमी, धैर्यवान और बेचैन पत्रकारिता है. इसमें यह विश्वास निहित है कि सच को दर्ज करना भी प्रतिरोध का एक रूप है. बिहार की मुक्तिकामी जनता के संघर्ष में विकास कुमार झा की रचनात्मक हिस्सेदारी इसी विश्वास से जन्म लेती है.
कथा-साहित्य: भूगोल का पुनर्पाठ
पत्रकारिता के समानान्तर विकास कुमार झा का कथाकार आकार लेता है. उनके उपन्यास और अन्य रचनाएँ उस भारत की ओर लौटती हैं, जो चमकते महानगरों से बाहर है. यह वह भारत है जहाँ गाँव, कस्बे, जंगल, पहाड़ और समुद्र-तट अब भी मनुष्य की नियति तय करते हैं.
‘मैकलुस्कीगंज’, ‘गयासुर संधान’, ‘वर्षावन की रूपकथा’ और ‘राजा मोमो और पीली बुलबुल’ जैसे उपन्यास बताते हैं कि विकास कुमार झा का रचनात्मक भूगोल असाधारण है. इसके अलावा उनकी काव्यकृतियाँ, जैसे ‘इस बारिश में’ मैथिली नाट्य रचनाएँ ‘जमपुत्र’ और सोनमछरिया, तथा बांग्ला-भाषियों के जीवन पर आधारित परिचय-पत्र जैसी पुस्तकें उनके बहुआयामी साहित्यिक विस्तार को स्पष्ट रूप से उद्घाटित करती हैं.
बिहार की मुक्तिकामी जनता और उपेक्षित समुदायों के संघर्ष में उनकी रचनाएँ सदैव सक्रिय रचनात्मक हिस्सेदारी निभाती हैं.
मैकलुस्कीगंज: स्मृति का नगर
विकास कुमार झा का उपन्यास मैकलुस्कीगंज हिन्दी साहित्य में केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक गहन प्रश्न के रूप में उपस्थित होता है. यह प्रश्न किसी एक गाँव तक सीमित नहीं है, बल्कि वह पूछता है, क्या कोई समुदाय, कोई स्मृति, कोई बस्ती इतिहास की प्रक्रिया में पूरी तरह मिट सकती है? और यदि मिटती है, तो क्या वह केवल भूगोल से मिटती है या मनुष्य की चेतना से भी?
राँची के निकट बसा मैकलुस्कीगंज एंग्लो-इंडियन समुदाय का एक स्वप्न था. भारत की आज़ादी से लगभग डेढ़ दशक पहले अस्तित्व में आया यह गाँव उन लोगों के लिए आश्रय बना, जिनकी पहचान औपनिवेशिक इतिहास की उपज थी, जो न पूरी तरह अंग्रेज़ थे, न पूरी तरह भारतीय. यह मिश्रित पहचान राष्ट्र-राज्य के इतिहास के लिए हमेशा असुविधाजनक रही है. स्वतंत्रता के बाद सत्ता बदली, प्राथमिकताएँ बदलीं, पर मैकलुस्कीगंज की नियति नहीं बदली. 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद यह गाँव प्रशासनिक रूप से बिहार से अलग हो गया, लेकिन उपेक्षा, असुरक्षा और विस्मृति की पीड़ा जस की तस बनी रही.
उपन्यास का मूल प्रश्न आज भी उतना ही तीखा है, क्या एक दिन पृथ्वी के नक़्शे से मैकलुस्कीगंज का नामोनिशान मिट जाएगा? या यह पहले ही इतिहास की स्मृति से बाहर फेंका जा चुका है?
यह उपन्यास विस्थापन की कथा है, लेकिन यह विस्थापन केवल भौगोलिक नहीं है. यह सांस्कृतिक, मानसिक और ऐतिहासिक विस्थापन का आख्यान है. यहाँ बूढ़े लोग हर शाम बीते समय को याद करते हैं, पुराने चर्च, स्कूल, क्लब और जीवन की उस लय को, जो अब केवल स्मृति में बची है. वहीं युवा पीढ़ी भविष्य के नाम पर विदेशों के पते गिनाती है. इस तरह मैकलुस्कीगंज धीरे-धीरे एक जीवित गाँव से बदलकर एक स्मृति-स्थल में रूपांतरित होता जाता है.
साहित्य में शहर और कस्बे जब कथा के केन्द्र में आते हैं, तो वे मात्र पृष्ठभूमि नहीं रहते, वह इतिहास और चेतना के सक्रिय पात्र भी बन जाते हैं. ओरहान पामुक की ‘इस्तांबुल’ स्मृति और सामूहिक अवसाद का शहर है, इतालो काल्विनो की ‘इनविज़िबल सिटीज़’ कल्पना और मनोविज्ञान के नगर हैं, और खुशवंत सिंह की ‘दिल्ली’ सत्ता, हिंसा और समय की परतों का दस्तावेज़. इसी परम्परा में, भले ही आकार में वह एक कस्बा हो, मैकलुस्कीगंज हिन्दी साहित्य में एक शहर-स्मृति की तरह उपस्थित होता है.
पामुक के इस्तांबुल में जिस सामूहिक उदासी, का अनुभव है, वही भाव मैकलुस्कीगंज में भी व्याप्त है. फर्क बस इतना है कि इस्तांबुल इतिहास के केन्द्र में रहा, जबकि मैकलुस्कीगंज इतिहास की हाशिये पर खड़ा रहा. काल्विनो के अदृश्य नगरों की तरह मैकलुस्कीगंज भी धीरे-धीरे भौतिक से अधिक मानसिक भूगोल बन जाता है, एक ऐसा नगर, जो नक़्शे पर तो मौजूद है, पर राष्ट्रीय स्मृति में लगभग अदृश्य है.
उपन्यास की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह एंग्लो-इंडियन समुदाय को किसी संग्रहालय की वस्तु की तरह प्रस्तुत नहीं करता. वे यहाँ जीवित मनुष्य हैं, डरते हुए, प्रेम करते हुए, उम्मीद और निराशा के बीच झूलते हुए. उनके साथ-साथ उपन्यास में आदिवासी जीवन भी समानान्तर चलता है. दोनों समुदायों के जीवन-दर्शन भिन्न हैं, लेकिन उनकी नियति में उपेक्षा, असुरक्षा और सन्ताप साझा है. राज्य और बाज़ार—दोनों—इन दोनों को हाशिये पर रखते हैं.
विकास कुमार झा इन समुदायों के बीच कोई कृत्रिम सामंजस्य नहीं गढ़ते. वे केवल यह दिखाते हैं कि इतिहास की बेरुख़ी सबके लिए समान होती है, चाहे वह औपनिवेशिक स्मृति का बोझ ढोता समुदाय हो या सदियों से उपेक्षित आदिवासी समाज.
मैकलुस्कीगंज इस अर्थ में एक महत्त्वपूर्ण सिटी हिस्ट्री और नगर-समाजशास्त्रीय दस्तावेज़ भी है. इसमें झारखंड की सामाजिक-राजनीतिक समस्याएँ, छोटानागपुर अंचल का भूगोल, प्रशासनिक उदासीनता और सांस्कृतिक विघटन एक अनुभूत सत्य की तरह उपस्थित हैं. कथा को आगे बढ़ाने के लिए जहाँ-तहाँ कल्पना का सहारा लिया गया है, लेकिन यह कल्पना यथार्थ को ढकती नहीं, बल्कि उसे और अधिक तीखा बनाती है.
यह उपन्यास पतझड़ और बसंत के कालचक्र की तरह है, जहाँ जीवन बार-बार उम्मीद करता है और समय बार-बार उसे तोड़ता है. मैकलुस्कीगंज केवल अतीत की कहानी नहीं है, यह हमारे वर्तमान पीढ़ी की भी कथा है, जो वैश्विक बाज़ारवाद की दौड़ में अपनी जड़ों से कटती जा रही है. यह उपन्यास चेतावनी देता है कि जब स्मृति टूटती है, तो केवल गाँव नहीं टूटते, मनुष्य भी टूटता है.
गयासुर संधान: मिथक और यथार्थ का संगम
विकास कुमार झा का उपन्यास ‘गयासुर संधान’ कथ्य और शिल्प दोनों स्तरों पर हिन्दी उपन्यास-परम्परा में एक महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप है. यह कृति केवल कथा-विस्तार नहीं करती, भारतीय सांस्कृतिक चेतना, आस्था और दर्शन की परतों को खोलती है. गया और बोधगया यहाँ साधारण भौगोलिक स्थल नहीं, मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा के प्रतीक बनते हैं.
गयासुर की पौराणिक कथा के माध्यम से लेखक अनैतिक कामनाओं, अतृप्त इच्छाओं और एषणाओं के क्षय की दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत करता है. उपन्यास यह रेखांकित करता है कि गया मृत्यु और पितृ-श्राद्ध की भूमि होने के साथ जीवन के अहंकार और वासना के क्षरण का क्षेत्र भी है. इहकाल और परकाल के बीच फैला हुआ महाशून्य मनुष्य को आत्ममंथन की ओर ले जाता है.
यह उल्लेखनीय है कि गया और बोधगया, बनारस जैसे सांस्कृतिक नगरों के निकट होने के बावजूद, हिन्दी साहित्य में अपेक्षाकृत कम उपस्थित रहे हैं. बनारस पर केन्द्रित साहित्य की एक लम्बी परम्परा रही है, जहाँ वह आध्यात्मिकता, मृत्यु-बोध और आधुनिकता के द्वन्द्व का प्रतीक बनता है. इसके विपरीत, गया और बोधगया, जिनकी दार्शनिक और ऐतिहासिक महत्ता किसी भी दृष्टि से कम नहीं, साहित्यिक कल्पना में हाशिये पर रहे हैं.
‘गयासुर संधान’ इस रिक्तता को भरता है. यह उपन्यास गया-बोधगया को आस्था-पर्यटन के स्थलों के रूप में नहीं, एक जीवित सांस्कृतिक भूगोल के रूप में रचता है. यहाँ मिथक और यथार्थ, इतिहास और वर्तमान, लोकविश्वास और दार्शनिक चिन्तन एक-दूसरे में घुलते हैं. यह संलयन कथा को गहन और प्रभावी बनाता है.
इस अर्थ में ‘गयासुर संधान’ सांस्कृतिक आत्मचिन्तन का आख्यान भी है और मनुष्य के भीतर छिपे भय, सत्य और आत्मबोध की खोज भी. यह उपन्यास पढ़ने से अधिक अनुभव की माँग करता है और हिन्दी साहित्य में गया-बोधगया जैसे उपेक्षित नगरों को एक सुस्पष्ट सांस्कृतिक स्थान देता है.
वर्षावन की रूपकथा: अगुम्बे का सौंदर्यशास्त्र
‘वर्षावन की रूपकथा’ कर्नाटक के अगुम्बे गाँव पर केन्द्रित होकर भी केवल किसी स्थान-विशेष की कथा नहीं कहता. यह उपन्यास प्रकृति और मनुष्य के रिश्ते की एक नैतिक व्याख्या है. निरंतर वर्षा, घने जंगल, पहाड़ और बादलों की संगति से निर्मित अगुम्बे यहाँ एक जीवित इकाई की तरह उपस्थित होता है, ऐसा लगता है मानो यह गाँव स्वयं कथा बोल रहा हो.
शंकर नाग और ‘मालगुडी डेज़’ के प्रसंग इस उपन्यास को भारतीय सांस्कृतिक स्मृति से जोड़ते हैं. जब शंकर नाग अगुम्बे में आर.के. नारायण के काल्पनिक मालगुडी को साकार करते हैं, तब यह गाँव कल्पना और यथार्थ के बीच सेतु बन जाता है. इस क्षेत्र के साहित्य और लोकनाट्य की परंपरा, विशेषकर महान कन्नड़ लेखक कोटा शिवराम कारंथ की कृतियाँ और उनकी प्राकृतिक संवेदनाएँ, उपन्यास की धरातल को और समृद्ध करती हैं. कारंथ की कहानियाँ स्थानीय भूगोल, वनस्पति और पारिस्थितिकी के अनुभव से गहरी जुड़ी हैं, और ‘वर्षावन की रूपकथा’ उसी परंपरा को आधुनिक कथ्य और दर्शन के साथ जोड़ती है.
बाज़ारवाद के उन्मत्त और हिंसक समय में अगुम्बे मनुष्यता का एक दुर्लभ हरित मंडप बनकर उभरता है. विकास कुमार झा के यहाँ सुन्दरता केवल दृश्य या प्राकृतिक वैभव नहीं, बल्कि करुणा, सादगी और संतुलन का जीवन-मूल्य है. यह उपन्यास पाठक को धीमा होना सिखाता है.
गोवा और ‘उल्लास की नाव’
विकास कुमार झा का गोवा-केन्द्रित ‘राजा मोमो और पीली बुलबुल’ उपन्यास किसी प्रदेश का पर्यटन-वर्णन नहीं, बल्कि गोवा को एक सांस्कृतिक पाठ की तरह पढ़ने का गंभीर साहित्यिक प्रयास है. हिन्दी साहित्य में जहाँ गोवा प्रायः समुद्र-तटों, संगीत और अय्याशी की छवियों तक सीमित रहा है, वहाँ यह उपन्यास उसके भीतर छिपे अवसाद, स्मृति और नैतिक विघटन को उजागर करता है. इस अर्थ में यह कृति ‘मैकलुस्कीगंज’, ‘वर्षावन की रूपकथा’, और ‘गयासुर संधान’ की ही वैचारिक कड़ी में खड़ी दिखाई देती है, तीनों उपन्यास उन स्थलों की कथा कहते हैं, जो बाहर से रमणीय और भीतर से टूटे हुए हैं.
1947 के बाद भी चौदह वर्षों तक पुर्तगाली शासन में रहने का इतिहास गोवा की सामूहिक चेतना पर गहरी छाया डालता है. लेखक दिखाते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता अपने आप में सांस्कृतिक मुक्ति नहीं होती. गोवा की पीड़ा औपनिवेशिक अतीत से उतनी नहीं, जितनी उत्तर-औपनिवेशिक भारत में बाज़ार और सत्ता द्वारा उसके निरन्तर दोहन से उपजती है.
इस उपन्यास में गोवा एक ऐसे शरीर की तरह उभरता है, जो बाहर से आकर्षक और भीतर से रोगग्रस्त है.
विकास कुमार झा की विशेषता यह है कि वे गोवा को केवल ‘स्थल’ नहीं बनाते, बल्कि उसे पात्र में बदल देते हैं. इसके समुद्र-तट, चर्च, गाँव और खामोश रातें मिलकर एक ऐसा कोलाज रचती हैं, जिसमें सौन्दर्य और क्षरण साथ-साथ चलते हैं.
हिन्दी साहित्य में गोवा को केन्द्रीय विमर्श में लाने का यह प्रयास महत्त्वपूर्ण है. यह उपन्यास पूछता है—क्या कोई संस्कृति लगातार बाज़ार, सत्ता और उपभोग की मार सहते हुए अपनी आत्मा बचा सकती है? लेखक इसका उत्तर नहीं देते; वे पाठक को गोवा की चमक और अंधेरे के बीच छोड़ देते हैं. यही इस उपन्यास की सबसे बड़ी साहित्यिक उपलब्धि है.
उषा उथुप की जीवनी ‘उल्लास की नाव’ में लेखक एक बिल्कुल अलग रंग में दिखाई देते हैं. यह केवल एक प्रसिद्ध गायिका की कहानी नहीं, बल्कि उस स्त्री की आंतरिक यात्रा है, जिसने पॉप संगीत को भारत में गरिमा, आत्मविश्वास और वैश्विक पहचान दी. उषा उथुप का समुद्र-सा जीवन, उनकी बहुभाषिकता और उनका अटूट उल्लास लेखक की संवेदनशील दृष्टि से और भी आलोकित हो उठता है.
स्मृति का लेखक
विकास कुमार झा मूलतः स्मृति के लेखक हैं. पढ़ते हुए मिलन कुंदेरा का कथन याद आता है: सत्ता के विरुद्ध संघर्ष भूलने के विरुद्ध स्मृति के संघर्ष के समान है.
उनकी रचनाओं का केंद्र वे स्थान, समुदाय और अनुभव हैं, जिन्हें इतिहास अक्सर हाशिये पर छोड़ देता है. मिटती बस्तियाँ, विस्थापित समुदाय, घायल भूगोल और थकी हुई आत्माएँ उनके लेखन में बार-बार लौटती हैं. वे विस्मृति के विरुद्ध लिखते हैं.
‘मैकलुस्कीगंज’ इस स्मृति-लेखन का सर्वोत्तम उदाहरण है. यह केवल एंग्लो-इंडियन समुदाय की कथा नहीं, बल्कि हर उस समुदाय की कहानी है, जिसकी पहचान इतिहास के दबाव में धुँधली पड़ रही है. यह निरीह और भावुक कौम की पीड़ा के पक्ष में खड़ा एक नैतिक दस्तावेज़ है.
आज, जब साहित्य तेजी से उपभोक्ता वस्तु बन रहा है, झा का लेखन ठहरने, देखने और याद रखने की ज़िद सिखाता है. उनका लेखन धीमा आत्मबोध है और यही उनकी सबसे बड़ी साहित्यिक उपलब्धि है.
(आशुतोष कुमार ठाकुर एक मैनेजमेंट प्रोफेशनल हैं, साहित्य और कला पर नियमित लिखते है.)