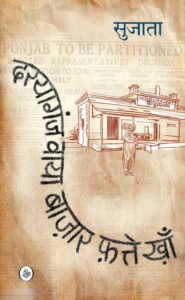स्त्रियों की लिखी प्रेम कहानियों को आधार बनाकर जाने माने आलोचक राकेश बिहारी ने यह लेख लिखा है। अपनी तरह के इस अनूठे लेख को आप भी पढ़ सकते हैं- मॉडरेटर
==================
हिन्दी की कुछ अविस्मरणीय प्रेम कहानियों के बहाने समय के साथ प्रेम के बदलते स्वरूप पर विचार करने की मंशा से जब मैंने कुछ कहानियों की सूची बनाई तो बिना किसी कालक्रम के अनुशासन में बंधे अनायास ही सबसे पहले ध्यान में आने वाली कहानियाँ थीं- ‘तीसरी कसम’, ‘रसप्रिया’, ‘कोसी का घटवार’, ‘परिंदे’, ‘उसने कहा था’, ‘पुरस्कार’, ‘आकाशदीप’… आदि-आदि। इस सूची में शामिल किसी कहानी विशेष के प्रेम कहानी होने न होने की बहस को थोड़ी देर के लिए परे छोड़ दें तो, इन सारी कहानियों को अमूमन हिन्दी की यादगार प्रेम कहानियों की सूची में शुमार किया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त इन कहानियों में जो एक बात समान है, वह है- इन सारी कहानियों के लेखकों का पुरुष होना। इस तथ्य के अहसास भर से मेरे समक्ष सहज ही कई प्रश्न खड़े हो उठे। क्या स्त्री लेखकों ने यादगार प्रेम कहानियाँ नहीं लिखी हैं? क्या स्त्री कहानीकारों द्वारा लिखी गई प्रेम कहानियों पर चर्चा नहीं होती है? या फिर यह मेरी ही दृष्टि की सीमा है? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने की मंशा से सबसे पहले मैंने हाल ही में गोवा में सम्पन्न हुये कथादेश के वार्षिक आयोजन ‘कथा समाख्या’, जो प्रेम की अवधारणा और दुनिया की चुनिंदा प्रेम कहानियों पर केंद्रित था, में शामिल कहानियों की सूची पर गौर किया। शंपा शाह द्वारा चयनित स्पेनिश भाषा की लेखिका इसाबेल एलिन्दे की कहानी ‘दो शब्द’ को छोड़ दें तो उस आयोजन में शामिल लगभग एक दर्जन प्रेम कहानियों में, जिसमें अधिकांश हिन्दी की ही थीं, एक भी कहानी किसी स्त्री लेखक की नहीं थी। इसके बाद मैंने प्रेम कहानियों के कुछ संकलनों, सूचियों, सर्वेक्षणों आदि पर भी निगाहें दौड़ाई। बीसवीं सदी की प्रेम कहानियों की ऐसी सूचियों में स्त्री लेखकों द्वारा लिखी कुछ इक्की-दुक्की कहानियाँ यथा- ‘यही सच है’ (मन्नू भण्डारी) और ‘बादलों के घेरे’ (कृष्णा सोबती) जैसी कहानियों को छोड़ दें तो यहाँ भी सिर्फ पुरुष कथाकारों की कहानियाँ हीं दिख रही थीं। हाँ, इक्कीसवीं सदी की कहानियों पर केन्द्रित संकलनों में युवा स्त्री कथाकारों की उपस्थिति जरूर उत्साहजनक दिखी। पिछले पचास वर्षों की समयावधि में अलग-अलग पीढ़ी की तीन स्त्री कथाकारों द्वारा लिखी गई कुछ चुनिन्दा कहानियों पर आधारित यह लेख ऊपर उल्लिखित प्रश्नों के उत्तरों की पड़ताल की दिशा में एक लघु प्रयास है। यदि इसके बहाने प्रेम के स्त्री मनोविज्ञान और उसके युगीन विकासक्रम को समझने के कुछ सूत्र भी मिल जाएँ तो मैं इसे इसकी एक अतिरिक्त उपलब्धि मानूँगा।
प्रसिद्ध अमेरिकन मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने अपनी पुस्तक ‘मोटिवेशन एंड पर्सनैलटी’ में मनुष्य की क्रमबद्ध आवश्यकताओं के संबंध में एक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है, जिसे ‘आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत’ के रूप में जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि इस सिद्धान्त के अनुसार आवश्यकताओं के पदानुक्रम में मैस्लो ने प्यार की आवश्यकता को तीसरे स्थान पर रखा है। उक्त सिद्धान्त के अनुसार शारीरिक आवश्यकता और सुरक्षा की आवश्यकता इस पदानुक्रम में क्रमशः पहले और दूसरे क्रम पर स्थित है। मैस्लो ने आत्मसम्मान और आत्मबोध को इस पदानुक्रम में क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर रखा है। इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए कि शारीरिक आवश्यकताओं में भोजन, पानी, वस्त्र, निद्रा आदि के साथ यौन आवश्यकताओं को भी शुमार किया जाता है। इस तरह यह सिद्धान्त प्यार को न सिर्फ एक आवश्यकता का दर्जा देता है बल्कि यौन संबंध और प्यार को एक दूसरे से अलग भी करता है। इस आधार पर यौन संबंध स्थापित करने या होने के लिए प्रेम की अनिवार्यता के मिथक को सहज ही नकारा जा सकता है। लेकिन इन आवश्यकताओं के बीच पदानुक्रम का संबंध होने के कारण प्रेम सम्बन्धों में देह संबंधों की उपस्थिति या यौनाकर्षण को उतनी ही सहजता से नहीं नकारा जा सकता। पदानुक्रम का यही संबंध प्यार और आत्मसम्मान के बीच भी एक अंतर्संबंध का निर्माण करता है। क्रमबद्ध तरीके से आवश्यकताओं की प्राप्ति होने के कारण मैस्लो के इस सिद्धांत को मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा का सिद्धान्त भी माना है। प्रथम चरण की प्राप्ति होने के पश्चात ही दूसरे चरण की आवश्यकता महसूस करने में विश्वास करने वाले इस सिद्धान्त की मानें तो प्यार की आवश्यकता महसूस करने के पहले मनुष्य देह संबंध की आवश्यकताओं को पूरा कर चुका होता है।
अब्राहम मैस्लो के इस सिद्धान्त और इससे ध्वनित होनेवाले इन संकेतों के आलोक में अपनी चिंतन यात्रा जारी रखते हुये मुझे 1973 में प्रकाशित मृदुला गर्ग की कहानी ‘अवकाश’ और उसकी नायिका मिनी की याद हो आती है। कहानी के शुरुआती दृश्य में कथानायिका मिनी अपने पति महेश से कहती है- “मैं समीर से प्यार करती हूँ, मुझे तलाक चाहिए।” इक्कीसवीं सदी का लगभग एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है। इस छोटी सी कालावधि में व्यवहार और पारस्परिकता की जाने कितनी आचार संहिताएँ टूटी और पुनर्निर्मित हुई हैं। बावजूद इसके, स्त्री-पुरुष सम्बन्धों के पारंपरिक व्याकरण के अभ्यस्त पाठकों को आज भी यह संवाद बेतरह विचलित कर सकता है। ऐसे में इस बात का सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 51 वर्ष पूर्व लिखे गए इस संवाद ने तब पाठकों के मानस पर किस तरह के प्रभाव अंकित किए होंगे। प्रेम (सुविधा के लिए फिलहाल इसे विवाहेतर कह लेते हैं) के स्वीकार के साथ अत्यधिक शांत और सहज माहौल में पति को लगभगा दुलराते हुये समझाती मिनी अपने निर्णय के प्रति प्रतिबद्ध है। लेकिन इस क्रम में अंत तक आते-आते कहानी एक और अप्रत्याशित करवट लेती है। कहानी के उस दृश्य का सार प्रस्तुत करने के बजाय पाठकों को सीधे उस दृश्य तक ही ले चलना उक्त घटना के प्रभावों की गहनता को ठीक-ठीक समझने के लिए जरूरी है-
“मैं तुम्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकता,” करुणा से पिघलकर उसने कहा। सोफ़े पर बैठ उसका सिर अपनी छाती पर खींच, वह धीरे-धीरे उसकी पीठ सहलाने लगी।
“मुझे माफ करो,” उसने फिर कहा और अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिये। उनका हृदय समुद्र के समान हो रहा है, विशाल, अथाह और शांत। बहुत स्नेह है वहाँ, बहुत दया। वह उसे दुलराती गई, प्यार करती गई। उसके शरीर का एक-एक अंग उसका जाना-पहचाना है। लज्जा या दिखावा बाकी नहीं है और न ही आखेट की गंध।
कुछ देर महेश का शरीर कठोर बना रहा, फिर पिघलने लगा। वे एक झिलममिलाते पर्दे के पीछे सच्चाई से छिप गए। अहम को खोकर आदि पुरुष और आदि नारी में बदल गए। उसके पास देने को जो है, वह उसे दे देना चाहती है, जो स्नेह बाकी है, जितनी करुणा सँजो सकती है। जब वे एक शरीर हुये तब भी वह यही सोचती रही, महेश दुख मत करना… मेरा बेचारा प्यारा महेश… तुम भी सुखी हो सको, मेरी तरह सुखी…
वह फौरन उठकर बाथरूम में चली गई। लगा धो देने से ही सबकुछ धुल जाएगा। पानी डालते-डालते उसने सोचा, यह तो सर्दी से ठिठुरते भिखारी पर दुशाला डाल देने जैसी बात हुई। जाना तो मुझे है ही।”
‘अवकाश’ कहानी का यह अंतिम दृश्य जिसमें कथानायिका मिनी अपने पति के साथ उत्कट दैहिक अंतरंगता के क्षण स्वेच्छा और सहजता से जी रही है, को क्या प्रेम की दैहिक अभिव्यक्ति कहा जा सकता है? उपर्युक्त उद्धरण में आए वाक्य ‘वह उसे दुलराती गई, प्यार करती गई’ पर गौर करें तो ऐसा ही लगता है, लेकिन इस दृश्य (कहानी के भी) के आखिरी दो वाक्य इस निष्कर्ष को न सिर्फ प्रश्नांकित करते हैं बल्कि एक खास तरह की दृढ़ता के साथ इसे खारिज भी कर देते हैं। पति पत्नी के बीच देह संबंध ‘जरूरतों’ की पूर्ति का नतीजा भी हो सकता है, जो दैनंदिनी के अभ्यास से सहज ही अर्जित हो जाता है। इसके लिए उनके बीच प्रेम की पारस्परिकता का होना अनिवार्य नहीं। थोड़ी देर को कहानी में घटित इस विशेष क्षण को उस अभ्यास का उपक्रम न भी मानें तो ‘ठिठुरते भिखारी पर दुशाला डाल देने’ वाली बात इस घटना को करुणा या दया से उत्पन्न सदाशयता से जोड़ती है, जिसका ‘प्रेम’ या ‘प्यार’ से कोई विशेष रिश्ता नहीं है। गौरतलब है कि इस छोटी सी कहानी में प्यार या प्रेम शब्द का एक दर्जन से ज्यादा बार इस्तेमाल हुआ है। दो-एक बार ये प्रयोग तो लगभग अंतर्विरोधी भी मालूम पड़ते हैं। ‘समीर से प्यार करती हूँ’ की स्वीकृति से शुरू हुई इस कहानी में आगे मिनी अपने पति से यह भी कहती है- ‘तुमसे भी मैं बहुत स्नेह और प्यार करती हूँ।’ संबंधों में अंतर्निहित भावनाओं के लिए उपयुक्त शब्दों के अभाव में कथानायिका भले प्रेमी और पति दोनों को प्यार करने की बात कह रही हो, लेकिन बच्चे और परिवार के साथ जुड़ाव के नाजुक संवेदना तंतुओं के अहसास के बावजूद तलाक के निर्णय पर उसकी अडिगता और पति के साथ घटित अत्यंत अंतरंग साहचर्य के कुछ क्षणों बाद ही ‘जाना तो मुझे है ही’ का निर्णयात्मक आत्मबोध, ‘प्यार’ (समीर के लिये) और ‘प्यार’(महेश के लिए) के बीच के अंतर को रेखांकित कर जाता है। मिनी की जुनूनी आत्मस्वीकृति और तलाक के दृढ़ निश्चय तथा महेश की शांत प्रतिक्रिया के बीच फैली यह कहानी ऊपर से भले कोई तूफान नहीं खड़ा करती हो, लेकिन मिनी के अंतर्विरोधों के बीच से निकली दृढ़ता और उसकी दृढ़ताओं के भीतर से झाँकता अंतर्विरोध पाठकों के भीतर जिस तरह की बेचैनी और उद्वेलन पैदा करते हैं, वही इस कहानी को ‘कहानी’ बनाते हैं। कहानी यह भी स्पष्ट करती है कि स्नेह, दया, करुणा, सहानुभूति जैसे भाव प्यार के बहुत आसपास भले दिखते हों, पर प्यार इन सबसे अलग होता है। प्रसंगवश नासिरा शर्मा की बहुत ही खूबसूरत कहानी ‘शामी कागज़’ का अंतिम दृश्य मेरे स्मृति पटल पर कौंध रहा है… पाशा को जीवन के नए मोड़ पर नई ज़िंदगी शुरू करने की सलाह देता महमूद उसके लिए सालों इंतजार कर सकने की बात करता है। तब कुछ देर खामोश रहने के बाद पाशा कहती है- “मोहब्बत और हमदर्दी का फ़र्क तो तुम जानते हो न, महमूद?” पाशा और मिनी के चरित्र में एक उल्लेखनीय अंतर होने के बावजूद ‘अवकाश’ कहानी की मिनी के मन में पति महेश के साथ कुछ पल पहले बिताए अंतरंग क्षणों के लिए उपजा ‘ठिठुरते भिखारी पर दुशाला डाल देने’ का भाव और ‘शामी कागज़’ की पाशा के उपर्युक्त प्रश्न में एक दूसरे की अनुगूँजे साफ सुनी जा सकती हैं। शामी कागज़ में पाशा का प्रश्न ठोस और बेधक तो है ही, लेकिन उसे ताकत अगली पंक्ति से मिलती है- “माथे पर छलक आई बूंदों को रुमाल से पोंछते हुए महमूद ने आहिस्ता से कहा- ‘मुझे माफ करना पाशा।’” पाशा की निगाहें मोहब्बत और हमदर्दी के फ़र्क को तो समझती ही थीं, उसकी साफबयानी ने महमूद को भी उस अंतर के मर्म तक पहुंचा दिया। यदि ऐसा नहीं होता तो माफी मांगते हुए बूंदें उसके माथे पर नहीं, उसकी आँखों में उतरतीं। ‘अवकाश’ में तलाक के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान महेश के साथ घटित मिनी की अंतरंगता जहां दया और करुणा से उपजी है, वहीं ‘शामी काग़ज़’ में महमूद का पाशा को अपने साथ नई ज़िंदगी शुरू करने का दिया गया प्रस्ताव हमदर्दी और सहानुभूति से उपजा है। अक्सर जिस भाव को प्रेम समझ लिया जाता है, वह वास्तविक प्रेम से कैसे अलग होता है, ये कहानियाँ इस तथ्य को गहराई से रेखांकित करती है।
एक बार फिर ‘अवकाश’ की तरफ लौटते हैं। छोटी कहानियाँ चुस्त तो होती हैं, लेकिन उनकी एक सीमा यह होती है कि वे अपने कथानक से उत्पन्न कई जरूरी सवालों के उत्तर नहीं दे पातीं। ‘अवकाश’ इस मामले में कुछ हद तक इसका अपवाद है। मिनी को समीर से प्यार हो गया है। वह उसके सान्निध्य के लिए महेश से तलाक लेना चाहती है। इस कहानी को पढ़ते हुए किसी पाठक के मन में यह जानने की सहज ही जिज्ञासा हो सकती है कि मिनी ने समीर में ऐसा क्या पाया जिसे वह ‘प्यार’ कह रही है? इस प्रश्न को पलट कर भी पूछा जा सकता है कि महेश के ‘प्यार’ में किस तरह का अभाव था कि मिनी का उसके लिए प्रतिदान प्रेम के बदले सहानुभूति तक ही आकर ठहर गया? कहानी मिनी की आत्मस्वीकृति, उसके जुनून और निर्णय की दृढ़ता को अपने समय से बहुत आगे जाकर तो पकड़ती ही है, इन प्रश्नों के उत्तर तक पहुँचने का रास्ता भी दिखाती है-
“पिछले दो वर्षों में ऐसे अनेक क्षण आए हैं, जब उसने यही सोचा है कि शारीरिक सुख के अलावा इसमें और कुछ नहीं है। पर वे क्षण भी वह भुला नहीं पाती जब समीर के साथ रहकर लगा, शरीर कुछ नहीं है, वे मन-मस्तिष्क से एक हैं। लगा, उसे स्पर्श किए बगैर, उसके साथ बातें करते या चुप रहकर वह पूरा जीवन सुख से बिता सकती है।”
मन-मस्तिष्क से एक होना हो या स्पर्श के बगैर बातें करना, या फिर चुप रहकर जीवन सुख से बिता सकने की सुखद संभावना की कल्पना, ये सब सम्मिलित रूप से मानसिक और भावनात्मक साझेदारी के साथ एक दूसरे की निजता के सम्मान की तरफ इशारा करते हैं। कहने की जरूरत नहीं कि ‘अवकाश’ की कथानायिका का यह आत्मालाप महेश और उसके संबंधों के बीच की रिक्तियों की तरफ भी इशारा करता है। ऐसे में समीर से प्यार हो जाने को उस रिक्ति की पूर्ति भी कहा जा सकता है।
लोग प्यार में क्यों पड़ते हैं? क्यों किसी का प्यार लंबे समय तक चलता है तो किसी का दो दिन भी नहीं टिकता? इसे ‘प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है’ के बहुश्रुत जुमले से नहीं समझा जा सकता है। प्यार और प्यार जैसे अन्य भावनात्मक लगावों, उनके लक्षणों और प्रभावों को समझने की कोशिशें मनोवैज्ञानिकों ने लगातार जारी रखी हैं। सन 1970 में प्यार और पसंदगी के बीच स्थित बारीक अंतरों को विश्लेषित करते हुए नामचीन मनोवैज्ञानिक रुबीन ने लगाव, देखभाल और अंतरंगता को प्यार के तीन घटकों की तरह रेखांकित किया था। एक अन्य मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 1986 में प्रेम के त्रिकोणीय सिद्धांत को प्रस्तावित करते हुए अंतरंगता, जुनून और प्रतिबद्धता को प्रेम के तीन जरूरी तत्व बताया। यदि इन दोनों ही सिद्धांतों को मिला दें तो लगाव, देखभाल, अंतरंगता, जूनून और प्रतिबद्धता में जुनून को छोड़कर प्यार के शेष चार लक्षणों को अभ्यास से भी अर्जित किया जा सकता है। विश्व प्रसिद्ध पुस्तक ‘आर्ट ऑफ लविंग’ में एरिक फ्रॉम इसे ही प्रेम के उन सिद्धांतों की तरह रेखांकित करते हैं, जिन्हें सीखकर मनुष्य खुद को प्यार किए जाने लायक बना सकता है।
ऊपर मैंने यह बताया कि ‘अवकाश’ कहानी इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि मिनी ने समीर में ऐसा क्या देखा जिसके कारण उसे उससे प्यार हो गया। इसे छोटी कहानी की जरूरत कहें या ‘अवकाश’ की सीमा, मृदुला गर्ग उस तरफ संकेत करने के लिए आत्मालाप या आत्मवीक्षा का सहारा लेती हैं। इस प्रविधि से पाठकों की जिज्ञासा का जवाब तो मिल जाता है लेकिन इस क्रम में मिनी के भीतर का वह लोक बहुत गहराई से उद्भासित नहीं होता। वैसे ही, पति के समक्ष प्रेम के आत्मस्वीकार तक पहुँचने की यात्रा का कश्मकश व उस अंतराल की मानसिक और भौतिक उथलपुथल को भी ‘अवकाश’ गहराई में जाकर नहीं पकड़ती। इसके लिए कहानी को बहुत विस्तार की जरूरत होती। नासिरा शर्मा की एक अन्य कहानी ‘संगसार’ का उल्लेख यहाँ इसलिए जरूरी है कि यह ‘अवकाश’ कहानी के उस अभाव की भरपाई गहरी संवेदना के साथ करती है। ‘अवकाश’ में मिनी की जिन मनोदशाओं का कोई पाठक सिर्फ अनुमान ही लगा सकता है, ‘संगसार’ की आसिया उसे शिद्दत से साकार करती है-
“आसिया के दिमाग ने दिल को समझाया, मगर दिल तन को न समझा सका। यह कोशिश भी जब बेकार गई तो हिम्मत करके आसिया ने तय किया कि वह अफजल को सबकुछ बता देगी, कुछ नहीं छिपाएगी। इस तरह तनाव में हर रात बसर करना उसके बस की बात नहीं है। उसके सारे तन्तु टूट रहे हैं। वह अफजल को सुख देने की जगह एक चिंता में डुबो देती है। फैसला कर वह उस रात आराम से सोई, मगर सुबह उठते ही उसे दूसरी फिक्र लग गई।
*** *** ***
अंत में उसने फैसला ले लिया कि अफजल को अभी आराम से जाने दे, मगर जिस दिन वह वापस आएगा, उसे वह अपना फ़ैसला सुना देगी।”
इस प्रसंग से गुजरते हुए आसानी से समझा जा सकता है कि आसिया के मनोमस्तिष्क में उठता-गिरता यह तूफान मिनी के मनोजगत का किस तरह पता देता है। मिनी जानती है कि उसके भीतर समीर के प्रति दैहिक आकर्षण है, लेकिन वह मन-मस्तिष्क के बहाने अपने प्रेम को एक दिव्य और अशरीरी स्वरूप देने का भी जतन करती मालूम पड़ती है। शारीरिक सुख की बात को स्वीकार करते हुए भी शरीर को नगण्य बनाकर पेश करना उसकी आध्यात्मिकता है या किसी खास तरह की परदेदारी या वर्जना, यह चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन देह के स्वीकार और नकार की यह अभिसंधि उसके मन पर छाए कुहासे की तरफ कुछ हद तक इशारा तो करती ही है। लेकिन प्रेम और देह की स्वीकारोक्ति को लेकर आसिया के समक्ष किसी तरह का धुंधलका नहीं है। अंतर और बाह्य के सहज द्वन्द्व के बीच प्रेम में देह की तुष्टि को वह बहुत बेबाकी और साहसिकता के साथ स्वीकार करती है। इस क्रम में आसिया की उसकी माँ और बहन के साथ जो बातचीत होती है, उस पर ठहर कर सोचा जाना चाहिए –
“तुम अफजल को जलील कर रही हो हो?
“बिलकुल नहीं, वह बिस्तर पर मेरा पूरक नहीं है, यह मैं जानती हूँ। उसका जोड़ा भी कहीं होगा और…”
“मैं भी इस घर में पैदा हुई, पली-बढ़ी और अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, कम और ज्यादा का संतुलन बनाकर शादीशुदा ज़िंदगी को खुशहाल बनाने की हम दोनों कोशिश करते हैं, मगर तुम? तुम भी तो उसी घर में पैदा हुईं, पली-बढ़ीं और अचानक यह तब्दीली… वह भी शादी से पहले नहीं, शादी के बाद, आखिर क्यों?”
“इसलिए कि मोहब्बत ने मेरा दरवाजा खटखटाया है।” आसिया ने कहा सहज स्वर में, मगर उसके तेवर को देखकर आसमा के माथे पर पसीना छलक आया।”
आसिया और उसकी बहन आसमा के बीच ऐसे बेधक संवादों के कई-कई उदाहरण कहानी में मौजूद हैं। आसिया के शब्द और व्यवहार में व्याप्त सहजता और तेवर का सम्मिश्रण न सिर्फ उसकी साफ दृष्टि का परिचय देता है, बल्कि परिवार, समाज और व्यवस्था की तरफ से खड़ा किए गए उसके प्रतिपक्षी के मस्तिष्क पर भी बल डालने में कामयाब होता है। आसिया मिनी (अवकाश) की तरह मोहब्बत का सिर्फ स्वीकार भर नहीं करती, बल्कि उससे दो कदम आगे बढ़कर बहन के आगे जैसे उसका ऐलान-सा करती है। इस बात का भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि इस प्रसंग के पहले आसिया ने आसमा से उसके जीवन का सच भी जानना चाहा था- “सच बताना, क्या वह सब तुम्हें अपने शौहर से मिला जिसकी तमन्ना एक औरत के दिल में रहती है या सिर्फ हर साल एक अदद औलाद का तोहफा मिलता रहा?” आसिया के इस सवाल के जवाब में पहले तो आसमा हँसते हुए ‘हाँ’ कहती है, लेकिन बाद में इसकी संजीदगी को समझकर वह हँसना भूल जाती है और अपनी ‘हाँ’ में छिपे ‘झूठ’ को ही अपना जेवर बताने लगती है। फिर आसिया के ऐलाने मोहब्बत को सुनकर आसमा के माथे पर पसीना छलक आना भी तो उसके उसी झूठ को रेखांकित करना है, जिसे वह जेवर समझ कर पहनती रही है। नासिरा शर्मा आँसू और पसीने के फर्क को समझती हैं। ‘शामी कागज़’ के आखिरी दृश्य में महमूद के माथे पर छलक आई बूंदें हों या फिर यहाँ आसमा के माथे पर छलक आया पसीना, दोनों का आस्वाद तो एक जैसा ही है।
इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए कि आसिया मोहब्बत में जिस्म की मौजूदगी को बिना किसी वर्जना के स्वीकार तो करती है, लेकिन उसके लिए यह मुहब्बत के राह की पहली नहीं, आखिरी सीढ़ी है- “दूर से पैदा हुई कशिश पहले ही दिन तन-गाथा में नहीं बदली थी, बल्कि जब दोनों हर तरह के तर्क, अंकुश और व्यथा पर विजयी हो गए तो इस मुकाम पर पहुंचे थे।”
‘संगसार’ की एक खासियत यह भी है कि इसमें वर्णित मोहब्बत की गाथा किसी युगल विशेष के बीच घटित होनेवाले प्रेम-संबंधों के मानसिक, भावनात्मक और दैहिक पक्षों तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि परिवार और समाज के अन्य किरदारों को शामिल करते हुए प्रेम, समय और समाज के तिराहे पर घटित होनेवाली लैंगिक राजनीति के बृहत्तर प्रश्नों से भी टकराती है।
‘अवकाश’ और ‘संगसार’ को आमने सामने रखते हुए इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए कि दोनों ही कहानियों की केन्द्रीय चरित्र ऐसी स्त्रियाँ हैं, जिनका असली प्रेम दाम्पत्य से बाहर है। दोनों ही कथानायिकाएं अपने इस प्रेम को स्वीकारती भी हैं। लेकिन क्या कारण है कि ‘अवकाश’ में मिनी का देह संबंध प्रत्यक्षतः पति महेश के साथ घटित होता है और प्रेमी के साथ देह संबंध का जिक्र दृश्य में नहीं कथन में आता है, जबकि ‘संगसार’ की आसिया के संदर्भ में यह बात ठीक उलटी है। मिनी और आसिया की स्वीकृतियों और यौन व्यवहारों का यह अंतर इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि मिनी की वर्जनाएं जहां दिमागी और मानसिक स्तर पर टूट रही हैं, वहीं आसिया के भीतर यह सब व्यवहार और जज़्बात के स्तर पर घटित हो रहा है। यहाँ यह उल्लेख किया जाना भी जरूरी है कि ‘अवकाश’ जहां सत्तर के दशक की शुरुआत में लिखी गई वहीं ‘संगसार’ आठवें दशक के अंत या नौवें दशक की शुरुआत में। क्या इन दोनों कहानियों के बीच के इस फासले को समय के फासले की तरह भी नहीं देखा जाना चाहिए?
हंस, मई 2023 में प्रकाशित नाज़िश अंसारी की पहली कहानी ‘हराम’, जिसे उस वर्ष का ‘राजेन्द्र यादव हंस कथा सम्मान’ भी दिया गया था, की चर्चा भी यहाँ प्रासंगिक लगती है। स्त्री, प्रेम और दाम्पत्य का जो त्रिकोण ‘अवकाश’ और ‘संगसार’ में देखने को मिलता है, इस कहानी में वह एक अलग और बदले हुए स्वरूप में सामने आया है। पहली दो कहानियों की तरह प्रेम यहाँ भी दाम्पत्य के बाहर है, पर वह शादी के बाद नहीं, पहले ही घटित होता है। ‘अवकाश’ और ‘संगसार’ की कथानायिकाएं जहां क्रमशः अपने पति और बहन के समक्ष स्वयं के प्रेम में होने को स्वीकार करती हैं, वहीं ‘हराम’ की नायिका सकीना हैदर को अपनी शादी तय होने की सूचना देती है। ‘मैं समीर से प्यार करती हूँ, मुझे तलाक चाहिए’ (‘अवकाश’) के ठीक उलट सकीना यहाँ हैदर से कहती है- ‘शाम को मेरा निकाह है।’ इन दोनों वाक्यों के बीच अर्थ, संवेदना और निर्णय का एक लंबा फासला है। भर पेट भोजन, तन भर वस्त्र और सर पर छत की सुरक्षा के बाद सकीना को मुहब्बत की जरूरत थी। हैदर मुहब्बत का जीता-जागता प्रतिरूप था, लेकिन अम्मा के सामने वह वह इसका इकबाल नहीं कर सकी। उसके पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। उसे इस बात का पूरा अहसास था कि उसकी माँ ने किस श्रम और संघर्ष से उसे पाला है। इसलिए अपनी शादी के प्रस्ताव पर उन्हें खुश देख वह उनके आगे बिलकुल चुप हो जाती है। रोहिणी अग्रवाल और रश्मि रावत जैसी प्रमुख स्त्रीवादी आलोचकों ने इस कहानी को स्त्री अस्मिता और माँ-बेटी के संबंध की दृष्टि से व्याख्यायित किया है। कहानी के प्रति रोहिणी अग्रवाल की असहमति और रश्मि रावत की सहमति में स्त्री अस्मिता और ग्लोबल सिस्टरहुड को समझने के कई सूत्र मौजूद हैं। यह इस कहानी का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष है भी। लेकिन प्रस्तुत चर्चा उसके प्रेम पक्ष पर ही केंद्रित है। सकीना एक आज़ादख्याल स्त्री है और उसकी माँ पितृसता की सताई, लेकिन उसी से अनुकूलित एक पारंपरिक श्रमिक स्त्री। वैचारिक स्तर पर एक दूसरे के विपरीत होने के बावजूद स्त्री होने का साझापन उन्हें एक दूसरे के आमने-सामने नहीं खड़ा करता।
धर्म (संप्रदाय के अर्थ में) जहां व्यक्ति को बांधने और संकुचित करने का काम करता है, वहीं प्रेम मुक्त और विस्तारित करने का। इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि इक्कीसवीं सदी के दो दशक बीतने के बाद भी इस कहानी में सकीना प्रेम का स्वीकार नहीं करती, बल्कि एक गहरी खामोशी के साथ बिला हील हुज्जत शादी के लिए तैयार हो जाती है। ठीक निकाह के दिन किसी तरह परीक्षा का पर्चा लिखने के बाद कहानी के आखिरी दृश्य में कॉलेज के सबसे उजाड़ हिस्से में वह हैदर से आखिरी बार मिल रही है-
“पत्थर से फूटे झरने को रोकने की चाह में होंठ पलकों पर रखे ही थे कि रोकते हुए हैदर ने कहा – ‘यह हराम है सकीना!’
वह पीछे हटी, ठहरकर उन आँखों में झाँकते हुए पूछा, “…और शाम को जो मुझसे कुबूलवाया जाएगा, वो हलाल होगा क्या?’ दोनों तरफ खामोशी फैल गई। कुछ देर के लिये मुसलसल खामोशी।
फिर अचानक रात से बिंधे बादल छूटे और स्लेटी आसमान टूट के सुरमई धरती का मुंह चूमने लगा। बेतहाशा…हाँ, पहली और आखिरी बार।”
प्रेम विद्रोह करने की ताकत और साहस दोनों देता है। लेकिन सकीना अपनी माँ से विद्रोह करने की बात तो दूर, अपने प्रेम का स्वीकार करने का साहस भी नहीं दिखा सकी। हैदर के साथ देह-संबंध बनाने को हराम और हलाल से जोड़कर देखें तो मजहबी मान्यताओं और वसूलों से विद्रोह की एक तस्वीर यहाँ जरूर बनती दिखाई पड़ती है। लेकिन वह भी सिर्फ सतह पर। यदि सकीना निकाह के समय गर्भवती होती तो धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध यह एक स्पष्ट और मूर्त विद्रोह हो सकता था, लेकिन परिवार और समाज से कटकर दो लोगों के बीच बना एक गोपनीय देह-संबंध, जिसे जमाने के आगे कभी जाहिर भी नहीं होना है, को विद्रोह कैसे कहा जा सकता है? इक्कीसवीं सदी की एक पढ़ी-लिखी लड़की, जिसे कायदे से अपनी अकेली माँ की ताकत भी बनना चाहिए था, अपने लिए भी आवाज नहीं उठा पाती!
सकीना के संवाद ‘और शाम को जो मुझसे कुबूलवाया जाएगा, वो हलाल होगा क्या?’ से गुजरते हुए भी एक बार इस बात का अहसास होता है कि वह बेमन की शादी को हलाल नहीं समझती। पर यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि उसने एक बार भी न तो अपनी माँ से हैदर के बारे में कोई बात ही की है, न ही शादी से इनकार किया है। ऐसे में ‘मुझसे कुबूलवाया जाएगा’ में जबरनपने का जो भाव ध्वनित होता है, क्या वह असत्य और आरोपित नहीं है? इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए कि हैदर बेरोजगार है, जबकि सुहैल, जिससे सकीना की शादी तय हो रही है, एक धनाढ्य परिवार से आता है-
“हमीदा! जो गुरबत हमने देखी थी, इंशा अल्लाह हमाई बच्ची नहीं देखेगी, कितनी छोटी चीजों के लिए हम तरस के रह गए। पूरी ज़िंदगी दिल को समझाते ही कटी। लेकिन अब मेरी बेटी को किसी चीज की कमी नहीं रहेगी।”
सकीना की माँ ने बिना उससे पूछे उसकी जिंदगी का फ़ैसला ले लिया, उन जैसी पारंपरिक और पितृसत्ता से अनुकूलित स्त्री का यह फैसला स्वाभाविक भी है। लेकिन दिल में उठ रहे मरोड़ को दबाकर सकीना का चुप रह जाना खटकता है-
“अम्मा को बताया भी नहीं जा सकता कि मैं किसी और से प्यार… सुनते ही गला दबा देंगी। काश! हैदर के पास भी खूब पैसे होते…तंगहाली के मामले में दोनों के नसीब एक से निकले।”
सच्चा प्रेम हालात के आगे इतनी आसानी से समर्पण नहीं करता। सकीना की चुप्पी और समर्पण का असली कारण अम्मा का भय या उनकी खुशी नहीं है जिसकी तरफ कहानी की कुछ पंक्तियाँ इशारा करती-सी दिखती हैं। हैदर के लिये उसकी चाहत, जिसे कहानी पहली नजर का प्यार की तरह रेखांकित करती है, दरअसल किशोर या युवा वय का आकर्षण भर है। सकीना जीवन की व्यावहारिकता और दुनियादारी को न सिर्फ ठीक से समझती है, बल्कि अपनी जरूरतों के प्रति जागरूक भी है। हैदर और सकीना के बीच घटित संबंध को लेखिका के शब्द भले ‘पहली और आखिरी बार’ बता रहे हों, सकीना जिस तरह हराम और हलाल की अवधारणा पर तंज करती है, उसे देखते हुए यह तय नहीं माना जा सकता कि यह संबंध फिर से दुहराया नहीं जाएगा। यदि हम यहाँ अब्राहम मैस्लो के ‘आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत’ का सहारा लें तो, इसी कारण वह प्रेम के स्वीकार के पहले शरीर और सुरक्षा की जरूरतों के पूरा होने की गारंटी चाहती है। इसीलिए सकीना के भीतर मिनी या आसिया की तरह वह जुनून नहीं पैदा होता जो विद्रोह करने का साहस देता है। कहने को तो यह भी कहा जा सकता है कि सकीना शादी से पूर्व प्रेमी के साथ संबंध बनाने का निर्णय इसलिए लेती है कि उस अंतरंग स्मृति के सहारे अपना शेष जीवन बिता सके। ऐसे में यह प्रश्न भी सहज ही पूछा जा सकता है कि यदि हैदर के साथ उसे सचमुच का प्रेम है, तो उसे आजीवन याद रखने के लिए देह की जरूरत क्यों है? इन प्रश्नों के उत्तर एकरैखिक नहीं हो सकते। सकीना भूमंडलोत्तर समय की एक ऐसी स्त्री है, जो देह, प्रेम और दाम्पत्य के बीच की एकसूत्रता को अपरिहार्य नहीं मानती। उसके लिए ये तीनों अलग और आजाद अवधारणाएं हैं। इसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि यह एक ऐसे समय की कहानी है जब प्रेम, दाम्पत्य और देह परस्पर इतने जटिल और प्रतिच्छेदी हो चुके हैं कि इनकी कोई मुकम्मल छवि साकार नहीं होती। इसलिए सकीना (‘हराम’) के जीवन और यौन व्यवहारों को मिनी (‘अवकाश’) और आसिया (‘संगसार’) के आगे कमतर बताकर इस विमर्श को समाप्त नहीं मान लेना चाहिए। बाजार, जरूरत और विकल्पहीनता की अभिसंधि पर खड़े इस समय में लगातार क्षरित हो रहे प्रेम को बचाने के लिये इनकी जटिलताओं और चुनौतियों को समझा जाना जरूरी है।
***
(आज की जनाधारा साहित्य वार्षिकी में प्रकाशित)
राकेश बिहारी
जन्म : 11 अक्टूबर 1973, शिवहर (बिहार)
कहानी तथा कथालोचना दोनों विधाओं में समान रूप से सक्रिय
प्रकाशन : वह सपने बेचता था, गौरतलब कहानियाँ (कहानी-संग्रह)
केंद्र में कहानी, भूमंडलोत्तर कहानी (कथालोचना)
सम्पादन : स्वप्न में वसंत (स्त्री यौनिकता की कहानियों का संचयन),‘खिला है ज्यों बिजली का फूल’ (एनटीपीसी के जीवन-मूल्यों से अनुप्राणित कहानियों का संचयन), ‘पहली कहानी : पीढ़ियां साथ-साथ’ (‘निकट’पत्रिका का विशेषांक) ‘समय, समाज और भूमंडलोत्तर कहानी’ (‘संवेद’ पत्रिका का विशेषांक)’, बिहार और झारखंडमूल की स्त्री कथाकारों पर केन्द्रित ‘अर्य संदेश’ का विशेषांक, ‘अकार- 41’ (2014 की महत्वपूर्ण पुस्तकों पर केन्द्रित), दो खंडों में प्रकाशित ‘रचना समय’ के कहानी विशेषांक, ‘पुस्तकनामा’ साहित्य वार्षिकी के दो अंक ।
‘स्पंदन’ आलोचना सम्मान (2015), वनमाली कथा आलोचना सम्मान (2024) तथा सूरज प्रकाश मारवाह साहित्य सम्मान से सम्मानित।
संपर्क: B53, सृजन विहार , एन टी पी सी कॉलोनी, पोस्ट – कोहराड़ घाट, मेजा, जिला प्रयागराज -212301(उत्तर प्रदेश)
मोबाईल – 9425823033; ईमेल – brakesh1110@gmail.com