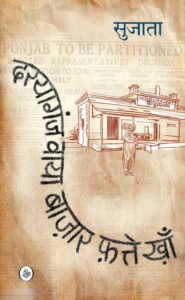महेंद्र मधुकर हिंदी के प्रोफ़ेसर रहे हैं, कवि-गीतकार-उपन्यासकार महेंद्र जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे हैं। आज पहली बार जानकी पुल पर उनकी कुछ कविताएँ पढ़िए-
==============================
बंधु से
कहाँ जा रहे हो बंधु?
दिगंत और अंतरिक्ष लाँघते
हवा चीरते
दुर्गम पगडंडियाँ गढ़ते
कहाँ जा रहे हो बंधु?
तुम्हारे चरणों के नीचे
पहाड़ दब रहे हैं
पृथ्वी चरमरा रही है
आंतकित हैं नदियाँ
विक्षुब्ध है वारिधि-विस्तार
चंचल हो गया है अखिल दृश्य-पट
आखिर कहाँ जाना है तुम्हें?
किस छाया के लिए
ढूँढ़ रहे हो वट-वृक्ष
कौन-सा जलाशय नीलवर्णी
या कमल-वन गंधच्छायी?
तुम्हें मालूम नहीं
सूर्य माथे पर चमक रहा है
गर्म हो गई है बालुका राशि
फेनिल हो रहा है नदी-जल
हवा के घोड़े चल पड़ने को हैं
कोड़े फटकार रहा है समय
कैसा समुद्र-मंथन चल रहा है!
खुल रहा है रहस्य
अमृत से पहले मिलता है विष
और इसे पीना पड़ता है सदा
दूसरों के लिए।¨¨¨
जन्म
चलो,
क्योंकि चलने से ही
कम होंगी दूरियाँ
घटेगा दुखों का बाढ़-पानी
रास्तों का टेढ़ापन
भला लगेगा।
इसी तरह
बस कुछ ऐसे ही
गढ़ी जाती हैं पगडंडियाँ
बड़े-बड़े पहाड़ भी
जमीन के पास सरक आते हैं।
मिट्टी से जान-पहचान बढ़ाओ
यह-
आदमी की सबसे बड़ी दोस्त है
खाई, खंदक, कीचड़, नाले
सब इसी की इकाइयाँ हैं।
बढ़ो-
क्योंकि तुम्हारा उन्माद अक्षय है
अमोघ है तुम्हारी हँसी।
आह! वर्षा में सिंची
थलथला रही है मिट्टी
यही वक्त है बीज बनने का
कँपकँपाकर
नए साँचे में
दुबारा जन्म लेने का।¨¨¨
आमंत्रण
आ, तू मुझे सभी इन्द्रियों से छू
मेरी साँस में हवा-सी बह
मेरे रक्त में नाच
मेरी त्वचा पर खिल
मेरी आँखों में रूप बन ठहर
मेरी उँगलियों को
मंदराचल-सी कस
मथ दे प्राण का खौलता समुद्र
पा लेने दे परम फल।
आ, गंधलतिके, तू आ, मुझे घेर
किसी ज्वार की तरह डुबा
अपने सागर की नील शÕया पर
लेने दे रस-निद्राएँ
पुरातन कथानायकों की तरह
घूम आने दे
मर्त्य, स्वर्ग और पाताल
इन्हीं में चुन लेने दे
अपना पात्र, अपना देश
बनने दे पूरा का पूरा मनुष्य
यही हो मेरा परिचय
यहीं मिले मेरा अस्तित्व। ¨¨¨
आग
मैं खोजने निकला हूँ आग
आग जो सूरज के पिटारे में बंद है।
चारों तरफ बह रही है
कोहरे की अनाम नदी
सफेद बादल शीशों पर जमे
आँखों पर पट्टी बाँधे हुए है रोशनी
रात सन-सी सफेद गांधारी की पट्टी जैसी
जो जहाँ है वहीं ठहरा हुआ
हाड़ हिलाती हुई हवा
बर्छियों की तरह चल रही है।
घिसो अपनी ठंडी उँगलियाँ
टकराने का मौका दो पत्थरों को
जमीन से निकल आओ
तैरते हुए लावे की तरह
कम-से-कम हमारे ठंडे होते पाँव
चलने की कूबत तो पा लेें!
चलो ढूँढ़ें हम आग
परमात्मा की जगह
आग जो किसी ठिठुरे नंगे आदमी की
देह पर कंबल की तरह थपकती है
आग जो किसी बच्चे को गोद में
लेते समय मीठी नींद बन जाती है।
ओ वैश्वानर,
आकाश से टूटो,
जैसे बिजलियाँ
सूखे पेड़ों को लहका देती हैं
आदमी की देह में
धधकती हुई, भूख बन जाओ
धूप-सा तपो, इतना तपो
कि कामगार के पसीने भी उसे
बुझा न सकें
उबलता हुआ गरम लोहा पानी बन जाए
और हम प्रतीक्षा करें
जब यह तरल ऊष्मा
इस्पात में ढल जाए।
हमारी आत्मा की तरह।¨¨¨
देना
देना आसान नहीं होता
उस पर दे देना सब कुछ।
सब कुछ दे भी दो
तो भी कुछ-न-कुछ बचा रह जाता है।
अक्सर हमने वे चीजें ही तो दी हैं
जो हमारी अपनी नहीं थीं
मसलन चाँद, तारे, पर्वत, गुफाएँ
नदी, निर्झर, समुद्र-जल और खुला आसमान
और यह बड़ी पृथ्वी भी
जिसके एक नाखून के हजारवें हिस्से के दावेदार बन
हम गेंडुली मारकर बैठे थे,
ये सब हमारे हों न हों
पर मुझे तो हमेशा लगा
जब मैं अपनी खुशी बाँटता हूँ
तो तुझे चाँद की ठंडक का एहसास होता है
मैं जब भी नाराज हुआ हूँ
अपनों या दूसरों से
या फिर कभी अपने आप से
तो धीरे-धीरे सुलगता हुआ सूर्य
मेरे भीतर धधकने लगता है
या जब भी कभी मैं प्रेम करता हूँ
तो मुझे लगता है मैं ही तो हूँ समूची पृथ्वी
पर्वतों का लंबा समुदाय
या आकाश छूता देवदारु का वृक्ष
जब भी संकल्प के लिए मैंने उठाए हाथ
मैं नदियों के बिल्कुल पास होता हूँ।
मंत्र पढ़ते समय मेरी बुदबुदाहट
मेरी अस्फुट प्रार्थनाएँ
लताओं, वनस्पतियों और औषधियों का
कुशल-क्षेम पूछती हैं।
मैं हवा से सीखता हूँ
देश और काल में लगातार बने रहने का गुर।
मुझे पसंद हैं यात्रएँ
अपने अलावा दूसरों को देखना
कभी खुले मैदानों में चरते हुए
बनैले पशुओं के पीछे भागते चलना।
तब मुझमें दिखाई देने लगता है
आक्षितिज फैला अनंत आकाश
एक साँस लेता हुआ ब्रह्मांड
अनंत देवता, अग्नि, वरुण, यम, वायु
सब मेरी साँस में आते-जाते हैं।
मैं ही हूँ फूटता हुआ ज्वालामुखी
या समुद्र के क्षोभ का हलाहल
मैंने आजतक दूसरों को
अपना विष ही तो दिया है!
धुएँ उठाता वज्र कालकूट
मेरे पास दुख के सिवा है क्या?
इसने मुझपर कम एहसान नहीं किए
हर बड़े दुख ने मुझे थोड़ा बड़ा ही बनाया है
और सिखाया है जीने का शऊर
तब मैं भूल जाता हूँ अपनी अनवरत चोटें
और मैं फिर मुस्कुराता हूँ जी भर
जैसे बारिशों में नहाता है जंगल
हरी हो जाती है धरा
और इधर मैं भी
छोटे-छोटे सुखों से लबालब भरा। ¨¨¨
आते हुए
उसने कोई दस्तक नहीं दी
पर मैंने दरवाजा खोल दिया
वह हवा की तरह दबे पाँव
निःशब्द आया था
पर मेरी साँस की धौंकनी ने
सुन ली थी उसकी पदचाप।
मैंने भी कुछ नहीं कहा
पर मेरे भीतर गूँज रहे थे
शब्द की खोल हटाकर बाहर आते अर्थ।
मुझे अक्सर सन्नाटे से
बात करना पसंद है
क्योंकि उसमें दूसरों को
सुनने की पूरी गुंजाइश है।
मैंने दरवाजा खोल दिया
वह आए और मुझे
आपूरित कर दे
जैसे वर्षा में ऊपर तक
खिंच आता है ताल का पानी,
वह आए जैसे मुड़ा हुआ नन्हा पत्ता
पेड़ की डाल से किसी ललछौहें
प्रसवित शिशु की तरह डगमगाता है।
वह आए,
जैसे गंधमयी पृथ्वी
हवा के दोल पर झूलती है
वह आए
जैसे सन्नाटे में शब्द गूंजते हैं
वह आए
जैसे दो मिलती-जुलती बातें
एक नये मिथ को रचती हैं
किसी नई शुरूआत के लिए। ¨¨¨
समुद्र होने तक
कभी-कभी क्यों लगता है मुझे
मैं बदलता जा रहा हूँ
धीरे-धीरे पर लगातार।
मुझमे जन्म लेता है कोई अंकुर
मेरी त्वचा पर जागता है कमल-वन
और मन किसी शापित यक्ष-सा
नर्मदा और शिप्रा का जल उलीचना चाहता है
शब्द मेरा पीछा करते हैं
और मैं
घाटियों में घूमती हुई प्रतिध्वनियों में
चट्टानों की कोख में धँसे हुए
काँटेदार पेड़ों की टहनियों पर
लहूलुहान
अपने शब्दों से लड़ता हूँ।
मेरे भीतर जो है
उसे शब्द क्यों रोकते हैं?
धुआँ पकड़ने जैसी चीज का पागलपन
क्यों होता है?
मैंं नहीं जानता
क्यों मेरे भीतर
शताब्दियों से महाभारत चल रहा है।
मैं रक्त की नदी फलाँग कर
उस आदिम स्रोत को छूना चाहता हूँ
और गहरे धँसकर
कहाँ से क्यों और कैसे मेरा जन्म होता है?
मुझे रोको नहीं
मेरी अस्फुट बुदबुदाहट सुनने की कोशिश करो
पतझर के चरमराते हुए पत्तों का संगीत
और डालियों को फोड़कर
निकलता हुआ ऋतुपर्ण
सब जैसे मन के रूपान्तर हैं।
क्यों बार-बार लगता है मुझे
भीड़ भरी सड़कें,
गोद में चिहुंकता बच्चा,
भाषण, जुलूस, दंगे और भीड़
सब किसी नदी, पहाड़ और वनों के
समानांतर हैं।
अक्सर सड़क पर चलते हुए मुुझे
नरम दूब का ख्याल आता है
ऐसे ही समय
मुझे घेरता है कोई सम्मोहन
और मैं भीतर, अपने और भीतर-
किसी तंग सुरंग से
घुटनों के बल सरकता हुआ
पहुँचना चाहता हूँ।
कोई गर्म लावा पिघलकर
मेरी चेतना के सारे दकियानूसी बुर्ज
ढाहता हुआ बह चलता है।
मेरे भीतर कहीं सोता फूट जाता है
और मेरी जगह बच जाता है
सिर्फ समुद्र!
==============================
दुर्लभ किताबों के PDF के लिए जानकी पुल को telegram पर सब्सक्राइब करें